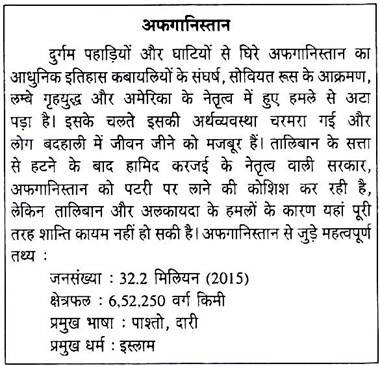ADVERTISEMENTS:
Here is an essay on ‘Afghanistan Crisis’ especially written for school and college students in Hindi language.
Essay # 1. अफगानिस्तान में सोवियत रूस-अमरीकी प्रतिस्पर्द्धा:
27 दिसम्बर, 1979 को अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों के प्रवेश से अफगान संकट उत्पन्न हुआ । इसका तात्कालिक परिणाम जहां एक ओर दूसरे शीत-युद्ध की शुरुआत थी वहीं दक्षिणी एशिया में भारत और पाकिस्तान के मध्य हथियारों की होड़ को तीव्रतम करना था ।
शीत-युद्ध के वैमनस्यपूर्ण वातावरण में केवल अफगानिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश था जहां महाशक्तियां एक-दूसरे की जडें काटने के बजाय कन्धे-से-कन्धा मिलाकर पारस्परिक सहयोग करने के लिए प्रयत्नशील थीं । सहयोग की प्रतिस्पर्द्धा का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि श्रीलंका, म्यांमार (बर्मा) और नेपाल को एक अवधि में महाशक्तियों ने कुल मिलाकर जितनी आर्थिक सहायता दी उससे कहीं अधिक सहायता अकेले अफगानिस्तान ने ही प्राप्त कर ली ।
द्वितीय महायुद्ध के तत्काल बाद यद्यपि अफगानिस्तान के प्रति सोवियत मन में कोई निश्चित कटुता नहीं थी किन्तु स्टालिन काल में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान के प्रति विभिन्न क्षेत्रों में अमैत्रीपूर्ण अभिमतों की अभिव्यक्ति को टाला नहीं जा सका ।
विशेषकर उत्तरी अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में तेलोत्खनन करने वाले अमरीकी तकनीशियनों की उपस्थिति पर सोवियत संघ ने आपत्ति की । अफगानिस्तान ने एक चतुर मध्यवर्ती और लघु शक्ति राज्य की तरह इस सोवियत आपत्ति को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने का प्रयत्न किया ।
उसने अपनी समक्षता का प्रदर्शन करते हुए यद्यपि सोवियत आपत्ति-पत्र को निरस्त कर दिया किन्तु सोवियत आक्रमण की सम्भावना का आधार दिखाकर अमरीका से सैनिक सहायता प्राप्त करने का प्रयल किया । अमरीका, अफगानिस्तान के लिए सोवियत संघ से भिड़ने के लिए तैयार नहीं था । अत: उसने सैनिक सहायता की मांग को अस्वीकार कर दिया । अफगानिस्तान ने अमरीकी तकनीशियनों को आखिरकार हटा लिया ।
लघु-शक्तियों की यह सामान्य प्रवृत्ति अफगान व्यवहार में परिलक्षित होती है कि आत्म-रक्षा की सामर्थ्य स्वयं में नहीं होती अत: आत्म-रक्षा के लिए चाहे उसकी आवश्यकता वास्तविक या काल्पनिक हो, उसे किसी महाशक्ति पर अवलम्बित होना पड़ता है इस मूलभूत दुर्बलता के बावजूद लघु-शक्तियां महाशक्तियों के साथ समान स्तर पर व्यवहार करना चाहती हैं ।
ADVERTISEMENTS:
इसीलिए सोवियत आपत्ति-पत्र को निरस्त करने के बावजूद अफगानिस्तान अमरीकी तकनीशियनों को सोवियत सीमान्तों के पास से हटा लेने के लिए विवश हो गया । शाह महमूद काल में अफगान शासकों को यह भी पता चला कि अमरीका केवल उस सीमा तक अफगानिस्तान के साथ है जब तक कि अफगानिस्तान के कारण उसका सीधे सोवियत रूस से मुकाबला नहीं होता और रूस केवल उस सीमा तक अफगानिस्तान के साथ है जब तक कि वह ‘साथ’ रूसी सुरक्षा मंतव्य को सिद्ध करता है ।
1953 में शाह महमूद खान के पद-त्याग और प्रधानमन्त्री पद पर सरदार दाऊद खान के आसीन होने पर अफगान विदेश नीति के समक्ष नयी चुनौतियां उपस्थित हुईं । मास्को में स्टालिन के स्थान पर मेलन्कोव-ख्रुश्चेव नेतृत्व आया और वाशिंगटन में ट्रूमैन प्रशासन को बदला आइजनहॉवर-डलेस प्रशासन ने ।
दोनों महाशक्तियों का ध्यान एशिया की ओर आकर्षित हुआ और अब एशिया भी शीत-युद्ध के प्रांगण के रूप में बदलने लगा । आइजनहॉवर प्रशासन ने जब सैनिक गठबन्धनों की नीति अपनायी तो स्पष्ट ही था कि जो देश उनसे असंलग्न रहेंगे उन्हें अमरीका डीन एचसिन के शब्दों में ‘कन्धों पर बिठाने के लिए’ तैयार नहीं था ।
दूसरी ओर ‘शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व’ की नीति का प्रतिपादक नया सोवियत नेतृत्व एशियाई देशों को अपने गुट में सम्मिलित किये बिना भी आर्थिक सहायता और समर्थन देने के लिए तैयार था । ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान को जहां सोवियत सहायता और समर्थन प्राप्त करना था वहां यह भी देखना था कि वह अपने उत्तरी पड़ोसी पर अत्यधिक निर्भर नहीं हो जाये ।
ADVERTISEMENTS:
अत: उसकी केन्द्रीय समस्या सोवियत संघ से प्रचुर आर्थिक सहायता स्वीकार करते हुए अनेक राजनीतिक प्रश्नों पर एकमत होते हुए भी अमरीका से ऐसे सम्बन्धों का निर्माण करना था जिनके द्वारा अफगान-सोवियत सामीप्य को सन्तुलित किया जा सके ।
अफगानिस्तान में सम-सामीप्य की प्रक्रिया विविधरूपा रही । अमरीका ने ज्योंही पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना प्रारम्भ किया अफगानिस्तान को अपनी प्रतिरक्षा की चिन्ता सताने लगी । पख्तूनिस्तान के विवाद को लेकर पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर कभी भी युद्ध छिड़ सकता था ।
अत: जो अफगानिस्तान कल तक अमरीका से शस्त्र मांग रहा था, वही अफगानिस्तान अब आर्थिक और सैनिक सहायता के लिए सोवियत संघ की ओर अभिमुख हुआ । सोवियत संघ इस स्थिति का पहले से ही लाभ उठाना चाहता था ।
उसने न केवल पख्तून प्रश्न पर खुलकर अफगानिस्तान का समर्थन किया बल्कि आर्थिक सहायता के पर्याप्त कल्पनाशील और प्रदर्शनात्मक कार्यक्रम शुरू कर दिये । सोवियत नेताओं ने अपनी प्रथम काबुल यात्रा में 70 करोड़ डॉलर का ऋण देने की घोषणा करके सोवियत-अफगान मैत्री का सम्मोहक वातावरण तैयार कर दिया ।
इस सोवियत-अफगान सामीप्य के बढ़ते हुए ‘खतरे’ को अमरीका उत्साहवर्द्धक देख रहा था किन्तु उसके पास इस मुकाबले में कोई सक्षम विकल्प नहीं था । अमरीकियों को विश्वास था कि अफगानिस्तान को अपनी स्वतन्त्रता उतनी ही प्रिय है जितना कि आर्थिक विकास ।
सोवियत संघ के साथ अभूतपूर्व घनिष्ठता बढ़ाते हुए भी सरदार दाऊद ने सदा यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि घनिष्ठता का अभिप्राय अनन्यता नहीं है । यदि अन्य महाशक्तियां अफगानिस्तान की सहायता करना चाहें तो उनका स्वागत है ।
वास्तव में अफगान-सोवियत सामीप्य को अफगान शासकों ने जिस सावधानीपूर्ण नाटकीयता के साथ विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया उससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि अफगान शासक अमरीका को अफगानिस्तान में रुचि दिखाने के लिए उत्तेजित करने का प्रयत्न कर रहे थे ।
एक बहुत बड़ी सीमा तक अफगान राजनीति सफल भी हुई । अमरीकी नीति-निर्माताओं ने विचार किया कि यदि अफगानिस्तान में एकछत्र सोवियत वर्चस्व हो गया तो अमेरीका की सुरक्षा-शृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट जायेगी, अत: सोवियत सहायता के मुकाबले में अमरीकी सहायता-कार्यक्रम भी प्रभावशाली ढंग से चलने लगा । अमरीकी सहायता-कार्यक्रमों में भी राजनीतिक व्यावहारिकता और चमत्कारोत्पादकता के तत्व का सन्निवेश होने लगा ।
दस करोड़ डॉलर के सोवियत ऋण की घोषणा होने के तत्काल बाद अफगानिस्तान को दी जाने वाली अमरीकी आर्थिक सहायता ‘नौ गुना’ बढ़ गयी और उसमें अब घोंघागति से चलने वाली हेलमन्द घाटी प्रायोजना को सफल करने का ही उद्देश्य नहीं था बल्कि यातायात वायु संचार शिक्षा कृषि एवं सिंचाई तकनीकी प्रशिक्षण तथा सांस्कृतिक प्रभाव, आदि सभी क्षेत्रों में सोवियत प्रभाव का मुकाबला करने की एक सुनिश्चित इच्छा दिखायी देने लगी ।
इस प्रतिस्पर्द्धा की विशेषता यह थी कि अमरीका न तो सोवियत प्रयत्नों को विफल करना चाहता था और न ही सोवियत संघ अमरीकी प्रयत्नों को विफल करना चाहता था बल्कि एक ही क्षेत्र के आधे-आधे भागों को पूर्ण करने के लिए दोनों महाशक्तियों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा देखी जा सकती थी ।
उदाहरण के लिए यदि सपूर्ण अफगानिस्तान की वृत्ताकार सड़क के उत्तरी हिस्से का निर्माण सोवियत संघ करता है तो उसी सड़क के दक्षिणी हिस्से का निर्माण अमरीका करता है । यदि अमरीका दक्षिणी-पश्चिमी अफगानिस्तान में कृषि सिंचाई तथा अन्य विकास कार्यों में संलग्न है तो रूस उत्तरी और पूर्वी अफगानिस्तान में इसी प्रकार के कार्यों में संलग्न है ।
यदि रूस ने काबुल के हवाई अड्डे का नवीनीकरण करके उसे आकर्षण बना दिया तो अमरीका ने कन्धार में एक विशाल और अधुनातन हवाई अड्डे का निर्माण कर दिया । 1961-63 में अफगान-पाक सीमाबन्दी के समय यदि सोवियत संघ ने अफगान माल को हवाई जहाजों में लदवाकर भेजने की विशिष्ट अनुकम्पा प्रदर्शित की तो अमरीका ने दस लाख डॉलर खर्च करके माल ले जाने के लिए ईरान होकर रास्ता बनाने का असाधारण कदम उठाया ।
इस प्रकार की सहयोगात्मक गतिविधियां न केवल आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रकट हुईं बल्कि दाऊद शासन के अन्तिम दिनों में सैनिक क्षेत्र में भी इसी प्रकार के लक्षण प्रकट हुए । अफगानिस्तान की सैन्य व्यवस्था को जिसका पर्याप्त मात्रा में रूसीकरण हो चुका था, पश्चिमाभिमुख करने के लिए अमरीकियों ने सैनिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी शुरू कर दिये । यहां रोचक बात यह है कि सोवियत विमानों को चलाने के लिए अमरीकी प्रशिक्षण दे रहे थे ।
इसी प्रकार विभिन्न अफगान मन्त्रालयों में सोवियत और अमरीकी विशेषज्ञ अनेक मामलों पर अफगानिस्तान के अधिकारियों को संयुक्त रूप से परामर्श देते थे । मिस्र में अस्वान बांध तथा भारत में बोकारो कारखाने को लेकर महाशक्तियों में जिस प्रकार की आक्रामक प्रतिस्पर्द्धा दिखायी दी उस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा अफगानिस्तान में दिखायी नहीं पड़ती ।
सोवियत संघ ने अपनी गतिविधियों को मुख्य रूप से उत्तरी अफगानिस्तान में तथा अमरीका ने अपनी गतिविधियों को दक्षिणी अफगानिस्तान में केन्द्रित रखा । यह प्रवृत्ति दोनों महाशक्तियों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त अनुकूल थी ।
अन्य कारणों के अतिरिक्त अफगानिस्तान की भौगोलिक अवस्थिति के कारण इस छोटे-से देश में जिस स्तर पर महाशक्तियों की प्रतिस्पर्द्धात्मक रुचि जाग्रत हुई वह बेमिसाल है । उदाहरणार्थ, अधुनातन आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका और नेपाल को कुल मिलाकर जितनी अमरीकी सहायता मिली उससे कहीं अधिक सहायता अकेले अफगानिस्तान को उसी अवधि में मिली ।
इसी प्रकार इन तीन देशों को जितनी सोवियत सहायता मिली, उसकी तुलना में अकेले अफगानिस्तान को लगभग छ: गुनी अधिक सहायता मिली । दूसरी ओर अफगानिस्तान में महाशक्तियों के इतने कर्मचारी कार्यरत थे कि उनकी संख्या की बराबरी में तुर्की पाकिस्तान ईरान नेपाल तथा भारत भी पीछे रह जाता है ।
इस प्रकार, शीत-युद्ध के वैमनस्यपूर्ण वातावरण में महाशक्तियों द्वारा अफगानिस्तान में कन्धे-से-कन्धा मिलाकर कार्य करना एक ऐसी विलक्षण प्रवृत्ति थी जिसे छोटे पैमाने पर ‘विश्व दितान्त’ का पूर्व-दर्शन कह सकते हैं ।
Essay # 2. अफगान संकट: नये शीत-युद्ध की दस्तक:
अफगानिस्तान को हड़पने का रूसी मंसूबा नया नहीं है । बहुत लम्बे समय तक ब्रिटिश सरकार ने जार सल्तनत को हिन्दूकुश के दक्षिण में प्रवेश करने से रोके रखा था । तब अफगानिस्तान के उत्तर में हिन्दूकुश पर्वत को एक ऐसा अवरोध समझा जाता था जिसे लांघना आसान नहीं था ।
19वीं और 20वीं सदी के आरम्भ में यहां ब्रिटिश और ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की खूंख्वार और दबंग कबायलियों से तीन बार लड़ाइयां हुईं । एक समकालीन प्रेक्षक के अनुसार- ”इसका उद्देश्य अफगान ऊंट को रूसी भालू से बचाना था ।” इस दौर में अफगानिस्तान एक ऐसी कमजोर लेकिन कामचलाऊ मध्यवर्ती राज्य (बफर स्टेट) था जिसका उद्देश्य ईरान एवं भारत-पाक उप-महाद्वीपों में जार सैनिकों की पेशकदमी को रोकना था ।
दूसरे विश्व-युद्ध के बाद सोवियत सरकार की दक्षिण-पश्चिमी एशिया में विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश रखने की ब्रिटिश भूमिका अमरीका ने निभानी शुरू कर दी । कुछ समय तक मुकाबले की होड़ बराबर रही । रूसियों ने काबुल में एक हवाई अड्डा बनाया तो अमरीकियों ने कन्धार में ।
रूसियों ने काबुल में विशाल अन्न भण्डार बनाया तो अमरीकियों ने उसमें गेहूं भर दिया । रूस ने सलांग राजमार्ग का निर्माण किया तो अमरीकियों ने अफगानिस्तान की राष्ट्रीय विमान सेवा के लिए सहायता देकर जवाबी कार्यवाही कर दी ।
लेकिन पर्याप्त अमरीकी योगदान के बावजूद साठादि दशक के अन्तिम दौर में सोवियत रूस का प्रभाव बढ़ने लगा । चूंकि उस समय अमरीका वियतनाम की जंग में उलझा था, इसलिए उसने आर्थिक सहायता में कमी कर दी, लेकिन सत्तरादि दशक के अन्त ने काबुल को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाकर 1.5 अरब डॉलर तक कर दी ।
रूस ने होनहार अफगान अधिकारियों को सोवियत संघ में प्रशिक्षण देना आरम्भ किया । अफगानिस्तान में कम्युनिस्टों ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (P.D.P.) संगठित की और सशस्त्र सेनाओं में भी अपना प्रभाव बढ़ाया ।
पी.डी.पी. नेता और तत्कालीन विदेशमन्त्री हफीजुल्ला अमीन ने 1978 में सीना तानकर कहा था- ”मैं 1966 से सेना के भीतर गुप्त रूप से काम कर रहा था…1973 के शुरू से ही मैं थल सेना और वायु सेना में तीन-सदस्यीय कम्युनिस्ट इकाइयों को संगठित करने में लगा था ।”
अप्रैल, 1978 में इन प्रयत्नों का सुपरिणाम सामने आया । अमीन के नेतृत्व में हुई क्रान्ति के द्वारा काबुल के रेडियो स्टेशन और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया और राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद की तटस्थ सरकार का तख्ता उलट दिया गया । अमीन के नेतृत्व में पी.डी.पी. सरकार ने सत्ता संभाल ली और नूर मोहम्मद तराकी को राष्ट्रपति बना दिया गया ।
अमीन ने अफगानों पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद थोपने के नाम पर बेरहमी से आतंक बरसाना शुरू कर दिया । अप्रैल, 1978 और नवम्बर, 1979 के दौरान काबुल की जेलों में ही करीब 12,000 अफगानों की मृत्यु हो गयी । जो बच गये उन्होंने बताया कि किस प्रकार बिजली के नंगे तारों को छुआकर और शिकंजे (पेंच लगी धातु की दो चादरें जिनका उपयोग लोगों के हाथ-पैर कुचल डालने के लिए किया जाता था) का उपयोग करके आतंक बरसाया गया बन्दियों को उन्हीं के मल-मूत्र में डुबा दिया गया ।
जब अफगानों को नयी सरकार के असली रंग-ढंग का पता चला तो सारे देश में मुजाहिद विरोध में उठ खडे हुए । ऐसा लगता था कि बढ़ती अव्यवस्था से चिन्तित होकर सोवियत शासकों ने पहले तो यह चाहा कि अमीन से तराकी छुटकारा पा लें, लेकिन सितम्बर 1979 में खुद तराकी को मार दिया गया और अमीन ने अपने को राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री घोषित कर दिया ।
इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में पी. डी. पी. का नियन्त्रण तेजी से खोने लगा । मुजाहिदों ने प्रमुख शहरों के बीच मुख्य मार्गों से होने वाले सम्पर्क को भंग करना शुरू कर दिया । 1979 के अन्तिम दिनों में सरकार देश के 29 प्रान्तों में से केवल छ: में प्रशासन चलाने का दावा करने की स्थिति में थी ।
ऐसा लगा कि सोवियत शासकों ने यह तय किया कि अमीन को रास्ते से हटा दिया जाये । भूतपूर्व वकील बबराक करमाल के नेतृत्व में पी.डी.पी के अमीन विरोधी गुट से मिलकर सोवियत शासकों ने 20 महीनों में तीसरी बार काबुल में कम्युनिस्ट क्रान्ति के लिए षड़यन्त्र रचा ।
24 दिसम्बर, 1979 को काबुल का आकाश सोवियत विमानों से भर गया और हवाई अड्डे पर सैनिक उतारे गये । काबुलवासियों को बताया गया कि मुजाहिदों के खिलाफ सरकार की सहायता करने के लिए रूसी आ रहे हैं । ठीक इसी समय अनेक सशस्त्र सैनिक टुकड़ियां सीमा पर आ पहुंचीं । निश्चित दिन 27 दिसम्बर, 1979 था ।
सुबह के सात बजे सोवियत सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन, हवाई अड्डे, रेडियो स्टेशन और अन्य प्रमुख केन्द्रों पर हमले कर दिये । मशीनों से लैस चार पैदल और बख्तरबन्द डिवीजनों का सोवियत सीमा से भीषण गर्जन सुनाई दिया जिन्होंने चन्द दिनों में ही सभी प्रमुख नगरों और कस्वों पर कब्जा कर लिया । वस्तुत: सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप करके नये शीत-युद्ध की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान कर दी ।
अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के मूलत: दो कारण थे:
i. प्रथम, गरम पानी के बन्दरगाहों की तलाश और
ii. द्वितीय, टर्की, ईरान एवं अफगानिस्तान से लगने वाली सीमाओं की सुरक्षा ।
राष्ट्रपति अमीन की सपरिवार हत्या कर दी गयी; उनके स्थान पर बबराक करमाल राष्ट्रपति बना दिये गये । 28 दिसम्बर, 1979 को सोवियत प्रवक्ताओं ने यह दलील पेश की कि अफगान सरकार ने अफगान-सोवियत मैत्री सन्धि के आधार पर सोवियत सरकार से सहायता जिसमें सैनिक सहायता भी सम्मिलित है की अपील की है और सोवियत सरकार ने उस अपील को स्वीकार कर लिया है ।
Essay # 3. अफगान संकट को जन्म देने वाले कारण:
27 दिसम्बर, 1979 को अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तथा उनका वहां 1988 तक बने रहना अफगान संकट को जन्म देता है, जिसके मुख्य कारण निम्न हैं:
1. अफगान साम्यवादी दल (P.D.P.) में गुटीय-प्रतिस्पर्द्धा:
जनवरी, 1965 में अफगानिस्तान में अफगान जनवादी जनतान्त्रिक दल की स्थापना हुई, परन्तु 2 वर्ष बाद ही यह दल ‘खल्की’ तथा ‘परचम’ गुटों में विभाजित हो गया । ‘खल्क’ गुट के नेता नूर मोहम्मद तराकी तथा ‘परचम’ गुट के नेता बबराक करमाल थे ।
अप्रैल, 1978 की क्रान्ति के समय दोनों गुट एक हो गये थे परन्तु बाद में दोनों एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गये । बबराक करमाल को उपप्रधानमन्त्री के पद से हटाकर चेकोस्लोवाकिया में राजदूत नियुक्त कर दिया गया । गुटबन्दी की इस अफगान राष्ट्रीय राजनीति के परिणामस्वरूप विदेशी हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त हुआ ।
2. अफगान सरकारों के जनाधार का अभाव:
अप्रैल, 1978 की क्रान्ति के समय से अफगानिस्तान में कोई ऐसी सरकार सत्तारूढ़ नहीं हुई जिसे जनसमर्थन प्राप्त हो । अप्रैल 1978 के बाद बनने वाली अफगान सरकारों का अस्तित्व सैनिक अफसरों के सहयोग पर टिका हुआ था । इन्हें सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था । इस प्रकार विदेशी सहायता पर टिकी हुई सरकार जन सहयोग के अभाव में अधिक समय तक चल नहीं सकती थी ।
3 अमीन की रूस विरोधी गतिविधियां:
सितम्बर, 1979 में नूर मोहम्मद तराकी को अपदस्थ करने के बाद हफीजुल्लाह अमीन अफगानिस्तान के नये राष्ट्रपति बने । ऐसा कहा जाता है कि अमीन कतिपय ऐसी नीतियां अपनाते जा रहे थे जो यदि 2-3 वर्ष तक जारी रह जातीं तो निश्चय ही अफगानिस्तान सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाता लेकिन सोवियत संघ को इसका आभास हो गया । इसलिए कुछ विचारकों की यह मान्यता है कि अफगानिस्तान में समाजवाद की रक्षा के लिए सोवियत संघ ने 27 दिसम्बर, 1979 को सैनिक हस्तक्षेप किया था ।
4. अफगानिस्तान में अनिश्चय और अस्थिरता का वातावरण:
अफगानिस्तान में अस्थिरता और अनिश्चय के वातावरण के परिणामस्वरूप 20 माह की अल्प अवधि में तीन क्रान्तियां हो गयीं । पहली क्रान्ति 27 अप्रैल, 1978 को हुई जिसमें राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद व उनके परिवार का सफाया कर दिया गया और साम्यवादी दल समर्थक खल्क पार्टी के नेता नूर मोहम्मद तराकी राष्ट्रपति बने ।
दूसरी क्रान्ति 6 सितम्बर, 1979 को हुई जिसमें तराकी का तख्ता पलटकर हफीजुल्लाह अमीन राष्ट्रपति बने । तीसरी क्रान्ति 27 दिसम्बर, 1979 को हुई जिसमें अमीन की हत्या कर दी गयी और परचम नेता बबराक करमाल राष्ट्रपति बने । वस्तुत: तीसरी क्रान्ति अफगान सैनिकों ने नहीं की बल्कि सोवियत संघ ने प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप करके बबराक करमाल को काबुल की गद्दी पर बिठाया ।
5. अफगानिस्तान-सोवियत प्रभाव क्षेत्र:
अफगान शासक तथा पश्चिमी शक्तियां दोनों ही अफगानिस्तान को सोवियत प्रभाव क्षेत्र स्वीकार करती रही हैं । अफगान शासक अपनी विदेश नीति को रूसी आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित करते रहे हैं । अफगानिस्तान ने सोवियत रूस की इस भावना का सदा आदर किया कि उसके उत्तरी भाग में कोई दूसरा देश अपनी गतिविधियां जारी न रखे ।
दाऊद ने सोवियत संघ के साथ विशिष्ट सम्बन्ध रखते हुए भी अफगानिस्तान की परम्परागत तटस्थता को बनाये रखा किन्तु तराकी और अमीन ने अफगानिस्तान की स्वतन्त्र हैसियत को नष्ट कर दिया और उसे चेकोस्लोवाकिया या हंगरी बना दिया । अफगानिस्तान के नेताओं ने सौर क्रान्ति (1978) को अक्टूबर क्रान्ति (रूसी क्रान्ति) का ही विस्तार माना । अफगान नेताओं की इस मनोवृत्ति ने सोवियत संघ को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया ।
6. अफगानिस्तान में सोवियत विशेषज्ञों एवं सलाहकारों का जमाव:
1978 की सौर क्रान्ति के बाद अफगानिस्तान में सोवियत तकनीशियनों एवं सलाहकारों का प्रभाव एवं जमाव इतना अधिक हो गया था कि उनकी राय के बिना कोई कार्य करना सम्भव नहीं था । सोवियत विशेषज्ञ एवं सलाहकार अफगानिस्तान के विविध विभागों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत थे जिसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने का सुअवसर प्राप्त हो गया ।
7. गरम पानी का बन्दरगाह प्राप्त करने की लालसा:
अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप का एक विशेष कारण यह भी था कि इसके द्वारा वह गरम पानी का बन्दरगाह प्राप्त करना चाहता था ।
8. सोवियत सुरक्षा का प्रश्न:
सोवियत संघ ने प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप का निर्णय विशुद्ध राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किया जिससे कि अमरीका और चीन सोवियत संघ विरोधी अभियान में अफगानिस्तान को अड्डा नहीं बना सकें ।
Essay # 4. अफगान संकट और संयुक्त राष्ट्र संघ:
अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति कार्टर ने अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं के प्रवेश तथा हस्तक्षेप की कड़ी निन्दा करते हुए मॉस्को से अपनी फौजें तुरन्त वापस बुलाने के लिए कहा और उसके ऐसा न करने पर उसने इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद् में उठाया ।
यद्यपि सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव द्वारा सोवियत संघ से अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियां समाप्त करने और सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की परन्तु रूस ने वीटो के अधिकार का प्रयोग करके इस प्रस्ताव को प्रभावहीन बना दिया । महासभा ने अपने आपात्कालीन अधिवेशन के दौरान 15 जनवरी, 1980 को एक प्रस्ताव द्वारा मांग की कि अफगानिस्तान से तत्काल विदेशी सेनाएं हटायी जायें ।
सुरक्षा परिषद् में करमाल सरकार के विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद दोस्त ने सोवियत फौजों की वापसी के प्रस्ताव पर प्रबल आपत्ति करते हुए कहा कि- “यह अफगानिस्तान का विशुद्ध रूप से घरेलू मामला है । इस कार्यवाही से इस प्रदेश में शान्ति को कोई खतरा नहीं है । प्रत्येक राज्य को आत्मरक्षा करने का अधिकार है और इसमें वह किसी भी देश से सहायता ले सकता है । अफगानिस्तान ने मॉस्को के साथ 1978 की सन्धि के आधार पर सहायता मांगी और उसकी प्रार्थना पर ही सोवियत संघ की सेनाएं काबुल आयीं ।”
चीनी प्रतिनिधि चेन चू ने अफगान प्रतिनिधि के कथन का खण्डन करते हुए कहा कि सोवियत संघ को अफगान सरकार द्वारा सेनाएं भेजने का कोई निमन्त्रण नहीं मिला है । यह कहना गलत है कि इसे अमीन की सरकार ने निमन्त्रित किया है क्योंकि इस क्रान्ति में मारे गये अमीन इतने मूर्ख नहीं थे कि वे अपने विरोधी को अपना सफाया करने के लिए खुद बुलाते ।
राष्ट्रपति करमाल भी रूसियों को निमन्त्रण नहीं दे सकते थे क्योंकि वे उस समय पूर्वी यूरोप में थे । वस्तुत: सोवियत संघ का यह कार्य उसकी विस्तारवादी नीति का एक अंग और दक्षिण में हिन्द महासागर की ओर बने समुद्री मार्गों और सामरिक अड्डों को नियन्त्रित करने यूरोप को घेरने एशिया को संकट में डालने और विश्व पर छा जाने का प्रयास था ।
अफगानिस्तान की समस्या के राजनीतिक हल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने सम्बन्धित देशों को एक चार-सूत्री योजना प्रस्तुत की । इस योजना पर बातचीत करने के लिए मार्च 1983 में महासचिव कुइयर एवं उसके प्रतिनिधि श्री कोरदोवेज ने मास्को की यात्रा की एवं सोवियत नेताओं से बातचीत की ।
इस योजना के अन्तर्गत एक नियत अवधि में अफगानिस्तान से सभी सोवियत सैनिक हटाये जाने की व्यवस्था की गयी । इसके अतिरिक्त सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमरीका तथा चीन की ओर से अफगानिस्तान की स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता तथा निर्गुटता की गारण्टी दिये जाने का प्रस्ताव था ।
साथ ही पाकिस्तान तथा ईरान को भी अफगानिस्तान के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का आश्वासन देना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में सोवियत संघ व अमरीका भी सहयोग देंगे । इसी प्रकार अफगानिस्तान भी यह वचन देगा कि वह पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कुइयर के प्रस्ताव में आगे कहा गया कि रूसी हस्तक्षेप के बाद जो अफगान नागरिक पाकिस्तान, भारत तथा अन्य देशों में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उनके स्वदेश लौटने की व्यवस्था की जायेगी ।
साथ ही स्वदेश लौटने पर उन्हें निवास, अपने जीविकोपार्जन की पूरी स्वतन्त्रता तथा सुविधा प्रदान की जायेगी । संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 नवम्बर, 1985 को एक नया प्रस्ताव पारित कर अफगानिस्तान से विदेशी फौजें हटाने का अनुरोध किया ।
गत पांच वर्षों में सातवीं बार महासभा ने यह प्रस्ताव पास किया । इसके पक्ष में 122 तथा विपक्ष में 9 वोट पड़े भारत सहित 12 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया । 10 नवम्बर, 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 123 मतों से यह प्रस्ताव पारित किया कि सोवियत संघ को अविलम्ब अफगानिस्तान से अपनी फौजें हटा लेनी चाहिए । प्रस्ताव के विपक्ष में 19 मत पड़े ।
4 नवम्बर, 1988 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफगानिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव में कहा कि 15 फरवरी, 1989 से पूर्व सभी सैनिकों को वहां से हटा लिया जाये । प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान समस्या से सम्बद्ध सभी पक्षों से वार्ता करके अफगानिस्तान में एक सर्वदलीय सरकार स्थापित की जानी चाहिए । इस प्रस्ताव का समर्थन 122 देशों ने किया । सोवियत संघ तथा वियतनाम सहित 19 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया । भारत सहित 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया ।
Essay # 5. अफगान संकट और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति:
अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के अत्यन्त महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम हुए । भबानी सेन गुप्ता लिखते हैं- ”अफगानिस्तान तीसरे विश्व की राजनीतिक स्थिति में सोवियत हस्तक्षेप का प्रथम मामला नहीं है, परन्तु यह तीसरे विश्व में तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत गुट को छोड्कर विश्व में अन्य कहीं प्रथम प्रत्यक्ष सोवियत सैनिक हस्तक्षेप है । यह पूर्वी यूरोप में सोवियत गुट के बाहर एक मार्क्सवादी शासन की रक्षा के लिए प्रथम प्रत्यक्ष सोवियत सैनिक हस्तक्षेप है, यद्यपि यह सोवियत संघ से लगा हुआ क्षेत्र है । इससे भी अधिक, यह पहला सोवियत हस्तक्षेप है जिसके विरुद्ध अमरीका ने जोरदार विरोध प्रकट किया तथा जिसने एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों को, जिनमें से कुछ मास्को मैत्री सम्बन्धों से बंधे हैं, वास्तविक रूप से चिन्तित कर दिया है ।”
डॉ.के.पी. मिश्र के शब्दों में- ”सोवियत संघ ने अर्थात् एक महाशक्ति ने अफगानिस्तान में ‘प्रमुखता अधिकार’ (Hegemonistic Right) के आधार पर हस्तक्षेप किया जिसने दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता और अखण्डता पर प्रश्न-चिह लगा दिया।”
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अफगान संकट के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं:
1. तनाव-शैथिल्य को गहरा धक्का:
अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप ने अमरीकी-सोवियत तनाव-शैथिल्य को एक गहरा धक्का पहुंचाया ।
2. नव शीत-युद्ध की शुरुआत:
अफगान संकट के कारण शीत-युद्ध की पुन: शुरुआत हो गयी । दक्षिण एशिया पुन: तनाव का केन्द्र बन गया और हिन्द महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गयी । डॉ. वेदप्रताप वैदिक के शब्दों में- ”अफगानिस्तान के संकट ने विश्व की राजनीति पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव यह डाला कि मॉस्को तथा वाशिंगटन में शीत-युद्ध उग्र हो गया । पिछले दो दशकों में दोनों देशों में तनाव-शैथिल्य (Détente) तथा मधुर-मिलन हो रहा था; दोनों देशों ने हथियारों की होड़ कम करने के लिए दो सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता (SALT-I & II) की दो सन्धियों पर हस्ताक्षर किये थे किन्तु काबुल में 80 हजार सोवियत सेनाओं की उपस्थिति तथा अफगान सीमा पर 25-30 हजार सैनिकों के जमाव से दोनों देशों का तनाव चरम शिखर पर पहुंच गया ।”
3. पाकिस्तान की बढ़ती हुई चिन्ता:
अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने उसके पड़ोसी राष्ट्रों-ईरान और पाकिस्तान में गहरी चिन्ता उत्पन्न कर दी क्योंकि इससे दक्षिणी-पश्चिमी एशिया में तीस वर्ष से चला आ रहा भूराजनीतिक सन्तुलन अस्त-व्यस्त हो गया ।
पाकिस्तान में लगभग 5 लाख अफगान शरणार्थियों ने शरण ली । पाकिस्तान ने अपने को किसी सम्भावित बदले की सोवियत कार्यवाही का सामना करने में अक्षम पाया । वह अपनी सुरक्षा के लिए अमरीका के और भी निकट आ गया । अमरीका ने पाकिस्तान को भारी सैनिक सहायता देने का निर्णय किया इससे भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया ।
4. अमरीकी-चीनी गठजोड़ को बढ़ावा:
अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने अमरीका-चीन गठबन्धन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि अमरीका और चीन दोनों ही सोवियत संघ की शक्ति और प्रभाव के विस्तार को अपने लिए घातक मानते थे तथा सोवियत संघ को विश्व समस्याओं के समाधान में बाधक समझते थे ।
5. भारत की दुविधापूर्ण स्थिति:
अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने भारत को अत्यन्त दुविधापूर्ण स्थिति में डाल दिया । ऐसा कहा जाता है कि भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के मुद्दे पर वही नीति अपनायी जो पं. नेहरू ने हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप के तथा श्रीमती गांधी ने चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप के सम्बन्ध में अपनायी थी ।
जबकि वास्तविकता यह है कि भारत इस बार पहले से कहीं अधिक चिन्तित रहा । हंगरी और चेकोस्लोवाकिया भारत से सात हजार किलोमीटर दूर थे जबकि अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी और भू-राजनीति की दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप का अंग है ।
अब तक सोवियत संघ और भारत के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो मध्यवर्ती राज्य थे किन्तु अफगानिस्तान पर प्रभाव कायम हो जाने से सोवियत संघ भारत के काफी निकट आ गया । अफगानिस्तान में पैर जमाकर सोवियत संघ एक ऐसी एशियाई शक्ति बन जाता जो ईरान और पाकिस्तान पर दबाव डाल सकती ।
इससे शीत-युद्ध भारत के दरवाजे पर दस्तक देने लगा । अमरीका द्वारा पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर की सैनिक सहायता का प्रस्ताव पाकिस्तान की एक अमरीकी अग्रिम आधार शिविर बन जाने की सम्भावना प्रकट करने लगा । इससे भारत को न चाहते हुए भी शीत-युद्ध के जाल में उलझना पड़ा ।
6. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को विभाजित करने का मुद्दा:
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन भी अफगान संकट का शिकार होते-होते बच गया । अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के प्रश्न पर कुछ देशों ने, जिनमें पाकिस्तान प्रमुख था बगैर लिहाज के सोवियत संघ की नयी दिल्ली शिखर सम्मेलन में निन्दा की । मिस्र और ईरान रूसी कार्यवाही की पहले ही निन्दा कर चुके थे ।
Essay # 6. अन्तर्राष्ट्रीय दबाव:
अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की वापसी को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव निरन्तर बढ़ने लगा । केवल अमरीका और पश्चिमी देश ही सोवियत संघ के अफगानिस्तान से हटने के लिए जोर नहीं डाल रहे थे बल्कि अरब, एशिया अफ्रीका आदि देशों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था ।
अमरीका ने पाकिस्तान को अस्त्रों से लैस करने का निर्णय किया तो चीन ने भी पाकिस्तान को इस तरह की सहायता देने का विश्वास दिलाया । अरब देशों ने भी सोवियत सैनिकों के अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने का सिवाय दक्षिणी यमन के विरोध किया । यहां तक कि इराक जिसे सोवियत संघ से खासी सहायता मिलती थी, उसने भी सोवियत संघ की इस कार्यवाही की निन्दा की ।
इराक की निन्दा के पीछे शायद कुर्द हैं जो ईरान-इराक की सीमा को सदैव गर्म किये रहते हैं । अमरीकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने सीनेट में सामरिक अस प्रसार विरोधी सन्धि साल-पर बहस स्थगित करने का आदेश दिया था ।
सोवियत नेताओं से कार्टर ने ‘हॉट लाइन’ पर काफी कड़े शब्दों का उपयोग किया । अमरीका ने सोवियत संघ को अनाज देने तथा आधुनिक प्रविधि की जानकारी देने के अपने निर्णय को बदलकर सोवियत संघ की कार्यवाही का विरोध किया ।
Essay # 7. अफगान संकट : राजनीतिक हल:
अमरीका से हथियार प्राप्त करते हुए भी पाकिस्तान चूंकि यह कहता आया है कि वह अफगानिस्तान संकट का राजनीतिक हल चाहता है अत: संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में वह अफगान सरकार के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत करने को सहमत हुआ तथा पहले दौर की बातचीत जून 1982 में हुई तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तैयार किये गये जिस चार-सूत्री फॉर्मूले पर भाग लेने वाले सभी पक्ष सहमत थे ।
वह निम्न प्रकार था:
a. अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं की वापसी;
b. पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाहरी ताकतों का अहस्तक्षेप;
c. ऐसे हस्तक्षेप के खिलाफ सम्भवत: सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्यों की अन्तर्राष्ट्रीय गारण्टी; और
d. अफगान शरणार्थियों का अपने देश को लौटना, अफगानिस्तान लौटने पर अपनी पसन्द की सरकार का निर्माण तथा अफगानिस्तान का गुटनिरपेक्ष स्वरूप । जेनेवा वार्ता के सभी पहले दौर असफल रहे क्योंकि पाकिस्तान का कहना था कि पहले सोवियत संघ को सैनिकों की वापसी की समय-सारणी बनानी चाहिए ।
अफगान संकट के हल के सन्दर्भ में वर्ष 1988 का प्रारम्भ अच्छा सिद्ध हुआ । सोवियत विदेश मन्त्री शेवर्दनाद्जे ने जनवरी 1988 के पहले सप्ताह में काबुल का दौरा किया तथा व्यापक आधार पर मिली-जुली सरकार बनाने की कोशिश करने की योजनाओं की घोषणा की । गोर्बाच्योव ने भी घोषणा की कि सोवियत सैनिकों का पूरी तरह हटना 15 मई, 1988 से शुरू हो जायेगा, यदि जेनेवा में 15 मार्च तक समझौता हो जाये ।
जेनेवा समझौता:
संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में 14 अप्रैल, 1988 को साढ़े आठ वर्ष पुराने संकट को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए । अमेरिका और सोवियत संघ गारण्टीकर्ता बने । अमेरिका की ओर से विदेश सचिव जॉर्ज श्नुत्न और सोवियत संघ की ओर से विदेश मन्त्री शेवर्दनाते, अफगानिस्तान की ओर से विदेश मन्त्री अछूत वकील और पाकिस्तान की ओर से विदेश राज्य मन्त्री जैन नूरानी ने हस्ताक्षर किये ।
समझौते की मुख्य व्यवस्थाएं निम्न प्रकार थीं:
i. 15 मई, 1988 से 9 माह के भीतर संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की देखरेख में सोवियत सैनिकों की वापसी ।
ii. अफगानिस्तान में सोवियत संघ-अमरीका द्वारा हस्तक्षेप व प्रवेश न किये जाने के प्रति वचनबद्धता ।
iii. विविध अफगान, दलों व गुटों को सोवियत संघ व अमरीका द्वारा किसी प्रकार की सहायता न दिये जाने का आश्वासन ।
iv. अफगानिस्तान की सम्प्रभुता व क्षेत्रीय अखण्डता व गुटनिरपेक्षता की सभी देशों द्वारा मान्यता तथा रूस व अमरीका द्वारा उसकी प्रत्याभूति ।
v. पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों की वापसी ।
vi. समझौते के उल्लंघन व मतभेद की दशा में संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि की उपस्थिति में पाक-अफगान वार्ता व समाधान की व्यवस्था ।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक ने जेनेवा शान्ति समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह 20वीं सदी का एक करिश्मा है । भारत ने आशा व्यक्त की कि इस समझौते के फलस्वरूप क्षेत्र में तनाव कम होगा और क्षेत्र में अत्याधुनिक हथियार जमा करने का बहाना समाप्त होने के कारण इन हथियारों को हटाने का काम भी शुरू होगा ।
शान्ति की सम्भावना क्षीण:
जेनेवा समझौते के बावजूद अफगानिस्तान में शान्ति की सम्भावना क्षीण ही रही है । इस समझौते से लगभग एक दशक से लगातार संघर्ष और तनाव के बीच जी रही अफगान जनता को सोवियत फौज से मुक्ति तो मिल गयी लेकिन इससे उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुईं ।
समझौते की सबसे बड़ी कमी तो यह है कि तीन महत्वपूर्ण पक्ष-मुजाहिदीन अफगान शरणार्थी और ईरान इसमें शामिल नहीं थे । मुजाहिदीन ने समझौते को अस्वीकार कर दिया था । इससे अफगानिस्तान में खून-खराबे की सम्भावना बढ़ गयी ।
सोवियत फौजों की वापसी के बाद अफगानिस्तान भीषण गृहयुद्ध से ग्रसित है । 1992 में सोवियत संघ द्वारा समर्थित साम्यवादी रुझान की नजीब सरकार के पतन के उपरान्त मुजाहिदीनों में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारम्भ हुआ ।
बुरहानुद्दीन रब्बानी का जमात इस्लामी गुट तथा गुलबुद्दीन हिकमतयार का हज्व-इ-इस्लामी मुख्य संघर्षरत गुट थे । हिकमतयार को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था । 1993 के जून माह के समझौते के अनुसार रब्बानी राष्ट्रपति बने तथा हिकमतयार को प्रधानमन्त्री का पद प्राप्त हुआ, किन्तु यह समझौता अप्रभावी सिद्ध हुआ और अगस्त, 1993 से ही हिकमतयार की सेना ने पुन: गृहयुद्ध आरम्भ कर दिया ।
फरवरी 1995 में नवगठित उग्रवादी संगठन ‘तालिबान’ ने हिकमतयार के हज्व-इ-इस्तामी गुट को खदेड़कर कन्धार पर कब्जा कर लिया । बाद में इस उग्रवादी गुट को पराजित कर राष्ट्रपति रब्बानी ने 11 मार्च, 1995 को काबुल पर पुन: कब्जा कर लिया ।
सितम्बर 1996 में तालिबान ने काबुल पर अधिकार करके राष्ट्रपति रब्बानी को उत्तरी अफगानिस्तान में शरण लेने को बाध्य कर दिया । काबुल विजय से तालिबान देश की लगभग दो-तिहाई भूमि को अधिकार में कर चुके थे ।
मई, 1997 में उज्बेक नेता रसूल पहलवान तथा उसके भाई जनरल अछूत मलिक ने उज्वेक नेता दोस्तम का साथ छोड़कर तालिबान के साथ मित्रता कर ली । मलिक के पाला बदलने से उत्तरी अफगानिस्तान में सैन्य शक्ति का संतुलन पूर्णत: तालिबान के पक्ष में हो गया । तालिबान ने बिना किसी कठिनाई के उत्तरी अफगानिस्तान के प्रमुख नगर मजार-ए-शरीफ पर अधिकार कर लिया ।
किन्तु तालिबान और जनरल मलिक की दोस्ती अधिक दिनों तक टिकाऊ नहीं रही जनरल मलिक ने तालिबान का साथ छोड़ दिया और जून, 1997 में उत्तरी अफगानिस्तान में ताजिक शिया और उज्वेक लोगों का तालिबान के खिलाफ एक मोर्चा बना लिया ।
तालिबान का संपूर्ण अफगानिस्तान पर अधिकार करने का स्वप्न भंग हो गया । तालिबान ने जुलाई, 1998 में उत्तरी अफगानिस्तान में भारी आक्रमण किए थे जिनके फलस्वरूप उन्हें जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम और हिज्वे बहादत की सेनाओं को खदेड़ते हुए उत्तरी और मध्य अफगानिस्तान के अनेक शहरों पर कब्जा करने में सफलता मिली ।
तथापि कमाण्डर अहमद शाह मसूद ने अपने पारम्परिक प्रभाव वाले क्षेत्रों में तालिबान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कड़ा मुकाबला किया और अक्टूबर-नवम्बर 1998 में पूर्ण तारवर प्रान्त और कन्डूज में कुछ क्षेत्रों पर से तालिबान का नियन्त्रण हटाकर कब्जा कर लिया ।
तालिबान का उदय, गृहयुद्ध का जारी रहना आदि ऐसा घटनाचक्र है जिसने विश्व के अनेक देशों को अफगानिस्तान की समस्या में रुचि लेने के लिए प्रेरित कर दिया । 27 अगस्त, 1999 को संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान पर खुली बहस की जिसमें भारत ने भी भाग लिया । इस बहस में अधिकांश देशों का रवैया तालिबान के विरुद्ध सामान्य तौर पर सख्त रहा ।
सुरक्षा परिषद् ने अफगानिस्तान की स्थिति पर 15 अक्टूबर, 1999 को एक प्रस्ताव सं. 1267 पारित किया । इस प्रस्ताव में सभी राज्यों से मांग की गई कि वे तालिबान के स्वामित्व वाले अथवा उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए किसी भी विमान को अपने क्षेत्र में उड़ान भरने अथवा वहां उतरने की अनुमति न दें और तालिबान की निधियों तथा अन्य वित्तीय संसाधनों पर भी रोक लगा दें ।
तालिबान पर लगाए गए प्रतिबन्ध 14 नवम्बर, 1999 से प्रभावी हुए । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने 19 दिसम्बर, 2000 को 13-0 से एक प्रस्ताव पारित करके तालिबान प्रशासन के विरुद्ध प्रतिबन्धों को और भी कड़ा कर दिया । इसके अन्तर्गत तालिबान नियंत्रित अफगानी क्षेत्र का वायु सम्पर्क शेष विश्व से कट जाएगा तथा तालिबानी नेता विश्व में किसी भी भाग की यात्रा नहीं कर सकेंगे ।
तालिबान की विदेशों में स्थित सम्पत्ति को सील करने तथा उसे शस्त्रों की आपूर्ति रोकने का प्रतिबन्ध भी इसके अन्तर्गत आरोपित किया गया । ज्ञातव्य है कि सऊदी अरब मूल के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन जो तालिबान के संरक्षण में अफगानिस्तान में रह रहा बताया जाता है के अमेरिका को समर्पण के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से यह प्रतिबन्ध अमरीका की पहल से सुरक्षा परिषद् ने लगाये ।
यह सर्वविदित है कि तालिबान पाकिस्तान की संतान हैं तथा उन्हें पालने-पोसने में सऊदी अरब के धन की विशेष भूमिका रही है । अफगानिस्तान में तालिबान आन्दोलन की उत्पत्ति 1994 के उत्तरार्द्ध में हुई थी । इस्लाम के एक कट्टरपंथी धर्म गुरु मौलवी मुहम्मद उमर ने अपने शिष्यों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें ‘तालिबान’ नाम की पहचान दी । तालिबान मूलत: अफगान छात्रों का संगठन था ।
तालिबान के माध्यम से पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपने एक तरह से संरक्षित राज्य की स्थापना करना चाहता था । यदि सऊदी अरब तथा पाकिस्तान तालिबान के पक्षधर हैं तो रूस तथा अफगानिस्तान के पड़ोसी मध्य एशिया के नये राज्य जो सोवियत संघ के विघटन के उपरान्त अस्तित्व में आए तालिबान विरोधी रुख अपनाते हैं । तालिबान की सफलता और उनका उत्तरी अफगानिस्तान में पहुंचना इन राज्यों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है । अत: इन राष्ट्रों ने तालिबान की सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की ।
Essay # 8. तालिबान का पतन और अफगानिस्तान में शान्ति की स्थापना:
11 सितम्बर, 2001 को अमरीका के दो प्रमुख शहरों व्यापारिक राजधानी न्यूयार्क तथा राजनीतिक राजधानी वाशिंगटन डी. सी. के दो महत्वपूर्ण ठिकानों पर आतंकवादी हमले किये गये । इन हमलों में विश्व व्यापार केन्द्र के दोनों टावर ढह गये तथा पेंटागन के विशाल क्षेत्रफल में बने पांच मंजिला भवन के एक हिस्से को भारी नुकसान हुआ ।
इन हमलों में मुख्य संदिग्ध के रूप में अफगानिस्तान में रह रहे सऊदी आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की पहचान की गई । संयुक्त राज्य अमरीका ने तालिबान सरकार से अपील की कि वह लादेन को उसके सुपुर्द कर दे किन्तु तालिबान सरकार ने अमरीका की सभी अपीलों को ठुकरा दिया ।
लादेन को सौंपने की तमाम अपीलें निष्फल सिद्ध होने पर अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली । अमरीका ने अपनी लड़ाई को लादेन तक ही सीमित न रखते हुए इसे ‘आतंकवाद के विरुद्ध अनंत जंग’ बताया ।
अमरीका इस मामले में सीधे युद्ध में कूदने के स्थान पर अफगानिस्तान के उत्तरी गठबंधन को मजबूत करके तालिबानों को सत्ताच्युत करने व लादेन को गिरफ्तार करने की रणनीति अपनाने को अधिक उपयुक्त मानने लगा । इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तरी गठबंधन एवं तालिबान के बीच लड़ाई तेज हो गई तथा इस लड़ाई में उत्तरी गठबंधन का पलड़ा भारी हो गया ।
अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर, 2001 से शुरू की गई सैन्य कार्यवाही के कारण लगभग दो माह में तालिबानी शासन का अंत हो गया तथा देश के अधिकांश भाग पर उत्तरी गठबंधन का नियन्त्रण स्थापित हो गया । अफगानिस्तान के अधिकांश भाग पर तालिबानी नियन्त्रण समाप्त होने के बावजूद तालिबानों के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद उमर व आतंकवादी सरगना ओसामा बिन लादेन का कुछ भी पता नहीं लग सका ।
तालिबानी शासन के पतन के पश्चात् अफगानिस्तान में वैकल्पिक सरकार के गठन के प्रयास प्रारम्भ किये गये । इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में चार प्रमुख अफगानी गुटों का एक सम्मेलन नवम्बर 2001 के अन्तिम सप्ताह में जर्मनी में बीन के पीटरबर्ग कान्फ्रेंस सेण्टर में आहूत किया गया ।
27 नवम्बर, 2001 को प्रारम्भ हुए इस सम्मेलन में उत्तरी गठबंधन अफगानिस्तान के पूर्व नरेश जहीरशाह (रोम गुट) साइप्रस (ईरान) व पेशावर (पाकिस्तान) में रह रहे विस्थापितों के क्रमश: साइप्रस व पेशावर गुट ने भाग लिया । पर्यवेक्षक की हैसियत से सम्मेलन में भाग लेने वाले 17 राष्ट्रों में अफगानिस्तान के सीमावर्ती राष्ट्रों व सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त टर्की भारत व मेजबान जर्मनी शामिल थे ।
बॉन समझौते के परिणामस्वरूप 22 दिसम्बर, 2001 को 44 वर्षीय पख्तून नेता हामिद करजई ने अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार की बागडोर संभाल ली । विगत 28 वर्षों में यह पहला अवसर था जब अफगानिस्तान में सत्ता का हस्तान्तरण शांतिपूर्ण तरीके से हुआ ।
नई अंतरिम सरकार में शामिल मन्त्रियों में सर्वाधिक मंत्री उत्तरी गठबन्धन से लिए गए । अफगानिस्तान में नई अंतरिम सरकार के सत्तासीन होने के साथ ही ब्रिटेन के नेतृत्व वाली अन्तर्राष्ट्रीय शांति सेना वहां तैनात कर दी गई । दिसम्बर, 2004 में हामिद करजई अफगानिस्तान के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने । तालिबान के कट्टरपन्थी शासन के अन्त के पांच वर्ष बाद भी अफगानिस्तान में पूरी तरह शान्ति कायम नहीं हो सकी है ।
Essay # 9. अफगानिस्तान में अराजकता और अशान्ति:
अफगानिस्तान को तालिबानी हिंसा और विश्व समुदाय की उपेक्षा से मुक्ति नहीं मिल पा रही है । अगस्त, 2006 के तीसरे सप्ताह में नाटो और तालिबान लड़ाकुओं के बीच हुई जंग में लगभग अस्सी आतंककारियों की मौत हो गई । इसे पिछले पांच वर्षों में सबसे खूनी संघर्ष माना जा रहा है । पिछले कुछ दिनों से दक्षिण अफगानिस्तान में अफगानी सेनाओं और आतंककारियों के बीच घमासान हो रहा है ।
वर्ष 2005 से ही यह संकेत मिल रहे थे कि तालिबान संगठित हो रहा है । इस वर्ष आतंककारी हिंसा में हुई वृद्धि ने यह साफ कर दिया कि पांच वर्ष की उपस्थिति के बाद भी अन्तर्राष्ट्रीय सेना अलगाववादी ताकतों की कमर तोड़ पाने में पूरी तरह विफल रही ।
पहले काबुल को देश का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब वहां आतंककारियों द्वारा आईईडी का इस्तेमाल आम बात है । करजई सरकार की ताकत सिमटती सी लग रही है । एक अनुमान के अनुसार, दक्षिण अफगानी क्षेत्रों में तालिबान अपने लगभग बारह हजार लड़ाकुओं की मदद से नाटो को टक्कर दे रहा है ।
सितम्बर, 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किये गये एक अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2000 के बाद से आत्मघाती हमलों में सात गुना वृद्धि हुई हे । अफगानिस्तान की इस बदतर हालत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भी कम दोषी नहीं है । अगर दानदाताओं ने वहां अधिक धन और संसाधनों का विनियोग किया होता तो अफगानिस्तान की कहानी कुछ और ही होती ।
आरम्भ से ही अमरीका ने यहां कम से कम सैनिक उपस्थिति रखने पर जोर दिया । इराक में उलझने के बाद तो ऐसा लगा कि अमरीका अफगानिस्तान को भूल चुका है । अफगानिस्तान को तालिबान से निजात दिलाने और सुरक्षा बहाल करने के लिए लगभग दो लाख सैनिकों की जरूरत का अनुमान लगाया गया था ।
आज अफगानिस्तान और अन्तर्राष्ट्रीय सैनिकों को मिलाकर भी लगभग सवा लाख सैनिकों का आकड़ा पार नहीं किया जा सका है । अमरीकी फौजों ने अफगानिस्तान की स्थानीय जनता को विश्वास में लेने का भी कोई प्रयास नहीं किया, बेगुनाह नागरिकों पर हवाई मामलों और यातनागृहों के संचालन ने भी कट्टरपन्थी ताकतों को ही मजबूत किया ।
वर्ष 2006 में लगभग दो हजार आतंककारी अफगानी सैनिक और विदेशी सैनिक मारे जा चुके हैं । अगर सेना की बात करें तो इस समय नाटो के लगभग 47,000 हजार सैनिक अफगानिस्तान में तैनात हैं । नाटो ने वर्ष 2003 में यहां कदम रखा था । इनमें से अधिकांश सैनिक ब्रिटेन कनाडा और हॉलैण्ड के हैं ।
इन सेनाओं का रिकॉर्ड बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है । अब तक नाटो का मुख्य एजेन्डा कम से कम जोखिम लेने का रहा है लेकिन बहुत जल्द अन्तर्राष्ट्रीय सेना की कमान नाटो के हाथ में आने वाली है । नाटो की विफलता की एक बड़ी वजह यह भी है कि वह अपने-अपने देशों की नीतियों से बंधी हुई हैं ।
उदाहरण के लिए स्पेन ने अपने विमान में अफगानियों की यात्रा पर प्रतिबन्ध लगा रखा है वहीं जर्मनी ने अपनी फौजों को अंधेरे में चल चिकित्सा इकाई के बिना कैम्प से निकलने पर पाबन्दी लगा रखी है । अमरीकी फौज और नाटो के बीच समन्वय का अभाव भी तालिबान को लाभ पहुंचा रहा है ।
नाटो फौजों के पास पर्याप्त संख्या में हैलिकॉप्टरों का भी अभाव है । इसके अलावा तालिबान ताकतों ने देश के बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं को निशाना बना कर नाटो का काम और मुश्किल कर दिया है । वर्ष 2006 में लगभग 70 गठबन्धन सैनिक मारे गये जिनमें से अधिकांश अमरीकी हैं ।
अमरीका ने तो अपने 2,500 सैनिक अफगानिस्तान से हटाने की भी घोषणा की तथापि तालिबानी हमलों की आशंका में फरवरी 2007 में अमरीकी सैनिकों की संख्या वहां बढ़ाकर 26 हजार कर दी गई; इससे पूर्व 2006 में 22-23 हजार अमरीकी सैनिक वहां तैनात थे ।
इराक में अलगाववादी हिंसा में हुई बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया में हिज्बुल्ला-इजरायल तनाव के माहौल में अफगानिस्तान के प्रति अमरीकी प्रतिबद्धता शक के घेरे में आ चुकी है । पश्चिमी देशों में भी विपक्षी दल अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी की लगातार मांग कर रहे हैं ।
पुनर्निर्माण के लिए जितना धन अफगानिस्तान को मिलना चाहिए था वह भी उसे नहीं मिल पाया । दखल के शुरुआती दौर में हुई उपेक्षा ने हालात को और विस्फोटक बना दिया । एक अध्ययन के अनुसार पुनर्निर्माण कार्यों के लिए बोस्निया को प्रति व्यक्ति 680 डॉलर कोसोवो को प्रति व्यक्ति 526 डॉलर सहायता अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दी गई थी जबकि अफगानिस्तान को प्रति व्यक्ति केवल 57 डॉलर मिले ।
वैसे जनवरी, 2007 में लन्दन में एक अहम बैठक हुई थी जिसमें अफगानिस्तान पर चर्चा की गई । लगभग साठ दानदाता देशों ने इस बैठक में भाग लिया । अगले पांच वर्षों तक अफगानिस्तान को सैनिक और पुनर्निर्माण सहायता जारी रखने का निर्णय इस बैठक में किया गया था ।
अब तक अन्तर्राष्ट्रीय सहायता का अधिकांश भाग सुरक्षा पर खर्च किया गया है जिससे पुनर्निर्माण कार्यों की उपेक्षा हुई है । अफगानी सेना को प्रशिक्षण देने का काम भी आसान नहीं है । वहां की पुलिस भी क्षेत्रीय स्तर पर संगठित है जिससे स्थानीय क्षत्रपों का पुलिस पर काफी प्रभाव रहता है ।
Essay # 10. अफगानिस्तान पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (काबुल : जुलाई 2010):
अफगानिस्तान में स्थायित्व एवं विकास संबंधी मुद्दों की समीक्षा के लिए उसकी सहायता करने वाले देशों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 20 जुलाई, 2010 को काबुल में संपन्न हुआ । सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान-की मून तथा अफगान राष्ट्रपति हमीद करजई की संयुक्त मेजबानी में आयोजित हुआ जिसमें भाग लेने वालों में अमरीका, पाकिस्तान, भारत एवं ईरान के विदेश मंत्री शामिल थे ।
वर्ष 2014 तक अफगानिस्तान सरकार को…अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपने की वैश्विक नेताओं की चर्चा के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस.एम.कृष्णा ने कहा कि युद्ध प्रभावित इस देश में स्थिरता लाने की कोई भी नई प्रक्रिया पूरी तरह अफगानिस्तान के नेतृत्व में और उसी के स्वामित्व के अन्तर्गत होनी चाहिए ।
अफगान राष्ट्रपति ने वर्ष 2014 तक विदेशी सेनाओं की पूर्ण वापसी का लक्ष्य प्रस्तावित किया तथा इसके लिए 2011 से वापसी शुरू करने का आह्वान किया । नाटो महासचिव एडर्स फांग रासमुसेन ने कहा कि किसी भी स्थिति में तालिबानों को अफगानिस्तानी सरकार को अपदस्थ नहीं करने दिया जायेगा ।
2014 में अफगानिस्तान से नाटो सेनाओं की वापसी के बाद भी अमेरिका अगले दस वर्ष तक वहां बना रहेगा । राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मई, 2012 में अफगानिस्तान की अचानक यात्रा करके अफगानी राष्ट्रपति करजई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें नाटो सेनाओं की वापसी के बाद भी अमरीकी मौजूदगी का प्रावधान है ।
जुलाई, 2012 में अफगानिस्तान के साथ सामरिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करते हुए अमरीका ने उसे ‘महत्वपूर्ण गैर-नाटो सहयोगी’ (Major Non-Nato Ally) का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की । इससे वर्ष 2014 में अमरीका कें नेतृत्व वाले नाटो बलों की अफगानिस्तान से वापसी के बाद दोनों देशों के सामरिक सम्बन्धों और सहयोग को बल मिलेगा ।
अफगानिस्तान में मार्च, 2011 में शुरू हुई सैन्य हस्तान्तरण प्रक्रिया का पांचवां चरण 18 जून, 2013 को उस समय पूरा हुआ जब नाटो बलों ने शेष बचे 95 जिलों की सुरक्षा व्यवस्था अफगान बलों को सौंप दी । नाटो बल के लगभग 97 हजार सैनिक अफगानिस्तान में तैनात रहे इनमें 50 देशों के सैनिक शामिल हैं जिनमें सर्वाधिक लगभग 68 हजार सैनिक अमरीका के हैं । इन सभी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी वर्ष 2014 के अन्त तक हो गई ।
अफगानिस्तान में स्थायित्व के लिए ‘हार्ट ऑफ एशिया’ सम्मेलन (8-9 दिसम्बर, 2015):
आतंकवाद के खात्मे और अफगानिस्तान में स्थायित्व लाने के लिए निकट आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने की सदस्य देशों की प्रतिबद्धता के साथ 8-9 दिसम्बर, 2015 को पांचवां ‘हार्ट ऑफ एशिया’ सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित किया गया ।
इस दो दिवसीय बहुपक्षीय सम्मेलन में 14 सदस्य देशों, 17 सहयोगी राष्ट्रों के मन्त्री तथा 12 संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए । सम्मेलन में इस्लामाबाद घोषणापत्र को स्वीकृति दी गई जिसमें सभी अफगान तालिबान समूहों से बातचीत की प्रक्रिया में शामिल-होने का आह्वान किया गया है ।
इस्लामाबाद घोषणापत्र के उन प्रमुख बिन्दुओं को साझा किया जिनमें भागीदारी करने वाले प्रतिनिधियों ने एक-दूसरे की सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता, एकता और राजनीतिक स्वतन्त्रता का सम्मान करने तथा एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में दखल नहीं देने के सिद्धान्तों का अनुसरण करने पर जोर दिया गया है । अफगानिस्तान एवं इस क्षेत्र के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा है और इस समस्या से निपटने के लिए साझा प्रयास की जरूरत है ।
ADVERTISEMENTS:
इस्लामाबाद घोषणापत्र में दोहराया गया कि आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद तथा इनमें आपस के जुड़ाव से कई देशों, क्षेत्रों एवं इसके बाहर के लिए भी गम्भीर चुनौती पैदा हुई है जिसका ठोस प्रयास के द्वारा हल किया जाना जरूरी है । सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान को आवश्यक आर्थिक सहायता देने के लिए आश्वस्त किया ।
अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की स्थिति एवं नाटो का नया मिशन:
1 जनवरी, 2015 को नाटो की अन्तर्राष्ट्रीय सेना का युद्धक मिशन ‘प्रशिक्षण और सहयोग’ मिशन में बदल गया है । अफगानिस्तान में नाटो का नया मिशन गैर-सैन्य यानी नागरिक कमान के अन्तर्गत कार्यरत रहेगा और उसका उद्देश्य अफगान सुरक्षा संस्थानों को हिदायत देना होगा ।
पिछले 13 वर्ष में अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, वह बहुत अच्छा नहीं रहा, जिसमें 25,000 अफगान नागरिक मारे गए और साथ ही संयुक्त सेना को भी 3500 जवानों को खोना पड़ा है । अफगानिस्तान युद्ध पर अमेरिका ने 1,000 अरब डॉलर खर्च किए ।
वर्ष 2014 में सबसे ज्यादा खूनखराबा हुआ और 6,000 अफगान सैनिक तथा 3,100 नागरिकों की जान गई । जर्मनी ने अमेरिका सहित दूसरे नाटो देशों की तरह अपने लड़ाकू दस्तों को 2014 के अन्त में अफगानिस्तान से हटा लिया था । अब अफगान सैनिकों के प्रशिक्षण में मदद दे रहे सैनिक ही मौजूद हैं । बाद के समय में अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अभी उसकी सेनाएं अफगानिस्तान से नहीं हटेंगी ।