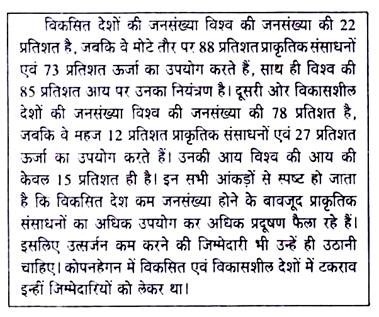ADVERTISEMENTS:
Here is an essay on ‘North-South Relation’ especially written for school and college students in Hindi language.
पिछले दो दशक से ‘नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था’ (New International Economic Order- NIEO) की स्थापना का सपना देखा जा रहा है । इस सपने को साकार करने के लिए दो प्रकार से प्रयत्न हुए- एक तो अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित कर जिसे ‘उत्तर-दक्षिण संवाद’ कहते हैं और दूसरा, गरीब विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग स्थापित कर जिसे ‘दक्षिण-दक्षिण सहयोग’ कहते हैं ।
उत्तर-दक्षिण संवाद: अभिप्राय:
भूगोलवेत्ताओं के अनुसार हमारी पृथ्वी दो गोलार्द्धों में विभाजित है- उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध । उत्तरी गोलार्द्ध में अधिकांशतया उत्तरी अमेरिका और यूरोप का क्षेत्र आता है तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का क्षेत्र आता है ।
उत्तरी गोलार्द्ध में उन्नत, समृद्ध, विकसित और औद्योगिक देश अधिक हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में निर्धन, पिछड़े, विकासशील और शोषित देश अधिक हैं । आगे चलकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शब्दावली में जब ‘उत्तर’ (North) और ‘दक्षिण’ (South) ‘संवाद’ (Dialogue) शब्दबन्ध का प्रचलन हुआ तो इसके स्पष्ट मायने थे ।
‘उत्तर’ से तात्पर्य था- पश्चिमी विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है, जिन्होंने तकनीकी एवं औद्योगिक क्षेत्र में चहुंमुखी प्रगति कर ली है, जहां बचत एवं पूंजी निर्माण की दर काफी ऊंची है और जहां राजनीतिक एवं वित्तीय स्थिरता है ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी आदि ‘उत्तर’ के देश माने जाते हैं । इसके विपरीत ‘दक्षिण’ में अधिकांशतया वे देश हैं जिन्हें ‘विकासशील’ तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है । इन देशों की विशेषताएं हैं- पूंजी की कमी, जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, तकनीकी ज्ञान का अभाव एवं रूढ़िवादिता । ‘संवाद’ से अभिप्राय है ‘परस्पर विचार-विमर्श’ ।
उत्तर-दक्षिण संवाद: पृष्ठभूमि:
‘उत्तर’ के देश लम्बे समय तक औपनिवेशिक शक्तियां रहे । वहां औद्योगिक क्रान्ति पहले हुई अतः 17वीं और 18वीं शताब्दी में इन देशों ने ‘दक्षिण’ के देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया । लम्बे समय तक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश गुलाम रहे । गुलामी की इस लम्बी कालावधि में ‘उत्तर’ के विकसित देशों ने अपनी आर्थिक व्यवस्था इन पिछड़े देशों पर थोप दी ।
ADVERTISEMENTS:
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ‘दक्षिण’ के अधिकांश देश राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो गए किन्तु उन्होंने यह पाया कि आर्थिक दृष्टि से वे पूंजीवादी देशों के शिंकजे में फंसे हुए हैं; विश्व अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका है जो विकासशील देशों के हित में नहीं है ।
उन्होंने यह पाया कि ‘दक्षिण’ के विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 73.9 प्रतिशत है, जबकि विश्व के कुल उत्पादन में उनका हिस्सा मात्र 21.5 प्रतिशत है। इसके विपरीत, उत्तर के विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का महज 26.4 प्रतिशत है जो विश्व के कुल उत्पादन के 78.5 प्रतिशत का भागी है ।
विकासशील राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय 730 डॉलर है, जबकि उत्तर के विकसित राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय 10,720 डॉलर है । ‘दक्षिण’ के विकासशील देश यह भी महसूस करने लगे कि आर्थिक सहायता के नाम पर ‘उत्तर’ के समृद्ध देश उनकी सहायता नहीं करते अपितु ऐसा व्यूह तैयार कर देते हैं जिसमें उत्तरोत्तर विकासशील देशों पर ऋण बढ़ता जाता है ।
विकसित देशों के उदासीनतापूर्ण दृष्टिकोण के कारण विकासशील देशों की व्यापार शर्तें प्रतिकूल होती गयीं तथा विश्व के कुल व्यापार में उनका सापेक्ष भाग कम होता चला गया । जहां 1950 में विश्व के कुल निर्यात का 20 प्रतिशत विकासशील देशों से प्राप्त होता था, 1975 तक यह अनुपात गिरकर 11 प्रतिशत रह गया । इसके विपरीत, इस अवधि में विश्व के कुल निर्यात में विकसित देशों का अंश 61 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गया ।
ADVERTISEMENTS:
1973 के अन्त में पेट्रोल के मूल्यों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप बड़े औद्योगिक देशों का उत्पादन 1974 में कम है । इसके फलस्वरूप 1975 में विकासशील देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं की मांग व इनकी कीमतों में भी कमी हुई ।
कॉफी तथा खोपरे के निर्यात मूल्यों में 70 प्रतिशत की, शक्कर की कीमत में 66 प्रतिशत की, कोको के बीजों में 50 प्रतिशत की, प्राकृतिक रबर की कीमतों में 40 प्रतिशत की, जूट में 40 प्रतिशत की तथा कपास की कीमतों में 16 प्रतिशत की कमी हुई ।
इसके विपरीत, इन देशों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं विशेषतः एवं उससे निर्मित वस्तुओं- कागज, इस्पात, मशीनों, खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गयीं । इनके फलस्वरूप इन देशों के विदेशी व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो गयीं ।
एक ओर प्रतिकूल व्यापार की शर्तें और दूसरी और बढ़ता हुआ ऋण प्रभाव-दोनों ने ‘दक्षिण’ के विकासशील देशों के भुगतान संतुलन को प्रतिकूल बना दिया । 1973 में गैर-तेल निर्यातक विकासशील देशों की ऋणात्मक भुगतान बाकी 900 करोड़ डॉलर थी, जो, 1974 एवं 1975 में क्रमश: 2,800 करोड़ डॉलर तथा 3,500 करोड़ डॉलर हो गयी ।
1984 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में स्पष्ट इंगित किया गया कि ‘दक्षिण’ के देश ऋण के भार से अत्यधिक दबे हुए हैं । दक्षिण राज्यों के ऋण भार का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जहां 1980 में यह 69 बिलियन डॉलर था, वहां 1982 में यह बढ़कर 98 बिलियन डॉलर हो गया ।
विकासशील देशों के मुद्रा भण्डार में वर्ष 1986 में 16.8 प्रतिशत की गिरावट आयी जबकि 1985 में यह गिरावट मात्र 5.3 प्रतिशत थी । इसके विपरीत, औद्योगिक देशों के मुद्रा भण्डार में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । विकासशील देशों का व्यापार घाटा निर्यात घटने के कारण 1986 में तिगुने से भी अधिक हो गया ।
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार 62 विकासशील देशों का कुल निर्यात इस अवधि में 480 अरब डॉलर का रहा और आयात 501 अरब डॉलर का । इस प्रकार लगभग 21 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ जबकि 1985 में यह घाटा मात्र 6 अरब डॉलर था । दूसरी ओर गैर-साम्यवादी औद्योगिक देशों के व्यापार में फिर वृद्धि हुई । यह लगभग 30 खरब डॉलर तक पहुंच गयी ।
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वित्तीय संस्थान प्रतिवर्ष विकासशील देशों को जितना ऋण देते हैं उससे कहीं अधिक वे ब्याज और भुगतान के रूप में वसूलते हैं । ‘विश्व विकास आन्दोलन’ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक ने वर्ष 1992 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को कुल 3 अरब डॉलर का ऋण दिया परन्तु ऋण के ब्याज और भुगतान के उपरान्त इन देशों को वस्तुत: मात्र 88 करोड़ 50 लाख डॉलर ही प्राप्त हो सके । इन वित्तीय संस्थानों की इस नीति के कारण ऋण का उद्देश्य ही समाप्त हो रहा है ।
1964 से 1967 तक व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते (GATT) के अन्तर्गत विकसित एवं विकासशील (ऊत्तर-दक्षिण) देशों के बीच विचार-विमर्श होता रहा परन्तु विकासशील देशों के निर्यात व्यापार के विस्तार हेतु कोई ठोस सुझाव स्वीकार नहीं किए गए ।
विकासशील देशों में से कुछ ने तो यहां तक कहना प्रारम्भ कर दिया कि वे आर्थिक सहायता की अपेक्षा निर्यात वृद्धि हेतु विकसित देशों से रियायतें प्राप्त करना अधिक उपयुक्त मानते हैं । इन देशों की यह शिकायत थी कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौते (GATT) के अन्तर्गत आयोजित मन्त्रणाओं पर धनी एवं विकसित देशों का वर्चस्व रहता है और ये देश विकासशील देशों से आने वाली वस्तुओं पर विद्यमान प्रतिबन्धों में किसी प्रकार की रियायत करने को तैयार नहीं हैं ।
उत्तर-दक्षिण संवाद के लिए दबाव:
1970 के दशक के प्रारम्भ में विकासशील देश इस बात पर जोर देने लगे कि आर्थिक सम्बन्धों का निर्धारण न्याय और लोकतान्त्रिक आदर्शों पर किया जाना चाहिए । संयुक्ता राष्ट्र महासभा ने मई 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में ‘नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था’ हेतु घोषणा एवं कार्यक्रम का मसौदा पारित किया ।
तबसे विभिन्न मंचों, जैसे – अंकटाड सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, आदि के माध्यम से दक्षिण के विकासशील देश विश्व अर्थव्यवस्था के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की मांग करने लगे । उत्तर के विकसित औद्योगिक देशों ने भी हवा के रुख को पहचानते हुए यह महसूस किया कि यह बुद्धिमानी नहीं होगी कि विकासशील देशों की उचित मांगों को अनदेखा किया जाए ।
विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट चलने से दीर्घावधि में हर हालत में विकसित देशों पर भी बुरा असर पड़ेगा । अत: अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों और अन्तत: विश्व शान्ति के समान विकास के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इन प्रस्तावित मुद्दों को धनी और निर्धन देशों के बीच व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श के जरिए सन्तोषजनक तरीके से हल किया जाए ।
संयुक्त राष्ट्र महासभा, अंकटाड, निर्गुट शिखर सम्मेलनों, प्रसिद्ध ब्रांट आयोग (पश्चिम जर्मनी के चांसलर विली ब्रांट की अध्यक्षता में, जिसमें ओलोफ पाल्म और एडवर्थ हीथ जैसे पश्चिम-यूरोपीय राज नेताओं ने भाग लिया) और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन तिनबर्गेन जैसे अग्रणी आर्थिक विचारकों ने इन वर्षों में सिफारिश की कि धनी और निर्धन देशों (उत्तर-दक्षिण के देश) के बीच शीघ्र और व्यापक विचार-विमर्श कराया जाए या फिर ‘नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था’ को लागू करने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श कराया जाए ।
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अपनी 1985 की रिपोर्ट में औद्योगिक राष्ट्रों से संरक्षणवाद को बढ़ने से रोकने तथा वर्तमान व्यापार व्यवधानों को हटाने को कहा ताकि विकासशील देशों के बाजार का विकास हो सके ।
मुद्रा कोष ने चेतावनी दी कि विदेशी व्यापार नीति ऐसा क्षेत्र है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सबसे गम्भीर खतरा है । औद्योगिक राष्ट्रों का यह विशेष उत्तरदायित्व है कि वे व्यापार-क्षेत्र को उदार बनाने के लिए प्रयत्न करें ।
उत्तर-दक्षिण संवाद: कतिपय प्रयत्न:
उत्तर-दक्षिण संवाद की दृष्टि से निम्नलिखित प्रयत्न उल्लेखनीय हैं:
1. पेरिस सम्मेलन, 1975-77,
2. ब्रांट आयोग, 1977,
3. कानकुन सम्मेलन, 1981,
4. उरुग्वे वार्ता, 1986-93 एवं विश्व व्यापार संगठन,
5. पृथ्वी सम्मेलन, जून 1992 एवं जून 1997,
6. जी-8 की एवियान (फ्रांस) में सम्पन्न वार्षिक बैठक (जून, 2003),
7. जी-20,
8. जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन एवं पेरिस सम्मेलन ।
1. पेरिस सम्मेलन, 1975-77 (Paris Conference, 1975-77):
महासभा द्वारा नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की घोषणा के एक वर्ष के भीतर अमरीका ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के बारे में सम्मेलन बुलाए जाने की दिशा में पहल शुरू कर दी और यह दिसम्बर, 1975 में पेरिस में आरम्भ हुआ ।
पेरिस सम्मेलन को ‘अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन’ के नाम से भी जाना जाता है । इस सम्मेलन के आयोजन में तत्कालीन अमरीकी विदेश सचिव डॉ. हेनरी किसिंजर ने विशेष दिलचस्पी ली । संयुक्त राष्ट्र महासभा की सातवीं विशेष बैठक को सम्बोधित करते हुए डॉ. किसिंजर ने विकसित और विकासशील देशों का सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया ।
कुल 8 विकसित और 19 विकासशील देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया । इस सम्मेलन का विचार-विमर्श बीच-बीच में रुक कर हुआ और लगभग 18 महीने तक चलता रहा । सम्मेलन जून, 1977 में समाप्त हुआ । उत्तर के समृद्ध देशों ने निर्धन देशों (दक्षिण के देशों) के लिए कुछ रियायतें और सहायता कार्यक्रमों की घोषणा की जिनमें गरीब देशों की तेल की जरूरतों पर बढ़ते खर्च को देखते हुए और जिंस मूल्यों को स्थिर करने में मदद के लिए गरीब देशों की सहायता के उद्देश्य से एक विशेष क्रोष की स्थापना करना भी शामिल था ।
इसके बदले में 1973 के कथित तेल संकट की मार से पीड़ित औद्योगिक देशों ने स्थिर मूल्यों पर तेल की सप्लाई की गारण्टी की मांग रखी । देखा जाए तो उत्तर के धनी देश थोड़ी-सी सहायता की बहुत बड़ी कीमत मांग रहे थे, अत: तेल निर्यातक देशों ने इसे सीधे अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार पेरिस सम्मेलन अर्थशून्य हो गया ।
2. ब्रांट आयोग, 1977 (Brant Commission, 1977):
पेरिस सम्मेलन की असफलता के बाद विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों को निपटाने के लिए एक गैर-सरकारी स्वतन्त्र आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया । प्रस्तावित गैर-सरकारी आयोग ने दिसम्बर 1977 में काम करना शुरू कर दिया ।
यह आयोग ब्रांट आयोग के नाम से लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसके अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चान्सलर विली ब्रांट थे । इसके सदस्यों में विश्व के सभी भागों के राष्ट्र शामिल थे – पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण । भारतीय अर्थशास्त्री डॉ. एल.के.झा आयोग के सदस्य थे । ब्रांट आयोग के नाम से लोकप्रिय इस प्रस्तावित आयोग की पहली बैठक दिसम्बर, 1977 में बोन में विली ब्रांट की अध्यक्षता में हुई ।
इसकी दो रिपोर्ट सामाजिक विकास समस्याओं के बारे में सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती हैं । इन रिपोर्टों को ‘नार्थ-साउथ-ए प्रोग्राम फार सर्वाइवल’ (North-South: A Programme for Survival) और ‘कॉमन क्राइसिस’ (Common Crisis) शीर्षक से जाना जाता है ।
इनके अतिरिक्त यह प्रामाणिक दस्तावेज ‘परस्पर-निर्भरता’ के प्रसिद्ध सिद्धान्त के लिए भी जाना जाता है जिसमें ‘विकसित और विकासशील देशों’ (उत्तर-दक्षिण संवाद) की परस्पर-निर्भरता का विश्लेषण है । आयोग ने जोर देकर यह स्पष्ट किया था कि विश्व शान्ति के लिए विकसित और विकासशील देशों में ‘परस्पर-निर्भरता’ जरूरी है ।
इसके लिए आयोग ने ‘विश्व के नेताओं की अनौपचारिक बैठक’ बुलाने का प्रस्ताव किया ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच विभाजन से सम्बद्ध मुद्दों; जैसे – सहायता, व्यापार, वित्तीय प्रवाह, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी का स्थानान्तरण और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का लोकतन्त्रीकरण के बारे में रियायतें, आदि पर स्पष्ट और निर्भीक विचार-विमर्श किया जा सके । इस बैठक को मैक्सिको के राष्ट्रपति ने अपने यहां आयोजित करने का प्रस्ताव किया ।
संक्षेप में, ब्रांट आयोग ने उत्तर-दक्षिण संवाद पर जोर देते हुए निम्नलिखित मुद्दों पर सुझाव दिए:
a. वस्तु व्यापार,
b. विकासशील देशों के लिए विदेशी कर्जे,
c. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार,
d. टेक्नोलॉजी हस्तान्तरण,
e. बहुराष्ट्रीय निगम,
f. समुद्री कानून तथा
g. बहु-उद्देश्यीय व्यापार ।
3. कानकुन सम्मेलन, 1981:
मैक्सिको के राष्ट्रपति की पहल पर भारत सहित 22 देशों ने मैक्सिको के कानकुन शहर में उत्तर-दक्षिण संवाद के लिए गरीब-अमीर राष्ट्रों का एक लघु शिखर सम्मेलन (अक्टूबर, 1981) आयोजित किया ।
इस बैठक का उद्देश्य अमीर-गरीब देशों के मसलों पर अन्तर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श के लिए उचित वातावरण बनाना और इस विचार-विनिमय के रास्ते की अड़चनें समाप्त करना था ।
विकासशील देशों ने इस बात पर जोर दिया कि विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे में व्यापक परिवर्तन किया जाए ताकि बदलती परिस्थितियों में वे अपने दायित्व का अच्छी तरह पालन कर सकें । इस प्रस्ताव का अमीर देशों ने कड़ा विरोध किया और प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । अमीर देशों का कहना था कि इन दोनों संगठनों के ढांचे के परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्णय अन्तिम हो ।
अमीर देश विश्व बैंक और मुद्रा कोष पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं । वर्तमान व्यवस्था यह है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमरीकी नागरिक होगा और मुद्राकोष का डायरेक्टर पश्चिमी यूरोप का नागरिक होगा ।
कुछ पश्चिमी देशों के पास इन दोनों संस्थाओं के निर्णय पर वीटो के प्रयोग का भी अधिकार है । इसी कारण वे इन दोनों संस्थाओं के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं चाहते । इस शिखर वार्ता में खाद्यान्न, भुखमरी, कृषि विकास, व्यापार व ऊर्जा पर भी विस्तार से विचार किया गया ।
विकासशील देशों के निर्यात से जुड़ी समस्याओं के सन्दर्भ में भारत की ओर से एक पांच-सूत्री योजना इस शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत की गयी । यह सम्मेलन के दस्तावेजों में सम्मिलित तो कर ली गयी लेकिन अमीर देशों ने इसे कोई खास महत्व नहीं दिया ।
ये पांच सूत्र निम्नलिखित हैं:
a. जिन्सों के आयात-निर्यात के बारे में नए सिरे से समझौते किए जाएं,
b. जिन्सों के भाव स्थिर करने के लिए अंकटाड के तत्वावधान में साझा कोष बनाने की प्रक्रिया को तुरन्त गतिशील बनाया जाए,
c. विकासशील देशों में निर्यात वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की प्रवृति को रोका और घटाया जाए,
d. रेशे सम्बन्धी समझौते के नवीनीकरण के लिए बातचीत जल्द शुरू की जाए,
e. विकासशील देशों के निर्यात पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्धों की समीक्षा का बन्दोबस्त हो और उन्हें एक निर्धारित अवधि में क्रमश: समाप्त किया जाए ।
कानकुन सम्मेलन की समाप्ति पर नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सन्दर्भ में कोई घोषणा नहीं की गयी । गरीब और अमीर देशों के बीच विश्व वार्ता के अगले कदम के सम्बन्ध में नेताओं के बीच सहमति नहीं हो पायी ।
विकासशील, देशों के नेता विश्व वार्ता को सन् 1982 के प्रारम्भ में चाहते थे जिसका अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों ने दृढ़ विरोध किया । डॉ.एल.के.झा के अनुसार, जो कानकुन सम्मेलन में शामिल हुए थे, इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि बस यह आयोजित हो गया ।
धनी देशों के नेताओं, विशेषकर तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति रीगन के दुराग्रही रवैये के कारण कानकुन शिखर सम्मेलन असफल रहा । कानकुन सम्मेलन की विफलता के बाद भी ‘उत्तर-दक्षिण संवाद’ के लिए कुछ प्रयास किए गए ।
इनमें उल्लेखनीय है अंकटाड के तत्वावधान में 1983 में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयार्क में बुलाया गया विश्व नेताओं का सम्मेलन । किन्तु अमरीका की हठधर्मिता तथा कथित जी-7 राष्ट्रों की हठधर्मिता के कारण, ये सभी प्रयास विफल रहे ।
4. उरुग्वे वार्ता, 1986-93 (गैट समझौता) एवं विश्व व्यापार संगठन:
द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अस्तित्व में आई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था मुख्यत: तटकर और व्यापार से सम्बन्धित सामान्य समझौते के प्रावधानों द्वारा संचालित होती है । इस सामान्य समझौते को ‘गैट’ (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) कहते हैं ।
विश्वस्तरीय व्यापार के सम्बन्ध में नियम बनाने का कार्य ‘गैट’ संस्थान द्वारा किया जाता है । ‘गैट’ का मुख्य उद्देश्य, प्रशुल्क दरों को न्यूनतम करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करके पारस्परिक लाभ वाले लक्ष्यों को प्राप्त करना है ।
गैट की स्थापना (1947) से लेकर अब तक आठ बहुपक्षीय व्यापारिक सम्मेलन हो चुके हैं । आठवां अधिवेशन (उरुग्वे राउण्ड) 20 सितम्बर, 1986 को ‘गैट’ के तत्वावधान में दक्षिण अमरीका के देश उरुग्वे में प्रारम्भ हुआ, जिसमें लगभग सौ सदस्य देशों ने भाग लिया था । बाद में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 108 हो गयी । उरुग्वे वार्ता दौर के लिए चार वर्षों की अवधि निर्धारित की गयी थी और गैट को अपने निष्कर्ष दिसम्बर 1990 तक देने थे ।
लेकिन 7 वर्षों के निरन्तर प्रयासों और वार्ताओं के सात दौर सम्पन्न होने के बावजूद भी कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थाओं पर आम सहमति प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल सकी । वार्ता का आठवां दौर उरुग्वे के शहर ‘पुन्ता डेल इस्ते’ में प्रारम्भ हुआ ।
इसमें ‘गैट’ के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों पर निर्णय लिए जाने के सम्बन्ध में वार्ता हुई । परम्परागत रूप से ‘गैट’ केवल वस्तुओं के व्यापार से सम्बन्धित नियम ही बनाता रहा है जिनमें मुख्यत: निर्मित माल ही सम्मिलित है, कृषि इसके कार्य क्षेत्र से बाहर है । उरुग्वे वार्ता के वर्तमान दौर में गत परम्परा से हटकर वार्ता क्षेत्र में विस्तार किया गया तथा पहली बार वार्ता सूची में चार नए क्षेत्रों को शामिल किया गया ।
ये क्षेत्र हैं:
a. व्यापार से सम्बन्धित निवेश उपाय (Trade Related Aspects of Investment Measures-TRIMs),
b. बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार के पहलुओं से सम्बन्धित व्यापार (Trade Related Aspects of Investment Property Rights-TRIPs),
c. सेवाओं में व्यापार (Trade in Services),
d. कृषि (Agriculture) ।
गैट वार्ता की सूची में यह क्षेत्र विकसित देशों के आदेश से शामिल किए गए । विकासशील देशों का विचार था कि गैट केवल अब तक के परम्परागत क्षेत्र में ही नियम बनाने तक अपनी कार्यवाही सीमित रखे । वार्ता सूची के विस्तार के विषय में विकसित देशों (उत्तर) के अपने तर्क थे ।
उनके अनुसार व्यापार से सम्बन्धित निवेश उपायों (TRIMs) को वार्ता सूची में रखा जाना चाहिए क्योंकि विकासशील देश (दक्षिण) विदेशी निवेश को नियन्त्रित करने की नीतियां बनाते हैं जिससे विदेशी कम्पनियों को स्वतन्त्रता से व्यापार करने में बाधा पड़ती है ।
बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, विशेषकर पैटेण्ट, कॉपीराइट तथा ट्रेडमार्क के सम्बन्ध में विकसित देशों का कहना था कि विकासशील देशों में उपर्युक्त अधिकारों के अपर्याप्त संरक्षण के कारण जाली तथा चोरी के व्यापार का प्रचलन हुआ है और वैध व्यापार को क्षति पहुंची है, अत: बौद्धिक सम्पदा अधिकार से सम्बन्धित व्यापार पहलुओं (TRIPs) को वार्ता सूची में शामिल किया जाना चाहिए । विकासशील देशों ने ऐसे प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया ।
उरुग्वे चक्र में पांच वर्ष के वार्ता दौर के पश्चात् भी किसी सर्वसम्मत परिणाम पर पहुंचने में असफल होने पर गैट के महानिदेशक आर्थर डुंकेल (Arthur Dunkel) ने 20 दिसम्बर, 1991 को 108-सदस्यीय गैट के भावी स्वरूप पर 500 पृष्ठ के अपने प्रस्ताव रखे ।
सदस्य राष्ट्रों को सहमति के लिए पहले 13 जनवरी, 1992 तक का समय दिया गया, बाद में इस समय सीमा को 17 अप्रैल, 1992 तक बढ़ा दिया गया । विकासशील देशों (दक्षिण) की दृष्टि में हुंकेल प्रस्तावों का सर्वाधिक नकारात्मक पहलू यह है कि वह केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं हैं, इनमें कृषि सब्सिडी, बौद्धिक सम्पदा अधिकार (पैटेण्ट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आदि), विदेशी निवेश उपायों तथा सेवाओं को भी शामिल कर लिया गया । इस प्रस्ताव में विकासशील देशों की मांगों तथा आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया केवल विकसित देशों के व्यापार प्रसार तथा हितों को ही आगे बढ़ाने की चेष्टा की गयी ।
हुंकेल प्रस्तावों में सर्वाधिक विरोध पैटेण्ट अधिकारों के सम्बन्ध में था जिनमें पैटेण्ट प्राप्तकर्ताओं के अधिकारों में वृद्धि और उनके दायित्वों एवं वैधानिक बन्धनों में कमी की गयी । कृषि के क्षेत्र में पैटेण्ट अधिकार लागू करने की सिफारिश की गयी जिसके लागू हो जाने की दिशा में विकासशील देशों को विकसित देशों से कृषि सम्बन्धी तकनीकी खरीदने के लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा ।
संक्षेप में, डुंकेल प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने से विकासशील देशों के विकास उद्देश्यों पर मूलरूप में विपरीत प्रभाव पड़ेगा । आर्थर डुंकेल ने ऐसे नए नियम प्रतिपादित किए जिनसे ‘गैट’ विकासशील देशों पर ऐसी नीतियां थोप सकेगा कि वह अपने विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे ।
गैट के अधिवेशनों में विकासशील देशों ने अपने व्यापारिक हितों की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा प्रशुल्क कटौती एवं विकसित देशों के प्रतिबन्धात्मक व्यवहार के विरुद्ध इन्होंने अपनी आवाज बुलन्द की । दुर्भाग्यवश, गैट के विभिन्न सम्मेलनों में इन राष्ट्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार ही हुआ और औद्योगिक राष्ट्रों के हितों का ही गैट के अन्तर्गत वर्चस्व स्वीकार किया गया ।
उत्तर के राष्ट्र अपनी समृद्धिशाली स्थिति के कारण अपने राजनीतिक हित सुरक्षित कर लेते हैं तथा फलतः आर्थिक हित सिद्ध करने में भी सफल हो जाते हैं । इसीलिए ‘गैट’ को ‘अमीरों के क्लब’ की संज्ञा दे दी जाए तो उचित ही होगा ।
15 दिसम्बर, 1993 को विश्व के 117 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से नए व्यापार एवं तटकर सामान्य समझौता (गैट) को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी । यह समझौता 1995 से लागू हो गया । इस समझौते के तहत एक नया ”विश्व व्यापार संगठन” (WTO) गठित किया गया । गैट की तुलना में अधिक शक्ति सम्पन्न प्रभावी संगठन के रूप में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई है ।
विश्व व्यापार संगठन विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धों से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया और 1995 में मोरक्को के मर्राकेश में पारित किया गया था ।
यह संगठन ‘गैट’ से भी व्यापक है और यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के वास्ते संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराता है । संगठन असल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी है जो सभी देशों की व्यापार व्यवस्थाओं पर लगातार निगाह रखता है ।
विश्व व्यापार संगठन का प्रति दो वर्ष में एक सम्मेलन होता है । सदस्य देशों के वाणिज्य या व्यापार मन्त्री इसमें भाग लेते हैं । प्रथम सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था, मई 1999 में द्वितीय सम्मेलन जेनेवा में हुआ, 30 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1999 तक तृतीय सम्मेलन सिएटल में, चतुर्थ सम्मेलन दोहा (कतर) में 9-13 नवम्बर, 2001 में, पंचम सम्मेलन कानकुन (मैक्सिको) में 10-14 सितम्बर, 2003 को, छठा मत्रिस्तरीय सम्मेलन हांगकांग (चीन) में 13-18 दिसम्बर, 2005 को, 7वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 30 नवम्बर, 3 दिसम्बर 2009 को जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड); आठवां मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन 15-17 दिसम्बर, 2011 को जेनेवा में, नौवां मत्रिस्तरीय सम्मेलन 3-7 दिसम्बर, 2013 को बाली (इण्डोनेशिया) में तथा 10वां मत्रिस्तरीय सम्मेलन 15-19 दिसम्बर, 2015 को नैरोबी (केन्या) में सम्पन्न हुआ ।
सिएटल सम्मेलन सफल नहीं माना जा सकता क्योंकि कोई सांझी घोषणा जारी नहीं की जा सकी । अमेरिका श्रम एवं पर्यावरण मानकों को विश्व व्यापार संगठन के एजेण्डे में शामिल करना चाहता था जबकि भारत एवं अन्य विकासशील देश इस प्रयास का विरोध करते हुए कह रहे थे कि श्रम मानकों पर अमेरिका इसलिए जोर दे रहा है ताकि विकासशील देशों में बने सस्ते मालों से प्रतिस्पर्द्धा में धनी देशों को बचाया जा सके । भारत ने यूरो-अमेरिकी मन्सूबों को कठघरे में खड़ा किया तथा विकासशील देशों की आवाज का नेतृत्व किया ।
लगभग 75 विकासशील देशों ने पहली बार विश्व व्यापार संगठन को ज्ञापन दिए । सभी देशों में चल रहे स्वदेशी आन्दोलनों ने अपनी-अपनी सरकारों को सावधान व सचेत किया था, समृद्ध देशों के आगे न झुकने का उन पर जबरदस्त दबाव बनाया था ।
फलत: विकासशील देश अमेरिकी हेकड़ी के खिलाफ एकजुट थे । दोहा (कतर) मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन के एजेंडे को स्वीकार किया जाना विकासशील राष्ट्रों के बजाय यूरोपीय संघ एवं अमरीका के लिए ही अधिक लाभदायक माना जा रहा है ।
इस मामले में भारत की आपत्ति चार सिंगापुर मुद्दों को लेकर थी । इनमें विदेशी निवेश व प्रतिस्पर्द्धा नीति के सम्बन्ध में नये वैश्विक नियमों के निर्धारण, सरकारी परियोजनाओं के लिए सामान की खरीद में विदेशी कम्पनियों को अवसर प्रदान करने तथा व्यापारिक नियमों को सरल बनाने के मुद्दे शामिल थे ।
मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन में स्वीकार किए गए दोहा घोषणा-पत्र को भारत ने अपनी सहमति तभी प्रदान की जब सम्मेलन के अध्यक्ष ने यह स्पष्ट घोषणा की कि उपर्युक्त चारों विवादित मुद्दों पर सदस्य राष्ट्रों की सहमति हो जाने पर ही पांचवें मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए बातचीत होगी ।
दोहा सम्मेलन में भारत के नेतृत्व में विकासशील राष्ट्रों को एक बड़ी सफलता जनस्वास्थ्य सम्बन्धी औषधियों के उत्पादन एवं अधिग्रहण के मामले में मिली । एच.आई.वी./एड्स, टी.बी. व मलेरिया आदि रोगों से जन सामान्य की सुरक्षा के लिए औषधियों के उत्पादन के मामले में विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स (TRIPS) एवं पैटेंट सम्बन्धी नियम अब आड़े नहीं आ सकेंगे । जनस्वास्थ्य सम्बन्धी इस प्रावधान को दोहा घोषणा-पत्र में शामिल किया जाना विकासशील राष्ट्रों की एक बड़ी विजय के रूप में देखा गया है ।
हांगकांग सम्मेलन में विकसित देश अपने आग्रह कम करने और कुछ रियायतें देने को तैयार हुए । कृषि क्षेत्र को राज सहायता खत्म करने के साथ औद्योगिक वस्तुओं पर तटकर में कमी पर सहमति बनी और सबसे पिछड़े देशों को सहायता देने का वादा किया गया ।
वस्तुत: हांगकांग (दिसम्बर 2005) में विकासशील देशों की एकजुटता बहुत काम आयी । भारत समेत विकासशील देशों के लिए राहत की बात यह है कि कुछ कृषि उत्पादों को विशिष्ट उत्पाद में शामिल करने के साथ ही इनके लिए विशेष सुरक्षा उपायों को मसौदे में शामिल कर लिया गया । इससे विकासशील देश भाव गिरने पर सुरक्षात्मक उपाय कर सकेंगे ।
पिछले एक दशक से जो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) दुनिया की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों को एक ही ढांचे में ढालने की राह पर अनवरत गति से आगे बढ़ रहा था, उस डब्ल्यू.टी.ओ. की दोहा वार्ता जुलाई 2006 में अनिश्चितकाल तक के लिए अवरुद्ध हो गई ।
अब इस वार्ता को पुनर्जीवित करने में कई महीने या कई साल भी लग सकते हैं । लेकिन, डब्ल्यू.टी.ओ. के जिन समझौतों एवं कानूनों पर सदस्य देशों की सहमति हो चुकी है, उनके अन्तर्गत विश्व व्यापार चलता रहेगा । ऐसे परिदृश्य में विश्व के विकासशील और विकसित देश मुक्त व्यापार संगठनों में तेजी से एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि वे व्यापारिक प्रतियोगिता और प्रशुल्क रणनीतियों का सामूहिक रूप से मुकाबला कर सकें ।
गौरतलब है कि डब्ल्यू.टी.ओ. के अन्तर्गत अमरीका और यूरोपीय समुदाय की स्वार्थपूर्ण गुटबंदी ने जुलाई 2006 तक कृषि एवं औद्योगिक टैरिफ कटौती के लिए फॉर्मूले पर सहमति नहीं होने दी । डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्य देशों ने सब्सिडी सीमा शुल्क में कटौती व्यापार की अन्य बाधाओं को दूर करने तथा विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए 2001 में दोहा दौर की व्यापार वार्ता शुरू की थी । इस वार्ता को वर्ष 2004 में समाप्त होना था, लेकिन सदस्य देशों की विभिन्न सरकारें इस समय सीमा का अनुपालन नहीं कर पाईं ।
इस कारण यह वार्ता आगे बढ़ती रही और पिछले वर्ष दिसम्बर 2005 में हांगकांग में हुई डब्ल्यू.टी.ओ. की बैठक में निर्णय हुआ था कि कृषि और गैर कृषि वस्तुओं के व्यापार में शुल्कों की कटौती के नए समझौते को तैयार कर लिया जाएगा, परन्तु पिछले माह अगस्त 2006 तक ऐसा नहीं हो सका ।
विकसित देशों द्वारा शुल्क कम करने के नए समझौते को अंतिम रूप देने के लक्ष्य को टाले जाने से डब्ल्यू.टी.ओ. की दोहा दौर की बातचीत अनिश्चितकाल तक के लिए रुक गई है । वस्तुत: विश्व व्यापार संगठन की बातचीत में रुकावट के लिए विकसित देश ही जिम्मेदार हैं, जो व्यापार को प्रभावित करने वाली अपनी भारी-भरकम कृषि सब्सिडी में कमी के बदले विकासशील देशों के कृषि और औद्योगिक उत्पादनों के बाजार में अपनी दखल बढ़ाना चाहते हैं ।
5. पृथ्वी सम्मेलन: जून 1992 एवं जून 1997:
रिओ-डी-जेनेरो (ब्राजील) में आयोजित ‘पृथ्वी शिखर सम्मेलन’ (3 जून से 14 जून, 1992) उत्तर और दक्षिण (अमीर एवं गरीब) के देशों में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर मतभेद का एक महत्वपूर्ण नजारा प्रस्तुत करता है ।
विकसित देश (उत्तर) मानते हैं कि गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण ही पृथ्वी की यह हालत हुई है । दक्षिण के गरीब देशों में अभी भी उष्णकटिबन्धीय घने जंगल हैं और अंदेशा है कि अपनी बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए वे इन जंगलों का सफाया कर सकते हैं । विकासशील देशों के अनुसार पश्चिमी देशों की बेलगाम फिजूलखर्ची से ही पृथ्वी प्रदूषित हुई है । ऊर्जा के स्रोतों के अति दोहन को वे पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण मानते हैं ।
रिओ सम्मेलन से पूर्व छ: ऐसे मुद्दे उभर कर सामने आए जिन पर उत्तर-दक्षिण मतभेद था:
a. ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन:
उत्तर के देश 2000 ई. तक कार्बन-डाइ-ऑक्साइड और मिथेन जैसी गैसों के उत्सर्जन में 20 प्रतिशत कटौती चाहते थे जबकि दक्षिण के गरीब देश प्रिछले 50 वर्षों से गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के लिए अमीर देशों को दोषी करार देते हैं और इसमें भारी कटौती चाहते हैं ।
b. वन:
अमीर देश ऐसी कानूनी बाध्यता चाहते हैं जिससे वनों, खासकर उष्णकटिबन्धीय वनों की कटाई पर कडे प्रतिबन्ध लगें । गरीब देशों के अनुसार ऐसा प्रावधान राष्ट्र की प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप माना जाएगा । वनों को अब तक हुए नुकसान की भरपाई मुख्य रूप से अमीर देश करें ।
c. जनसंख्या:
उत्तर के अमीर देश पर्यावरण के निरन्तर विनाश के लिए जनसंख्या विस्फोट और गरीबी को जिम्मेदार ठहराते हैं जबकि दक्षिण के देश अमीर देशों पर संसाधनों के अत्यधिक उपभोग का आरोप लगाते हैं । उनके-अनुसार मुट्ठी भर होने के बावजूद ये देश विश्व के कुल संसाधनों का 75 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा उपभोग करते हैं ।
d. तकनीकी हस्तान्तरण:
अमीर देश तकनीकी विकास को व्यावसायिक मानते हैं और जो देश इसका इस्तेमाल करेंगे उनसे इसकी पूरी कीमत लाभ सहित वसूल की जानी चाहिए । गरीब देश तकनीकी का इस्तेमाल प्रदूषण को साफ करने और ऊर्जा क्षमता में सुधार के लिए करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यह तकनीक गरीब देशों को सस्ती दर पर मिले ।
e. पैसा:
अमीर देश पर्यावरण सुधार के लिए अनिवार्य अनुदान नहीं देना चाहते, उनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां विश्व पर्यावरण एजेंसी या विश्व बैंक पैसे का वितरण करें । गरीब देश पर्यावरण सुधार पर खर्च के लिए नई संस्था का निर्माण चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा विश्व बैंक पर अमीर देशों का नियन्त्रण बना हुआ है ।
f. पर्यावरण विनाश:
अमीर देश औद्योगीकरण और गरीबी को पर्यावरण की तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और खर्च का बोझ बांटना चाहते हैं जबकि गरीब देशों के अनुसार पर्यावरण तबाही के लिए विकसित देश ही जिम्मेदार रहे हैं और अब पर्यावरण को स्वच्छ करने का पूरा खर्च वहन करें ।
रिओ में 3 जून से 14 जून, 1992 तक चलने वाला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन तीन प्रमुख दस्तावेजों को मान्य करने के बाद सन्तोष और आशा के वातावरण में सम्पन्न हो गया । इस महा सम्मेलन में 178 राष्ट्रों की ओर से 115 राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष उपस्थित थे ।
इसमें:
i. एजेण्डा 21 आगामी शताब्दी के लिए विकास तथा पर्यावरण सुधार योजना,
ii. 27-सूत्री रिओ घोषणा-पत्र था,
iii. विश्व के वनों के संरक्षण सम्बन्धी वक्तव्य प्रमुख उपलब्धियां हैं ।
एजेण्डा 21 के लिए पर्याप्त कोष जुटाने जैसे विवादास्पद प्रश्न पर भी सहमति बन सकी, यह सन्तोष की बात है । अनेक देशों ने अपने कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.7 प्रतिशत सरकारी विकास सहायता के रूप में देने का वायदा किया ।
कुछ ने इसका भरोसा दिलाया, कुछ देश इससे अधिक भी योगदान कर सकते हैं । पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित विश्व जैव विविधता सन्धि 29 दिसम्बर, 1993 से प्रभावी हो गयी है । यद्यपि अमरीका ने विविध जैविक सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए और वुडलैण्ड कमीशन द्वारा चाहे गए 10 अरब डॉलर का फण्ड नहीं बन सका पर पर्यावरण की रक्षा को जो महत्व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मिला है वह आशाजनक है ।
जापान ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत की । उसने लगभग एक अरब डॉलर प्रतिवर्ष अगले पांच वर्षों तक देने की घोषणा की । जर्मनी ने लगभग 40 करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष देने की घोषणा की । फ्रांस ने 0.7 प्रतिशत कुल राष्ट्रीय आय का भाग दे देने का वायदा किया ।
स्पेन ने दक्षिण अमरीका के देशों की सहायता को तिगुनी कर देने का वायदा कर यह राशि एक अरब डॉलर तक बढ़ाना स्वीकार किया । हॉलैण्ड ने 25 करोड़ डॉलर तक की सहायता देने का वायदा किया । पृथ्वी सम्मेलन से यह बात स्पष्ट हो गयी कि गरीब (दक्षिण के) देशों में अपने भविष्य के प्रति चेतना उत्पन्न हुई और इस सम्मेलन में वह मुखर भी हुई । सर्वाधिक विवादास्पद मुद्दा यह था कि पर्यावरण को शुद्ध करने का आर्थिक भार कौन उठाए ।
एक विचार आया कि जिन देशों की जीवन शैली पर्यावरण को दूषित करने के लिए जिम्मेदार हैं वे अपने व्यवहार में संयम बरतें । उदाहरण के लिए, अमरीका पर यह आरोप था कि वह सर्वाधिक कार्बन उगलता है, अत: उसे अपना कदम पीछे ले जाना चाहिए ।
इसी तरह एक मुद्दा यह उठाया गया कि जंगलों को सार्वभौम सम्पदा न मानकर स्थानीय सम्पदा माना जाए । इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उग्र रूप में भारत के मन्त्री कमलनाथ ने उठाया । उनका कहना था कि यदि जंगलों को सार्वभौम सम्पदा माना जाए तो क्रूड आयल को भी सार्वभौम सम्पदा माना जाए क्योंकि इसका उपयोग सम्पूर्ण मानव जाति के लिए होता है ।
तीसरा मुद्दा यह था कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अनुमानित व्यय लगभग सवा लाख करोड़ डॉलर कौन उठाये । अमीर देशों के नेता पर्यावरण शुद्ध करने के मुद्दे पर तो सहमत थे परन्तु खर्च उठाने के नाम पर कृपणता दिखा रहे थे । सर्वाधिक कठोर रवैया अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपनाया ।
“सम्मेलन का कुल मिलाकर यह प्रभाव रहा कि गरीब देश पर्यावरण को दूषित करने के परिणामों से सजग हो उठे । उनकी चिन्ता अब यह है कि पर्यावरण के नाम पर भावी विकास के कामों पर अमीर देशों का दबदबा न बढ़ जाए ।”
वस्तुत: पृथ्वी शिखर सम्मेलन का मुख्य झगड़ा उत्तर-दक्षिण विभाजन का है और इसकी पृष्ठभूमि में अमीर देशों से गरीब देशों को धन व पर्यावरण प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण को लेकर दूरी बनी हुई है । 1992 में रिओ-डी-जेनेरी में सम्पन्न हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु एक 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन 23-27 जून, 1997 को झूयार्क में सम्पन्न हुआ ।
सम्मेलन में 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । विश्व में निरन्तर कम हो रहे वनों, नष्ट हो रही प्रजातियों तथा घटते हुए मत्स्य स्टॉक के प्रति अधिकांश देशों ने सम्मेलन में चिन्ता व्यक्त की । विकासशील राष्ट्रों ने इस बात पर बल दिया कि पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विकसित राष्ट्रों से वांछनीय वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है ।
अमरीकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने विकासशील राष्ट्रों को पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए एक अरब डॉलर की सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की, किन्तु यूरोपीय संघ के भारी दबाव के बावजूद मौसम में परिवर्तन लाने वाली गैसों को नियन्त्रित करने के किसी मात्रात्मक लक्ष्य को स्वीकार करने से उन्होंने स्पष्ट इंकार किया ।
यह सम्मेलन बिना किसी ठोस निष्कर्ष के समाप्त हो गया । पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के वित्तीयन एवं इसकी रियायती शर्तों पर हस्तान्तरण, विषैली गैसों के उत्सर्जन तथा वन संरक्षण आदि मुद्दों पर व्यापक बहस के बावजूद सम्मेलन में किसी समझौते पर सहमति न हो सकी ।
6. जी-8 की एवियान (फ्रांस) में सम्पन्न वार्षिक बैठक: जून 2003:
विकसित देशों के समूह जी-8 की जून, 2003 में सम्पन्न वार्षिक बैठक का महत्व इस बार हमेशा से ज्यादा रहा । बैठक के मेजबान फ्रांस ने भारत सहित एक दर्जन प्रमुख विकासशील देशों को आमन्त्रित कर एक नई पहल की । इस नई पहल से विश्व की आर्थिक समस्याओं पर बातचीत का अवसर मिला । इसकी निश्चय ही बहुत जरूरत थी ।
जी-8 की वार्षिक बैठक में सामान्यतया आर्थिक मुद्दे ही प्रधान रहते हैं । इस बार माहौल कुछ बदला हुआ था, क्योंकि इराक युद्ध के सवाल पर समूह के आठों देश दो धड़ों में बंट गए थे । अमरीका, ब्रिटेन, इटली और जापान युद्ध के पक्ष में थे तो रूस, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा उसके खिलाफ थे ।
ऐसे विभाजन की पृष्ठभूमि में हुई बैठक में विकासशील देशों को शामिल करने की पहल सुविचारित थी । विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक बातचीत का कोई मंच है ही नहीं । संयुक्त राष्ट्र में सत्तर के दशक में कुछ पहल हुई थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई ।
विश्व व्यापार संगठन उत्तर-दक्षिण बातचीत का मंच नहीं बन सकता । यह भूमिका जी-8 बैठक के पूर्व हुए विचार-विमर्श से सम्भव हो पाई । वाजपेयी ने कहा भी, ‘इस बार एक मंच पर आने से लगता है कि विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन खड़ा हो गया है ।’ आज की दुनिया में साथ चलने में ही सबका भला है ।
विश्व व्यापार संगठन में कई मुद्दे अटके हुए हैं । संगठन की दोहा में हुई वार्ता के नतीजों की निगरानी और मूल्यांकन के मापदण्ड तय होने चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं विश्व व्यापार संगठन के प्रयासों से सुलझ गईं नहीं मानी जा सकतीं ।
विकासशील देशों के निर्यात की असमान शर्तों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है । वाजपेयी ने शुल्क और गैर-शुल्क अवरोधों को हटाने की बात कही । विकासशील देशों के निर्यात को संरक्षणवाद को बढ़ावा देने वाले शुल्कों का सामना करना पड़ता है ।
गैर-शुल्क अवरोधों में कृषि क्षेत्र को राज-सहायता सर्वप्रमुख है । विकसित देशों में किसानों को दी जाने वाली राज-सहायता विकासशील देशों के किसानों के समक्ष आजीविका का संकट पैदा करती है । पूंजी के मुक्त प्रवाह की बात कही जाती है लेकिन सेवाओं के प्रवाह में अवरोध क्यों लगाया जाना चाहिए ? इसके साथ ही सेवा क्षेत्र के लोगों की निर्बाध आवाजाही का सवाल भी जुड़ा है ।
उत्तर-दक्षिण विभाजन तीव्रतर हो रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इस पर अंकुश लगा पाने में विफल रहे हैं । इस सन्दर्भ में जी-8 में विकसित-विकासशील वार्ता की पहल सराहनीय है । समूह आठ देशों के सेंटपिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन (16-17 जुलाई, 2006) में समूह आठ के सदस्य देशों के अतिरिक्त भारत, चीन, ब्राजील, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था ।
सम्मेलन ने पहले सत्र में विकासशील देशों की 204 अरब जनता तक ईंधन और 16 अरब जनता तक बिजली पहुंचाने पर सहमति दी । भारत के साथ परमाणु क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने का भी निर्णय लिया । विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों को पाने के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच सहमति बनाने और निर्णायक सहमति तक पहुंचने की भी इच्छा व्यक्त की गयी ।
फ्रांस के डीयूविले में 26-27 मई, 2011 को जी-8 के 37वें शिखर सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील देशों ने लीबिया में जारी संघर्ष, जापान में फुकुशिमा नाभिकीय दुर्घटना, यूरोपीय ऋण संकट, अफगान संकट, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा की ।
7. जी-20 (G-20):
जी-20 समूह का गठन सितम्बर, 1999 में किया गया । यह संगठन विश्व की कुछ सबसे चुनिंदा अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है जो हर आधार पर विश्व वित्तीय एवं मुद्रा व्यवस्था तथा व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । इस संगठन में जी-8 के आठ देशों-अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, कनाडा, जर्मनी तथा रूस के अतिरिक्त अन्य-देश शामिल हैं ।
ये देश हैं- भारत, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, चीन, इण्डोनेशिया, मैक्सिको, अर्जेन्टीना, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, सऊदी अरब तथा यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रहे देश को शामिल किया गया है । इस अनौपचारिक संगठन का गठन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान 1999 में किया गया था । संगठन का प्रथम अध्यक्ष कनाडा के पॉल मार्टिन को बनाया गया ।
संगठन का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को अधिक सुगम बनाना, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं में सरचनात्मक सुधार लाना, विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का कुशल प्रबन्धन करना आदि शामिल हैं ।
संगठन के दिसम्बर 1999 के सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि बीमार अर्थव्यवस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार ऋण दिए जाने के स्थान पर उन्हें आपातकालीन आवश्यकताओं हेतु ऋण उपलब्ध कराए जाएं ।
जी-20 राष्ट्रों का प्रथम विदेश मन्त्रीय सम्मेलन बर्लिन में (दिसम्बर 1999), दूसरा सम्मेलन मॉण्ट्रियल में (2000), तीसरा सम्मेलन ओटावा में (नवम्बर 2001), चौथा सम्मेलन नई दिल्ली में (नवम्बर 2002), तथा पांचवां सम्मेलन मैक्सिको सिटी (2003) में आयोजित हुआ ।
27-28 जून, 2010 को कनाडा की राजधानी टोरंटो में तथा 10वां सम्मेलन 15-16 नवम्बर, 2015 को अंताल्या (तुर्की) में जी-20 का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ । वैश्विक आर्थिक मंदी से उबरने की प्रक्रिया में निरन्तरता बनाये रखने, रोजगार के अवसर पैदा करने तथा अधिक मजबूत टिकाऊ और संतुलित वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए ठोस उपाय करने, राजकोषीय घाटा कम करने तथा जीडीपी बढ़ाने पर सम्मेलन में जोर दिया गया ।
सदस्य देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश वर्ष 2013 तक वित्तीय घाटे को आधा कर लेंगे तथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और सरकारी ऋण का अनुपात वर्ष 2016 तक कम कर लेंगे या कम-से-कम स्थिर अवश्य कर लेंगे ।
वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए किये गये उपायों की समीक्षा व वित्तीय बाजारों की मौजूदा स्थिति पर विचार के लिए जी-20 का छठा शिखर सम्मेलन 3-4 नवम्बर, 2011 को फ्रांस के कान में सम्पन्न हुआ ।
यूरो जोन के संकट को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए गम्भीर खतरा बताते हुए भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस संकट से निपटने की मुख्य जिम्मेदारी यूरोपीय देशों की ही बतायी । जी-20 के देशों ने अवैध धन जमा करने की सुरक्षित पनाहगाहों से टेक्स सम्बन्धी सूचनाएं साझा करने तथा बैंकिंग पारदर्शिता के लिए नियम बनाने को कहा ताकि मनी लाउड्रिंग व आतंकवाद के वित्त पोषण पर लगाम लग सके ।
अंताल्या (तुर्की) में 15-16 नवम्बर, 2015 को आयोजित सम्मेलन में भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोटा प्रणाली पर सवाल उठाये । जी-20 के सम्मेलनों में विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारी भी भाग लेते हैं । ये सम्मेलन मुख्यत: विश्व में अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत सुधार करने मौद्रिक संकटों से निबटने तथा व्यापार विस्तार से सम्बन्धित मुद्दों पर पारस्परिक सहमति हेतु आयोजित किए जाते हैं ।
8. जलवायु परिवर्तन पर कोपनहेगन एवं डरबन सम्मेलन:
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन ‘काँप-15’ डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में 7-18 दिसम्बर, 2009 को सपन्न हुआ । 192 देशों के प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर प्रदूषणकारी गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश के लिए एक सर्वसम्मत समझौते पर पहुंचने का प्रयास 12 दिन चले इस सम्मेलन में किया, किन्तु सर्वसम्मत समझौते पर नहीं पहुंचा जा सका ।
क्योटो समझौते में विकसित देशों के लिए उत्सर्जन कटौती की बाध्यता निर्धारित की गई थी, जबकि विकासशील देशों के लिए कोई बाध्यता नहीं थी । विकासशील देशों के लिए ऐसी किसी बाध्यता का कोपनहेगन में भी भारत ने पुरजोर विरोध किया । सम्मेलन के अंतिम दिन (18 दिसम्बर) एक गैर-बाध्यकारी कोपनहेगन समझौते को स्वीकार किया गया ।
अमरीका व बेसिक (BASIC-Brazil, South Africa, India, China) देशों के बीच अंतिम क्षणों की बातचीत के बाद स्वीकारे गये इस समझौते को सर्वसम्मत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनेक राष्ट्रों ने बाद में इसका पुरजोर विरोध किया है ।
भारत के सेंटर फॉर साइंस के निदेशक सुनीता नारायण ने इस समझौते को अमरीकी दबाव में विकासशील देशों के साथ बहुत बड़ा धोखा तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए आत्मघाती करार दिया है । संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन अभिसमय की रूपरेखा (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों के 17वें सम्मेलन तथा क्योटो प्रोटोकाल के पक्षकारों की 7वीं बैठक 28 नवम्बर-9 दिसम्बर, 2011 तक डरबन में आयोजित की गई ।
डरबन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए । विशेषकर, विकसित देश के लिए क्योटो प्रोटोकाल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि पर सहमति व्यक्त की गई । इसके अतिरिक्त, इस सम्मेलन में 2010 में कानकुन में सहमत संरचनाओं के प्रचालन से सम्बन्धित निर्णयों को अपनाया गया । इसमें विकासशील देशों तथा साथ ही अनुकूलन समिति और प्रौद्योगिकी तन्त्र के प्रयासों के वित्तपोषण हेतु हरित जलवायु निधि शामिल है ।
डरबन में अभिसमय के अन्तर्गत संवर्धित कार्यवाइयों के लिए भावी व्यवस्थाओं पर बातचीत करने की नई प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी सहमति बनाई गई । इस प्रक्रिया पर कार्य, जिसे सम्बन्धित कार्यवाही के लिए डरबन मंच कहा गया-2012 के प्रथम हिस्से में प्रारम्भ किया जाना था और इसे 2015 में पूरा किया जाएगा और इसका उद्देश्य एक प्रोटोकाल, दूसरी विधिक व्यवस्था विकसित करना अथवा अभिसमय के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही का सहमत परिणाम है, जो सभी पक्षकारों पर लागू है । नई व्यवस्था वर्ष 2020 से प्रवृत्त होगी ।
पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन:
30 नवम्बर से 12 दिसम्बर, 2015 तक पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सम्पन्न हुआ । सम्मेलन के अन्तर्गत 21वीं कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP 21) में जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक समझौते को 196 देशों ने 12 दिसम्बर, 2015 को अपनी स्वीकृति दे दी ।
इस समझौते के अन्तर्गत धरती के बढ़ते तापमान को दो डिग्री सेल्सियस नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है । इस दिशा में विकसित देश 2020 से 2025 तक विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देंगे ।
उत्तर-दक्षिण संवाद : आलोचनात्मक मूल्यांकन:
उत्तर-दक्षिण संवाद के ऐसे परिणाम नहीं निकले जिसमें ‘नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था’ की स्थापना हो और विकासशील देशों के विकास की रफ्तार तीव्र हो । धनी और निर्धन (उत्तर-दक्षिण) देशों के बीच वार्ता या सौहार्दपूर्ण समझौते के रास्ते में अनेक अड़चनें हैं ।
प्रथम:
धनी देशों के नेता इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहते कि परस्पर-निर्भरता की वर्तमान व्यवस्था में वे भी विकासशील देशों की सहायता (तेल एवं अन्य कच्चे माल के लिए) पर निर्भर हैं और वे सदियों से विकासशील देशों का शोषण करके ही सम्पन्न बन सके हैं ।
द्वितीय:
ADVERTISEMENTS:
धनी देशों के नेताओं के मन में आज भी यह भावना मौजूद है कि वे चालबाजी से आपसी रियायतें, सहायता और व्यापार नीति के सहारे विकासशील देशों का शोषण करते रह सकते हैं ।
तृतीय:
विकासशील देश (दक्षिण के देश) एकजुट नहीं हैं, उनमें टकराव और प्रतिद्वन्द्विता पायी जाती है जिससे आर्थर डुंकेल जैसे पश्चिमी समर्थक ‘गैट’ के महानिदेशक अपनी शर्तें थोपने में सफल हो जाते हैं ।
सिएटल हो या दावोस या फिर दोहा-समस्या है, आर्थिक मुद्दों पर उत्तर और दक्षिण के बीच टकराव की । जबरदस्त आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर लेने के बावजूद ‘उत्तर’ में एक असुरक्षा है – समृद्धि के कम हो जाने या खो जाने की ।
इसी वजह से वह दक्षिण के विकास को अपनी गिरफ्त में रखना चाहता है, या उसे अवरुद्ध करना चाहता है, ताकि दक्षिण के बाजारों में वे अपना माल खपा सकें और अपनी समृद्धि व विकास को न केवल बरकरार रख सकें बल्कि और अधिक बढ़ा सकें ।