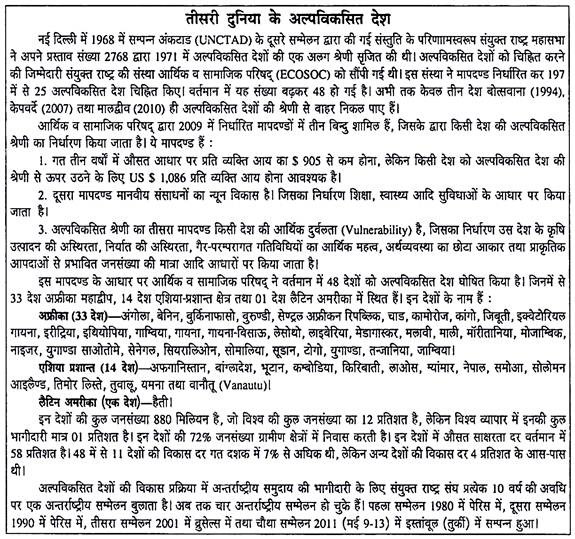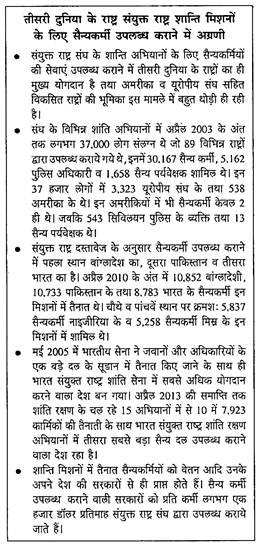ADVERTISEMENTS:
Read this article in Hindi to learn about the emergence of super powers and the third world countries.
थर्ड वर्ल्ड (Third World) या ‘तीसरी दुनिया’ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली का एक बहुप्रचलित मुहावरा है । इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक एक्फ्रेड सोवी ने एक लेख में सन् 1952 में किया था । सोवी के अनुसार ‘तीसरी दुनिया’ उन अज्ञात और शोषित देशों का समूह है जिन्हें प्राय: तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है और जो कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं ।
प्रत्यक्षत: सोवी का संकेत उन अफ्रीकी-एशियाई देशों की तरफ था जो सदियों तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जकड़ में थे और जो अब अपनी गरीबी और पिछड़ेपन से उबरकर आधुनिकता एवं सम्पन्नता की ओर बढ़ना चाहते थे । बहरहाल 1955 में बाण्डुंग में हुए अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन के बाद इस विशेषण का प्रयोग यदाकदा होने लगा, खासकर चीन और चीन से प्रभावित कुछ अफ्रीकी-एशियाई देशों में ।
‘तीसरी दुनिया’ शब्दांश से आज जो अर्थ निकाला जाता है वह 1950 के अर्थ से एकदम भिन्न है । जब शीत-युद्ध अपनी चरम सीमा पर था ‘तीसरे विश्व’ का अर्थ उन तटस्थ या असंलग्न राष्ट्रों के झुण्ड से लिया जाता था जो न तो पश्चिमी शक्तियों (पहली दुनिया) से प्रतिबद्ध थे और न साम्यवादी गुट (दूसरी दुनिया) से प्रतिबद्ध थे ।
आज तथाकथित इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में कोई वैचारिक एकजुटता नहीं है जिससे किसी सामूहिक अवधारणा से उन्हें सम्बोधित किया जा सके । आज तो ये देश ‘गरीबी’ और ‘पिछड़ेपन’ के पर्यायवाची प्रतीत होते हैं । अत : आज ‘तीसरी दुनिया’ शब्द का प्रयोग ‘विकासशील राष्ट्रों’ (Developing nations) या ‘अल्प-विकसित राष्ट्रों’ (Developed countries) के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।
कतिपय विद्वानों का मत है कि सोवियत संघ के विघटन एवं साम्यवाद के पतन के पश्चात् ‘थर्ड वर्ल्ड’ का मुहावरा अपनी सार्थकता खो चुका है । कुछ सीमा तक यह विचार ठीक है तथापि बदले परिप्रेक्ष्य में भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण तीसरी दुनिया के देशों के प्रसंग में करना एकदम साररहित भी प्रतीत नहीं होता । यहां ‘तीसरी दुनिया’ से हमारा स्पष्ट अभिप्राय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ‘विकासशील देशों’ की भूमिका का विश्लेषण करना है ।
तीसरे विश्व की अवधारणा:
20वीं शताब्दी के छठे दशक के आखिरी वर्षों में चीनी नेता माओत्सेतुंग और उनके अनुयायियों ने अपनी ‘तीन दुनियाओं’ की कल्पना प्रचारित की । इस कल्पना के अनुसार ‘पहली दुनिया’ में केवल दो महाशक्तियां अमरीका और सोवियत संघ हैं ।
‘दूसरी दुनिया’ उन देशों से मिलकर बनी है, जिनका इन महाशक्तियों के साथ सैनिक अथवा व्यापक गठबन्धन है और ‘तीसरी दुनिया’ उन देशों का समूह है, जो कच्चा माल पैदा करते हैं, जो बड़े देशों के उपनिवेश थे तथा जो आधुनिक औद्योगीकरण से बहुत दूर हैं । इस परिभाषा के अनुसार सामान्यत: एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका क्षेत्र के वे नवोदित देश ही ‘तीसरी दुनिया’ की परिधि में आते हैं जो सदियों तक उपनिवेशवादी शोषण के शिकार रहे थे ।
ADVERTISEMENTS:
तीसरे विश्व की अवधारणा को दो रूपों में देखा गया है: एक तो इन सभी राष्ट्रों की समस्याएं एक जैसी हैं (The ‘Package’ of problems that the whole Third World seems to face) तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कतिपय मुद्दों पर मतदान करते समय इन राष्ट्रों में एकजुटता देखी गयी है (The seeming unity of the Third World bloc within the United Nations General Assembly during votes on Certain issues) खासतौर से उपनिवेशवाद विरोधी मुद्दों के बारे में ।
अल्जीरियाई लेखक फैन्ट्रज फैनन ने 1961 में प्रकाशित अपनी कृति ‘Les. Damnes. Delaterre’ में भी ‘तीसरी दुनिया’ शब्द का प्रयोग किया है जिसका अंग्रेजी अनुवाद सन् 1965 में “The Wretched of the World” शीर्षक से प्रकाशित हुआ ।
यह वह समय था जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका में नये-नये राष्ट्रों का उदय हो रहा था । ऐसे राष्ट्र जो वर्षो से उपनिवेशवादी शोषण और विसंगतियों के शिकार थे अपनी स्वतन्त्रता की मांग और शोषण के विरोध के नारे पर संघर्ष कर रहे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के इन राष्ट्रों को सम्बोधित करने के लिए फेनॉन ने ‘तीसरी दुनिया’ शब्द का प्रयोग किया । फेनॉन ने पूंजीवादी जगत को ‘पहली दुनिया’ और ‘साम्यवादी जगत’ को ‘दूसरी दुनिया’ का नाम दिया ।
‘तीसरी दुनिया’ को प्राय: ‘विकास’ के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है । इरविंग होरोविज ने इसी परिप्रेक्ष्य में एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था विकास की तीन दुनियाएं’ (Three Worlds of Developments) । वे विकास की पहली दुनिया में पश्चिमी यूरोप तथा अमरीका को लेते हैं ।
ADVERTISEMENTS:
इस दुनिया की प्रमुख विशेषता है प्रतियोगी पूंजीवाद, जिसने 16वीं शताब्दी से सामन्तवाद को क्षीण करना प्रारम्भ कर दिया था । 16वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति ने ऐसे प्रगतिशील विश्व के अभ्युदय में सहायता दी जिसने सर्वत्र आधुनिकीकरण की छाप छोड़ दी ।
प्रोफेसर होरोविज दूसरी दुनिया के अन्तर्गत सोवियत संघ और उसके गुटीय राष्ट्रों को लेते हैं । जारों के शासनकाल में रूस की हालत आज के विकासशील राष्ट्रों के समतुल्य थी । 1917 की बोल्शेविक क्रान्ति ने रूस को पूंजीवादी विकास मार्ग से विलग कर दिया और उसे नियोजित केन्द्रीभूत विकास के ढांचे में ढाल दिया ।
द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों ने सोवियत संघ के राजनीतिक-आर्थिक मॉडल को अपना लिया तथा चीन ने भी थोड़े-बहुत परिवर्तित रूप में इसी मॉडल को वरीयता दी । ‘तीसरी दुनिया’ एक नूतन तथ्य है । ये वे राष्ट्र हैं जो सदियों की उपनिवेशवादी गुलामी से मुक्त हुए हैं और विकास के किसी मार्ग की खोज में हैं ।
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के कई राष्ट्रों की विकास की समस्याएं लगभग एकसमान हैं, अत: उनमें समस्याओं और ध्येयों की एकजुटता की प्रवृत्ति पायी जाती है । उनका मुख्य ध्येय विकास है, अपने विकास हेतु वे पहली और दूसरी दुनिया के देशों से विचारधारा राजनीति और अर्थनीति उधार लेने में नहीं हिचकिचाते किन्तु पूरब एवं पश्चिम के शीत-युद्ध में असंलग्न रहना चाहते हैं ।
सर्वाधिक स्वीकृत धारणा के अनुसार- ‘तीसरी दुनिया’ में वे देश आते हैं, जो न तो आर्थिक दृष्टि से विकसित पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में शामिल हैं और न पूर्णत: नियोजनबद्ध समाजवादी देशों की श्रेणी में आते हैं ।’ थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली’ (लन्दन) ने इसी कल्पना को पेश किया है – ”लगभग 135 अफ्रीकी-एशियाई और दक्षिणी अमरीकी देश अपने को सामूहिक रूप से ‘तीसरी दुनिया’ कहते हैं । वे अपने को विकसित पूंजीवादी और केन्द्रीय नियोजित समाजवादी देशों से अलग रखकर अपनी पहचान स्थापित करते हैं ।”
‘तीसरे विश्व’ की अवधारणा एक मानसिक अवधारणा है न कि कोई ठोस राजनीतिक इकाई । वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके बाहर सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अनेक बैठकें आयोजित की गयीं किन्तु अभी तक ‘तीसरे विश्व’ की कोई राजनीतिक इकाई अस्तित्व में नहीं आयी है ।
इन देशों में राजनीतिक विविधता और वैदेशिक नीति में इतनी अधिक भिन्नता है कि मात्र ‘तीसरे विश्व’ से सम्बन्धित मुद्दों जैसे- उपनिवेशवाद विरोध और विकास के अतिरिक्त किसी भी पहलू पर आम सहमति का अभाव पाया जाता है । यहां तक कि विकास के क्षेत्र में भी तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में अत्यधिक विविधता पायी जाती है ।
जैसा कि लेस्टर आर. ब्राउन ने लिखा है- “द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के निर्धन या अल्प-विकसित राष्ट्रों को सम्मिलित रूप से ‘तीसरी दुनिया’ कहा गया है । किन्तु आज यह शब्दांश अपना महत्व खोता जा रहा है । एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के देश आज निर्धनता के घर नहीं रह गए हैं । इनमें बहुत-से राष्ट्रों ने आर्थिक और सामाजिक मोर्चो पर सफलता प्राप्त की है ।”
तथाकथित तीसरी दुनिया के कुछ देशों में पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुआ है, चाहे इसका कारण तेल निर्यात ही क्यों न रहा हो ? इससे विकास की दौड में अधिसंख्य देश पिछड़ गए हैं, और अब उन्हें ‘चौथी दुनिया’ (Fourth World) भी कहा जाने लगा है ।
चौथी दुनिया के ये देश आर्थिक और राजनीतिक संकट के भयावह दौर से गुजर रहे हैं । जनसंख्या विस्फोट, भुखमरी, आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार, आर्थिक स्रोतों के अभाव में चौथी दुनिया के देशों के लिए तीसरी दुनिया के देशों का स्तर भी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल लगता है ।
कतिपय विश्लेषकों का मत है कि यदि ऊर्जा संकट तथा खाद्य संकट की वर्तमान प्रवृत्ति बनी रही तो चौथी दुनिया के राष्ट्रों के लिए अस्तित्व का ही संकट उत्पन्न हो जाएगा । सातवें दशक के प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजों में विश्व को तीन भागों में बांटा गया-विकसित निजी अर्थव्यवस्थाएं केन्द्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्थाएं और प्राथमिक माल उत्पादक विकासशील अर्थव्यवस्थाएं ।
तीसरी दुनिया को कच्चा माल उत्पादित करने वाली ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है जिनमें निम्न औद्योगीकरण हुआ है, विकास दर कम है और प्रथम और द्वितीय विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर आश्रित है । इस प्रकार तीसरी दुनिया को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया ।
डॉ. शिशिर गुप्ता के अनुसार, तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं हैं: निर्धनता, अस्थिरता, नयापन, अश्वेत तथा दुर्बलता । आज विकसित देश धन और खुशहाली के टापू बनते जा रहे हैं लेकिन विकासशील देश गरीबी और दुःखों की डगर पर ही खड़े हैं ।
यदि हम नवम्बर, 2001 के पहले सप्ताह में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ताजा रिपोर्ट को देखें तो पाते हैं कि विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या कुपोषण, प्रदूषण एवं सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का कारण बनती जा रही है ।
विश्व में धनवान और गरीब के बीच की दूरी घटने का नाम नहीं ले रही है । धनवान लोग जरूरत से ज्यादा अत्यावश्यक संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं । दूसरी ओर ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें इतना भी भोजन नहीं मिल रहा है कि वे जीवित रह सकें ।
विश्व की जनसंख्या पर किए गए संयुक्त राष्ट्र के दो अन्य अध्ययनों ‘पद चिह्न और मील के पत्थर’ तथा ‘जनसंख्या और पर्यावरण परिवर्तन’ हैं जिन्हें हाल ही में जारी किया गया है । इन रिपोर्टों के अनुसार विश्व में 80 करोड़ लोगों को आज भी भरपेट भोजन नसीब नहीं होता । यह जनसंख्या हिन्दुस्तान की आबादी से थोड़ी ही कम है । यह विश्व गरीबों और अमीरों के बीच बटी है ।
यह तो पहले भी पता ही था, लेकिन इन रिपोर्टो के कुछ आंकड़े बेहद आक्रामक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं । सर्वेक्षण बताते हैं कि पृथ्वी पर 7 अरब से अधिक मनुष्य रहते हैं लेकिन इनमें से केवल 20 प्रतिशत मनुष्य ही पृथ्वी के 86 प्रतिशत संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं । ये लोग यूरोप जापान उत्तरी अमरीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसते हैं । शेष विश्व की अति निर्धन 20 प्रतिशत जनसंख्या सिर्फ दशमलव दो प्रतिशत संसाधनों पर आश्रित है ।
जहां विकसित देश वर्ष प्रति वर्ष समृद्ध हो रहे हैं, वहीं विकासशील देशों पर विदेशी ऋण बढ़ता जा रहा है । ऋणग्रस्त विकासशील देश आर्थिक-सामाजिक संकटों से त्रस्त हैं । भारत का विदेशी ऋण मार्च 2014 तक बढ़कर 440.6 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया । लेकिन विश्व बैंक ने वर्तमान मूल्य पर आधारित ऋणग्रस्त विकासशील देशों की सूची में उसे अल्प रूप से ऋणग्रस्त देश बताया है ।
पाकिस्तान अब भी गम्भीर रूप से ऋणग्रस्त देशों की सूची में है । विश्व बैंक की सूची में विकासशील देशों को तीन श्रेणियों गम्भीर, साधारण व अल्प रूप से ऋणग्रस्त रखा गया है । विश्व बैंक ने पाकिस्तान के अलावा ब्राजील, अर्जेटाइना और इंडोनेशिया को गम्भीर रूप से ऋणग्रस्त देशों की सूची में रखा है । साधारण रूप से ऋणग्रस्त देशों में रूस परिसंघ, तुर्की, थाईलैण्ड, मलेशिया, फिलीपीन्स, वेनेजुएला और चिली को रखा गया है जबकि मैक्सिको, कोरिया, चीन, पोलैण्ड और भारत को अल्प ऋणग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है ।
पिछले वर्ष विश्व बैंक ने भारत को साधारण ऋणग्रस्त विकासशील देशों की सूची में रखा था । विश्व बैंक ने तीन श्रेणियों की जो कसौटी बनाई है, उसके ‘अनुसार जिन देशों का कुल ऋण निर्यात पर ऋण शोधन के वर्तमान मूल्य के 220 प्रतिशत और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में 80 प्रतिशत से अधिक है उन्हें गम्भीर रूप से ऋणग्रस्त की माना जाएगा ।
इसी तरह जिस देश का कुल ऋण, निर्यात ऋणों, शोधन के वर्तमान मूल्य के परिप्रेक्ष्य में 132 प्रतिशत और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में 48 प्रतिशत तक है उसे साधारण रूप से ऋणग्रस्त माना गया है । तीसरी श्रेणी में उन देशों को रखा गया है जिनका अनुपात इससे कम है ।
तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं (The Characteristics of the Third World Countries):
आज जिस विश्व में हम रह रहे हैं उस विश्व के 4.4 अरब लोग विकासशील देशों में रह रहे हैं । इस संख्या के एक-चौथाई को जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे शौचादि की भी सुविधा नहीं है, लगभग एक-तिहाई के लिए साफ पीने का पानी नहीं है एक-चौथाई के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, पांचवें हिस्से के पास चिकित्सीय सुविधाएं नहीं हैं, पांचवें हिस्से के बच्चे पांचवीं कक्षा से अधिक पढ़ नहीं सकते और इतने ही बच्चे भूखे-नंगे हैं । आज तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषता है-विकास के लिए संघर्ष ।
किन्तु इस आम विशेषता के अतिरिक्त उनमें अधोलिखित सामान्य विशेषताएं भी दिखायी देती हैं:
1. जीविकोपार्जित कृषि एवं बागवानी प्रधान अर्थव्यवस्था:
तकनीकी ज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान के अभाव में तीसरी दुनिया के ये अल्प-विकसित देश अधिकांशत: कृषि पर निर्भर हैं । यहां कृषि व्यवसाय नहीं बल्कि जीविकोपार्जन या बागवानी पर आधारित है । बढ़ती जनसंख्या का दबाव या कच्चे माल के निर्यात में ही सभी कृषक लगे हैं । विश्व जनसंख्या में 1.3 बिलियन कृषि पर निर्भर है जिसमें 1 बिलियन इन्हीं देशों में है । व्यावसायिक संरचना में असन्तुलन होने के कारण तथा कृषि पर निर्भरता अधिक होने से राष्ट्रीय आय में कमी होती है ।
2. निर्यातों पर आश्रित:
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक निर्यात नुकसानदायक नहीं होते परन्तु यदि कच्चे माल का अधिकांश भाग विदेशों को जाता है और उसके बदले में उन्हें कम लाभ प्राप्त होता है तो आर्थिक विकास नहीं बढ़ता । तीसरी दुनिया के देश अपने निर्यातों पर अधिक निर्भर रहते हैं । इन्हीं अल्प-विकसित देशों में निर्यात का राष्ट्रीय आय से अनुपात 20% है ।
यह समस्या तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब निर्यातक देश एक या दो ही वस्तुओं का निर्यात करते हैं । मिस्र, इण्डोनेशिया, मलाया, श्रीलंका, अफ्रीकन क्षेत्र, लैटिन, अमरीका, आदि सभी तीसरी दुनिया के देश एक या दो वस्तुओं के निर्यात से ही अधिकांश विदेशी मुद्रा अर्जित करते है ।
निर्यातों पर अधिक आश्रित होने के कारण तथा विदेशी बाजारों की स्थितियों में निर्यात नियम, आदि से विभिन्न वस्तुओं की मांग में जब कभी उच्चावचन होते रहते हैं जिसका प्रभाव इन देशों की अर्थव्यवस्था में होता है । प्राथमिक वस्तुओं की विदेशों में मांग कम हो जाने के कारण इन देशों में राष्ट्रीय आय तथा रोजगार पर प्रभाव पड़ता है । साथ ही सरकारी आय में भी अपेक्षाकृत परिवर्तन होते रहते हैं ।
3. असन्तुलित घटक:
उत्पादन में पूर्ण घटकों की गतिशीलता के कारण एक उद्योग से दूसरे उद्योग में सीमान्त प्रतिफल समान रहता है । गतिशील अर्थव्यवस्था में साधनों का अधिकतम उपभोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मिल जाता है, परन्तु अल्प-विकसित देशों में उत्पादन के विभिन्न घटकों में अचलता देखी जाती है ।
उदाहरण के लिए- श्रमिक एक उद्योग से दूसरे उद्योग में नहीं जाना चाहते यद्यपि वर्तमान में उनका उत्पादन कुछ नहीं है । जाति-प्रथा, सामाजिक व संस्थागत विचार, पूंजी गतिशीलता तथा विनियोग उद्योग को प्रभावित करते हैं ।
4. जनसंख्या वृद्धि:
विकासशील देशों में जनाधिक्य है तथा जनसंख्या वृद्धि-दर विकसित देशों की अपेक्षा अधिक है । जनसंख्या में कमी से ही वास्तविक आय में वृद्धि हो सकती है । जनसंख्या वृद्धि कई आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न करती है ।
5. अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं:
तीसरे विश्व के देशों में लोकतन्त्र अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है । इन देशों में राजनीतिक प्रक्रियाएं संक्रमण के दौर में होने के कारण संविधानों में लोकतन्त्र के आधार सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं । संविधानों में बार-बार मौलिक संशोधन किए जाते है तथा एक मूल्य के स्थान पर दूसरा मूल्य आरोपित कर दिया जाता है । इन राज्यों का लोकतन्त्र समाजवादी लोकतन्त्र के नाम से पुकारा जाने लगा है ।
इन लोकतन्त्रों में राजनीतिक समाजों के मूल्य तो उदारवादी लोकतन्त्र की अवधारणा के समान स्वतन्त्रता राजनीतिक समानता, सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा लोक- कल्याण की साधना के ही हैं परन्तु साधनों की दृष्टि से समाजवादी लोकतन्त्र साम्यवादी विचारधारा के समीप लगते हैं, क्योंकि इन राज्यों में साम्यवादी संरचनाओं व संस्थागत व्यवस्थाओं के प्रति आस्था बलवती बनती जा रही है ।
6. करिश्माती नेतृत्व:
इन देशों में कार्यपालिका अध्यक्ष करिश्मे व चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले नेता होते हैं । राष्ट्रीय आन्दोलनों के लम्बे कालों में ऐसे देव तुल्य नेता जनमानस में समा गए थे । इस कारण स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद ऐसे नेताओं के कार्यपालिका अध्यक्ष बनने पर उनको आदर व असाधारण प्रतिभा का प्रतीक ही नहीं वरन् राष्ट्र का पिता मान लिया गया था ।
जोमो केन्याता, सुकार्नो, बोर्गिबा, नासिर, नेहरू, ऐनक्रूमा, न्येरेरे, लुबुम्बा, शेख मुजीब, इत्यादि अनेक कार्यपालिका अध्यक्ष ऐसे ही अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण लम्बी अवधि तक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर छाए रहे । इन कार्यपालिका अध्यक्षों की शक्तियां असीमित रही हैं ।
7. विधायिका का ह्रास:
इन देशों में बहुल समाज परस्पर विरोधी व अधिकतर संघर्षशील शक्तियों के तनावों व खिंचावों से त्रस्त रहते हैं । राजनीतिक व्यवस्था में विधानमण्डल ऐसी विषम परिस्थितियों के कारण संयोजनकारी भूमिका निभाने में सर्वथा असफल रहते हैं । अत: कार्यपालिका अध्यक्ष तानाशाह की सी स्थिति में आ जाता है ।
8. एक दल प्रणाली:
इन देशों में प्रतियोगी दल प्रणाली आवश्यक सहिष्णुता के अभाव में अस्त-व्यस्त होते-होते एक दल पद्धति की परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है । एक दल की स्थापना व उसका एकाधिकार कार्यपालिका की प्रवृत्ति में अन्तर ला देता है । इस प्रकार के दल का केवल दिखावा ही रहता है ।
कार्यपालिका अध्यक्ष अपनी सत्ता की वैधता के लिए चुनावों का ढोंग इसी दल के माध्यम से करने लगे; किन्तु सभी तीसरी दुनिया के राज्यों के बारे में यह सामान्यीकरण खरे नहीं उतरते हैं । अनेक राज्यों में स्वतन्त्रताएं व दल प्रतियोगिता की वास्तविक परिस्थितियां बनाए रखने के संस्थागत साधन उपलब्ध रहते हैं । मैक्सिको, भारत व श्रीलंका इसके उदाहरण हैं ।
संक्षेप में, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में कार्यपालिका प्रतिमान अभी भी सुस्थिर नहीं हुए हैं । पुराने नेतृत्व के हटाने पर अनेक राज्यों में कार्यपालिका अध्यक्ष संस्थागत चयन प्रक्रिया की दृढ़ता के अभाव में, सामान्य ढंग से चुनकर नहीं आ पाता है और अधिकतर कार्यपालिका पद तानाशाहों के हाथ में चला जाता है । इस प्रकार तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में कार्यपालिका सामान्यतया नियन्त्रण मुक्त ही रहती है ।
व्यवस्थापिकाएं इन देशों में नाम से ही रह गयी हैं । न्यायपालिका पर महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर कार्यपालिका, शक्ति-केन्द्रण में बेरोकटोक हो जाती है । अत: विकासशील राष्ट्रों में कार्यपालिकाएं अधिकतर विशेष व्यक्तित्व-उन्मुखी बन गयी हैं ।
9. भ्रष्टाचार:
तीसरी दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार की आम शिकायत है । जहां संयुक्त राज्य अमरीका में 90% कर वसूल कर लिए जाते हैं वहां इन देशों में कर वसूली 50% से कम होती है । इन देशों में विकास कार्य सरकारी कोष पर निर्भर करता है और वंचना से प्रभावित होता है । राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी भ्रष्टाचार इन देशों में खूब फैला हुआ है ।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत व पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया क्षेत्र विश्व का भ्रष्टतम एवं निकृष्टतम (Poorly) प्रशासित क्षेत्र है । अकेले पाकिस्तान में प्रतिवर्ष 100 अरब रुपए से अधिक की राशि भ्रष्टाचार में लिप्त होती है जो कि वहां के सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत है ।
भारत के बारे में की गई एक टिप्पणी के अनुसार मुम्बई में एक भवन के निर्माण के लिए विभिन्न विभागों से कम-से-कम 47 किस्म की स्वीकृतियां लेने की आवश्यकता पड़ती है । इसी प्रकार एक लघु उद्यमी को प्रति माह 36 विभिन्न विभागीय इंस्पेक्टरों से निपटना पड़ता है ।
10. विलासितापूर्ण खर्चे:
तीसरी दुनिया के देशों में अभिजन वर्ग अनापशनाप खर्च करता है । जो धन विकास के कार्य में खर्च होना चाहिए उसे राजनीतिक और प्रशासनिक अभिजन अपने भोग-विलास के लिए खर्च कर देता है ।
11. सैन्य-सामग्री पर खर्च:
सेना और सैन्य-सामग्री पर भी तीसरी दुनिया के देश काफी धन अपव्यय करते हैं । 1964-1973 में विकासशील देशों ने 388 बिलियन डॉलर का सैनिक साज-सामान खरीदा । स्टॉकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टीट्यूट की मार्च, 2014 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2009-13 के बीच हथियारों के सबसे बडे आयातक देश क्रमश: भारत, चीन, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश हैं ।
सन्दर्भित अवधि में शस्त्रों के कुल निर्यात में 29% योगदान अमरीका का 27% योगदान रूस का, 7% योगदान जर्मनी का, 6% योगदान चीन का तथा 5% योगदान फ्रांस का रहा है । तीसरी दुनिया को जो धन रोटी पर खर्च करना चाहिए उसे बन्दूक पर खर्च कर दिया जाता है ।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए अध्ययन में विकासशील देशों में व्यापक निर्धनता, बेरोजगारी तथा आंशिक बेरोजगारी, आर्थिक वृद्धि की असन्तोषजनक दर काम की तलाश में गांवों से बड़ी संख्या में लोगों का शहरों की ओर पलायन के कारण विकास की असंगत नीति अपनाना, निरक्षरता, सरकार की उदासीनता, घटती हुई विदेशी सहायता तथा विश्व के विकसित देशों का असहयोगपूर्ण रवैया तथा व्यापार सम्बन्धी बाधाएं खड़ी करना बताया गया है ।
कई विकासशील देशों में बेरोजगारी की संख्या या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण संख्या उन लोगों की है जो काम करते हैं लेकिन उनकी आय इतनी कम है कि वे हमेशा गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं । तीसरे विश्व के विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां विकसित देशों की तुलना में नितान्त भिन्न हैं । इन देशों में बेरोजगारी तथा आशिक बेरोजगारी बहुत अधिक है ।
अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन गुजारते हैं । नौकरी की तलाश में कृषि क्षेत्र से सम्बद्ध लोगों की संख्या बराबर बढ़ती जाती है । सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की प्रधानता होती है जिनमें रोजगार के अवसरों में वृद्धि की सम्भावना बहुत कम होती है ।
इन देशों की जनसंख्या लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ती जाती है । प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम होती है तथा उसमें भी बहुत अधिक असमानता होती है । श्रमिक संघ बहुत छोटे तथा कमजोर होते हैं और वे राजनीतिक क्षेत्र की गतिविधियों से प्रभावित होते हैं ।
एक अध्ययन के अनुसार पिछले बीस वर्षों में तीसरी दुनिया को सम्पन्न देशों ने लगभग 235 अरब रुपए की आर्थिक सहायता दी । पर इसी काल में 3,800 अरब रुपए की फौजी सहायता दी । इस सहायता का नतीजा यह हुआ कि 1946 में रूस द्वारा हंगरी पर हमले को छोड्कर बाकी सभी युद्ध तीसरी दुनिया में हुए हैं । इन युद्धों में 1 करोड़ 63 लाख लोग हताहत हुए । यह संख्या द्वितीय विश्व-युद्ध में मारे गए लोगों की आधी तो होगी ही ।
तीसरे विश्व के देशों में विविधता:
रोजेन तथा जोन्स ने लिखा है कि तीसरे विश्व के देशों में कई क्षेत्रों में विविधता दिखायी पड़ती है जो इस प्रकार है:
1. संसाधनों के क्षेत्र में (Resources):
प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से तीसरी दुनिया के देशों में काफी अधिक भिन्नता पायी जाती है । उदाहरण के लिए, सूडान के पास विकास हेतु संसाधन काफी कम हैं जबकि नाइजीरिया के पास प्राकृतिक साधनों की भरमार है ।
2. जनसंख्या की दृष्टि से (Population):
जनसंख्या की दृष्टि से भी तीसरी दुनिया के देशों में काफी अन्तर पाया जाता है । कुछ राज्यों में जनसंख्या का घनत्व काफी अधिक है, जैसे जावा (इण्डोनेशिया) में संयुक्त राज्य अमरीका की एक-तिहाई जनसंख्या पायी जाती है, जबकि तेल उत्पादक देश लीबिया में जनसंख्या काफी कम है । कुछ देशों में शहरी जनसंख्या काफी है जबकि अन्य देशों में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है । कुछ देश भूमि की दृष्टि से काफी बड़े हैं, जैसे- ब्राजील और भारत जबकि अल साल्वाडोर, लेबनान, आदि छोटे देश हैं ।
3. जातीय दृष्टि से (Ethnic Divisions):
तीसरी दुनिया के देश जातीय समूहों की दृष्टि से भी एक-दूसरे से काफी भिन्न हैं । चिली जैसे कुछ देशों में समरूप समाज (Homogeneous Populations) पाए जाते हैं जबकि अन्य देशों में दो-तीन जातीय समूह (ethnic groups) पाए जाते हैं और उनमें काफी मतभेद (Conflict) पाए जाते हैं । उदाहरण के लिए- नाइजीरिया में आइबोज तथा हाउसास एवं योरीबा में जो संघर्ष चला उसमें गृह-युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गयी । भारत में भाषा, धर्म और जातिगत विविधताएं पायी जाती हैं ।
4. राजनीतिक विरासत (Political Heritage):
तीसरी दुनिया के राज्यों के राजनीतिक इतिहास में भिन्नता पायी जाती है । कुछ देश जो अभी तक भी (जैसे, मोरक्को, केन्या) उपनिवेश थे जबकि कुछ देशों पर कभी विदेशी प्रभुत्व स्थापित नहीं हो सका । (जैसे- थाईलैण्ड) । कुछ देश तो काफी पुराने हैं और उनका राजनीतिक अस्तित्व अमरीका से भी पुराना है (जैसे- ईरान)। कुछ देश तो उपनिवेशवादी शक्तियों की उपज हैं (जैसे- नाइजीरिया) और कुछ देश भूतपूर्व पृथक् राज्यों को मिलाकर अभी-अभी संघ के रूप में आए हैं (जैसे- मलेशिया) ।
5. आधुनिक और पारम्परिक संस्कृति (Modernizing and Traditional Cultures):
तीसरी दुनिया के कुछ देशों में आज भी प्राचीन परम्पराएं विद्यमान हैं, राजनीतिक चेतना का अभाव है और वे पुरातन ग्रामीण, धार्मिक समस्याओं से जूझ रहे हैं । कुछ देशों में परम्परागत अवस्था को आधुनिक अभिजन (Modernized Elite) द्वारा चुनौती दी जा रही है, शासन में जन-सहभागिता में वृद्धि हो रही है और पुरातन समाज व्यवस्था ढह रही है। साक्षरता का प्रतिशत विकासशील देशों में काफी भिन्न है ।
6. शासन सम्बन्धी विभिन्नता (Governments):
तीसरी दुनिया के देशों में कहीं पर पारम्परिक अभिजनीय शासन (Traditional ruling elites), कहीं पर राजतन्त्र (Monarchies), कहीं पर निर्वाचित सरकारें (Elected regimes), कहीं पर पश्चिमी प्रतिमान की सरकारें (Western Democratic Model) तथा कहीं पर सैनिक शासन (Military juntas) पाया जाता है ।
7. आर्थिक व्यवस्था (Economies):
तीसरे विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था में काफी अन्तर पाया जाता है । कुछ देशों की अर्थव्यवस्था (जैसे, चिली) पूर्ण रूप से अपने आयात-निर्यात पर निर्भर करती है । कुछ देशों के लिए विदेशी व्यापार (जैसे- भारत) उतना महत्वपूर्ण नहीं है; कुछ देशों में लोगों की आय में पनारी अन्तर पाया जाता है (जैसे- सऊदी अरेबिया); कुछ देशों में समाज पूर्णतया कृषि पर निर्भर है (जैसे, श्रीलंका); कुछ देशों का समाज मोटे रूप में औद्योगिक है (जैसे- दक्षिण कोरिया); कुछ देशों की अर्थव्यवस्था में गतिरोध आ गया है (जैसे- अफगानिस्तान); कुछ देशों की अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि हो रही है (जैसे- ब्राजील); कुछ देशों की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तत्व मौजूद हैं (जैसे- अर्जेण्टाइना) तो कुछ देशों की अर्थव्यवस्था समाजवादी ढांचे पर आधारित है (जैसे- वियतनाम) ।
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरे विश्व के देशों की भूमिका:
एशियाई मैत्री सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आन्दोलन ग्रुप ऑफ 77, जी-15 आदि मंचों से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरी दुनिया की भूमिका का अध्ययन किया जा सकता है ।
एशियाई मैत्री सम्मेलन:
द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के अधिकांश देशों को स्वाधीनता मिलती गयी और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका में वृद्धि हुई । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उपयुक्त प्रभाव की प्राप्ति के लिए तीसरे विश्व के देश एक ओर तो पाश्चात्य शक्तियों और साम्यवादी गुट के द्वन्द्व में अधिकांशत: गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति अपनाने लगे तथा दूसरी ओर वे गुटनिरपेक्षता, पंचशील उपनिवेशवाद का विरोध जातीय समानता की मांग आदि के आधार पर एक सामान्य नीति के विकास का प्रयत्न करने लगे ।
एक प्रयत्न के परिणामस्वरूप ‘एशियाई-अफ्रीकी ऐक्य’ (Afro-Asian solidarity) कें आन्दोलन का विकास हुआ । मार्च, 1947 में ‘विश्व मामलों की भारतीय परिषद्’ के तत्वावधान में नयी दिल्ली में आयोजित एक गैर-सरकारी ‘एशियाई मैत्री सम्मेलन’ सम्भवत: इस आन्दोलन की प्रथम अभिव्यक्ति थी । इसमें 28 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।
यद्यपि इस सम्मेलन को किसी सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं था लेकिन इसका महत्व इस बात में है कि एशिया के विभिन्न देशों के नेता इसमें शामिल हुए थे । इस सम्मेलन में एशियाई देशों की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, आर्थिक विकास, प्रजातीय विभेद, आदि विविध समस्याओं और एक स्थायी संगठन कायम करने के प्रस्ताव पर विचार हुआ ।
तीसरी दुनिया की एकता तब एक कदम और आगे बढ़ गयी जब जनवरी, 1947 में 15 राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया । इसमें मुख्य रूप से इण्डोनेशिया में डच सरकार द्वारा की गयी सैनिक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर विचार-विमर्श हुआ । एशियाई व्यक्तित्व का विकास होता गया ।
मई, 1950 में फिलिपाइन्स द्वारा बोगुई नामक स्थान पर एशियावासियों के सांस्कृतिक व आर्थिक सहयोग पर विचार करने के लिए सम्मेलन आमन्त्रित किया गया । अप्रैल, 1954 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका म्यांमार (बर्मा) और इण्डोनेशिया के प्रधानमन्त्री हिन्दचीन सहित विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए परस्पर मिले । दिसम्बर में पांचों प्रधानमन्त्री बोगार में एकत्र हुए और वहां एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों का एक वृहद् सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया ।
बाण्डुंग सम्मेलन:
तीसरे विश्व में द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद नव-जागरण की लहर का सर्वोत्तम रूप बाण्डुंग सम्मेलन में प्रकट हुआ । भारत बर्मा (म्यांमार) और इण्डोनेशिया द्वारा इस महान अफ्रो-एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया जो 18 अप्रैल से 27 अप्रैल, 1955 तक चला । इस सम्मेलन में भारत सहित 29 राष्ट्र सम्मिलित हुए ।
इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि- ”यह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि एशिया और अफ्रीका का पुनर्जन्म हो चुका है ।” इस सम्मेलन ने विदेशी सहायता एक राष्ट्र संघ फण्ड, तकनीकी ज्ञान तथा बहुपक्षी व्यापार के आदान-प्रदान एवं भिन्न-भिन्न प्रकार के निर्यात द्वारा विश्व के एशियाई एवं अफ्रीकी क्षेत्र के आर्थिक विकास की आवश्यकता पर जोर दिया ।
इसने एशियाई व अफ्रीकी देशों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व से युक्त ‘अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति संस्था’ की स्थापना की मांग की; प्रजाति भेदभाव तथा उपनिवेशवाद के प्रत्येक स्वरूप, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका, के प्रजाति भेदभाव को उनके मानवीय सम्मान के विरुद्ध कहकर निन्दा की, फिलिस्तीन में अरबों के अधिकारों का समर्थन किया राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या में वृद्धि तथा अफ्रीका एवं एशिया को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की । तीसरे विश्व के दृष्टिकोण से बाण्डुंग सम्मेलन के दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले ।
प्रथम:
इसने विश्व राजनीति की समस्याओं के प्रति एशिया और अफ्रीका में एक समान दृष्टिकोण को जन्म दिया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में एक ऐसे एशियाई-अफ्रीकी ग्रुप की आधारशिला रखी जिसने बाद में पूरब-पश्चिम संघर्ष में सन्तुलन पैदा करने का काम किया । पांच वर्ष के अन्दर (1960 तक) संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अफ्रीका तथा एशिया के राज्यों की संख्या 45 हो गयी । अब दो-तिहाई बहुमत से पास होने वाले प्रस्ताव के लिए इस गुट का समर्थन आवश्यक हो गया ।
द्वितीय:
पहली बार साम्यवादी चीन भी गैर-साम्यवादी राष्ट्रों के साथ सद्भावना और मैत्रीपूर्ण विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए उपस्थित हुआ । वारनेट के शब्दों में- ”यह सम्मेलन तीसरी दुनिया के पुनरुत्थान का प्रतीक था ।”
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन:
बाण्डुंग सम्मेलन के बाद तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका की अभिव्यक्ति गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में होने लगी । डॉ. पुष्पेश पन्त लिखते हैं- ”पश्चिम पश्चिमी और साम्यवादी देशों के गुटों या उनके द्वारा प्रेरित सैनिक सन्धियों में शामिल न होना गुटनिरपेक्षता की पहली शर्त है लेकिन यह इसका बाहरी लक्षण है । वास्तव में, इसका सम्बन्ध अफ्रेशियाई और अन्य विकासशील देशों की स्वतन्त्र चेतना से है जो साम्राज्यवादी चंगुल से छुटकारा पाने के बाद बाहरी दबावों से यथासम्भव मुक्त रहना चाहते हैं । भारत में प्रथम एशियाई सम्मेलन (1947) और इण्डोनेशिया में बाण्डुंग सम्मेलन (1955) के पीछे मुख्यतया यही प्रेरणा काम कर रही थी । अपना रास्ता खुद तलाश करने की इसी प्रवृत्ति ने 1961 में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की विधिवत् नींव रखी…….. ।”
अपने प्रारम्भिक वर्षो में गुटनिरपेक्षता के विचार की खिल्ली उड़ायी गयी थी लेकिन आज इस आन्दोलन में एशिया और अफ्रीका के ही नहीं यूरोप और लैटिन अमरीका के देश भी शामिल हैं । गुट-निरपेक्षता की व्यापक शक्ल लेने से पहले कुछ नेताओं ने इसे एशियाई देशों तक ही सीमित रखने का सुझाव दिया ।
उनके अनुसार एशियाई देशों की आपसी एकता से शान्ति का एक क्षेत्र विकसित होगा और इस ‘सुस्थिर’ क्षेत्र से वे अधिक विकास कर पाएंगे । जून 1964 में कोलम्बो में भारत, पाकिस्तान, म्यांमार (बर्मा), इण्डोनेशिया और श्रीलंका के प्रधानमन्त्रियों की बैठकों से पहले गुटनिरपेक्ष और अफ्रेशियाई आन्दोलन की स्थापना के बारे में कई महत्वपूर्ण बैठकें और सम्मेलन हुए ।
संयुक्त राष्ट्र में अफ्रेशियाई गुट प्रभावी ढंग से सक्रिय था । इसी गुट की सक्रियता के कारण ही कोरिया युद्ध समाप्त हुआ । सर्वप्रथम, बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन (1961) हुआ जिसमें नेहरू नासिर और टीटो की तिकड़ी की तरफ दुनिया की नजरें उठीं ।
डॉ. वैदिक लिखते हैं- “बेलग्रेड में एक तीसरी शक्ति का उदय हुआ था, जिसके नेता अपनी असंलग्नता और नैतिक बल के आधार पर युद्ध के कगार पर खड़ी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को शान्ति के मार्ग पर के जाने को बेताब थे ।”
बेलग्रेड सम्मेलन ने तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को कहां तक प्रभावित किया यह एक अलग प्रश्न है लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि शीत-युद्ध के डरावने बादलों के घटाटोप में बेलग्रेड सम्मेलन एक आशा की किरण-सा उभरा था । इसमें 28 देशों ने भाग लिया था ।
काहिरा के दूसरे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन (5-10 अक्टूबर, 1964) में पण्डित नेहरू की अनुपस्थिति सभी ने महसूस की । सम्मेलन की सदस्य संख्या बढ्कर 47 हो गयी । अफ्रीकी एकता संघ और अरब राज्य के महासचिवों ने भी प्रेक्षक की हैसियत से भाग लिया ।
भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री ने अपना पांच-सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया:
(1) परमाण्विक निःशस्त्रीकरण;
(2) सीमा-विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान;
(3) विदेशी प्रभुत्व, आक्रमण; विनाश तथा जातिगत भेदभाव से मुक्ति;
(4) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा आर्थिक विकास में तेजी लाना और
(5) संयुक्त राष्ट्र के शान्ति और विकास के कार्यक्रमों को पूर्ण समर्थन ।
नेहरू के बाद नासिर भी नहीं रहे और एक बार ऐसा लगा कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन भी गर्दिश में है । इसको बचाने का बीड़ा उठाया मार्शल टीटो ने । लुसाका में तीसरे सम्मेलन (6-10 सितम्बर, 1970) में एक नयी समस्या सतह पर आ गयी-हिन्द महासागर में बढ़ती हुई बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा ।
भारत का प्रतिनिधित्व श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया । जब उन्होंने कहा कि ”सैनिक गठबन्धन से अलग हुए गुटनिरपेक्ष देश शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के पक्ष में सत्ता का सन्तुलन बनाए रखने के लिए अपने सामूहिक विवेक और प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं” तो एक बार प्रतिनिधियों को भारत से आशा बंधी ।
अल्जीयर्स में चौथे सम्मेलन (5-9 सितम्बर, 1973) तक गुटनिरपेक्षता की परिभाषा भी बदल चुकी थी । अब शुद्ध ‘तटस्थ या गुटों में अलग देश’ ही इस आन्दोलन के सदस्य नहीं रह गए थे बल्कि उसकी परिभाषा को व्यापक बनाकर इस आन्दोलन को वृहत् स्वरूप प्रदान किया जा चुका था । सामूहिक आत्म-निर्भरता की विचारधारा कोलम्बो के पांचवें शिखर सम्मेलन (16-19 अगस्त, 1976) में सुनने को मिली । आर्थिक सहयोग सम्बन्धी कार्यवाही के लिए कार्यक्रम भी स्वीकार किया गया ।
एक प्रस्ताव में कहा गया कि जिस प्रकार विश्व-शान्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता उसी प्रकार तनाव-शैथिल्य भी सार्वदेशिक होना चाहिए । हवाना का छठा शिखर सम्मेलन (3-9 सितम्बर 1979) अवधि के लिहाज से लम्बा था । विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं के लिए विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराया गया । निर्गुट राष्ट्रों का सातवां शिखर सम्मेलन (7-12 मार्च 1983) नयी दिल्ली में हुआ ।
आठवां सम्मेलन हरारे (सितम्बर, 1986) में, नौवां सम्मेलन बेलग्रेड (सितम्बर, 1989) में, दसवां सम्मेलन जकार्ता (सितम्बर, 1992) में, ग्यारहवां सम्मेलन कोलम्बिया (सितम्बर, 1995) में, बारहवां शिखर सम्मेलन डरबन (2-3 सितम्बर, 1998) में, तेरहवां शिखर सम्मेलन मलेशिया (फरवरी, 2003) में, चौदहवां शिखर सम्मेलन हवाना (क्यूबा) (सितम्बर, 2006) में, पन्द्रहवां शिखर सम्मेलन शर्म-अल-शेख (मिस्र) में 15- 16 जुलाई, 2009 में तथा 16वां शिखर सम्मेलन तेहरान (ईरान) में 30-31 अगस्त, 2012 को सम्पन्न हुआ । वर्तमान में इस आन्दोलन की सदस्य संख्या 120 है ।
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में ज्यादातर (90% से भी अधिक) तथाकथित तीसरी दुनिया के राष्ट्र शामिल हैं । संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशवाद की कोई समस्या उठने अथवा विश्व-शान्ति के बारे में कोई आम प्रस्ताव आने की स्थिति में गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक साथ वोट देते आए हैं ।
12 जनवरी, 1989 को निर्गुट देशों की ओर से सुरक्षा परिषद् में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें दो लीबियाई विमानों को अमरीकी लड़ाकू विमानों द्वारा मार गिराए जाने की निन्दा की गई थी और अमरीका से कहा गया था कि वह लीबियाई तट पर सैनिक गतिविधियां स्थगित कर दे ताकि क्षेत्र में तनाव कम करने में मदद मिल सके ।
यद्यपि तीन स्थायी देशों-ब्रिटेन, अमरीका और फ्रांस के वीटो कर देने से प्रस्ताव नामंजूर हो गया तथापि यह निर्गुट देशों की एकजुटता का ताजा उदाहरण है । गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के कारण उपनिवेशवाद की समाप्ति की प्रक्रिया में तेजी आयी और साथ ही देशों का दो गुटों में ध्रुवीकरण धीमा पड़ा ।
ग्रुप ऑफ 77 (Group of 77):
1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों में अफ्रीकी राज्यों की संख्या काफी थी और संघ के लगभग दो-तिहाई सदस्य विकासशील देशों में से थे जो अपने को ‘ग्रुप ऑफ 77’ कहने लगे । वर्तमान में समूह-77 की सदस्य संख्या बढ्कर 132 हो गई है । फिर भी इन्हें ‘ग्रुप ऑफ 77’ के नाम से ही सम्बोधित किया जाता है । ‘ग्रुप ऑफ 77’ के अधिकांश देश तीसरे विश्व के हैं ।
ये देश नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करते हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ में ‘ग्रुप ऑफ 77’ के देशों ने इस बात पर जोर दिया कि नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में संघ के अभिकरणों को सक्रिय किया जाए । ‘ग्रुप ऑफ 77’ में ऐसे देश हैं जिनके आर्थिक हित समान हैं और जो संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना में बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं ।
‘ग्रुप ऑफ 77’ तीसरे विश्व के देशों की एकता का परिचायक है । वे संगठित होकर सौदेबाजी करना चाहते हैं तथा समुद्र से सम्बन्धित विधि शस्त्र-नियन्त्रण आणविक ऊर्जा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करना चाहते हैं । फिर भी अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ‘ग्रुप ऑफ 77’ देश विभाजित हैं । ग्रुप-77 का एक अन्तरंग लघु समूह भी है जिसे जी-24 (G-24) के नाम से जाना जाता है ।
जी-77 शिखर सम्मेलन का घोषणा-पत्र (हवाना: अप्रैल, 2000):
विकासशील देशों के समूह जी-77 का शिखर सम्मेलन 15 अप्रैल, 2000 को हवाना में आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग के आह्वान के साथ सम्पन्न हो गया । सम्मेलन में पारित घोषणा-पत्र में सदस्य देशों की राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को अस्थिर बनाने वाले आतंकवाद के सभी रूपों पर चिन्ता जताई गई । घोषणा-पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद के विभिन्न रूप खासकर राज्यपोषित और सीमा पार से चलाए जाने वाला आतंकवाद राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति एवं स्थिरता के लिए खतरनाक है ।
हवाना घोषणा-पत्र में नई सदी में विकासशील देशों के विकास के मुद्दों को तरजीह देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया गया । इसके साथ ही विश्व की सम्पदा और सत्ता को बढ़ावा देने के लिए नई वैश्विक मानवीय व्यवस्था का भी आह्वान किया गया ।
जी-15:
जी-15 या तीसरी दुनिया के 15 विकासशील देशों के ग्रुप की स्थापना 1989 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के समय की गई थी । जी-15 देशों का पहला शिखर सम्मेलन जून, 1990 में कुआलालम्पुर में हुआ था । सम्मेलन में दो प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था । यह थे-विकासशील देशों का कर्ज और विकसित एवं विकासशील देशों के बीच आर्थिक उदारवाद ।
काराकास में आयोजित दूसरे शिखर सम्मेलन (नवम्बर, 1991) की कार्य सूची में विकास की नई दिशाएं विकासशील देशों के बीच सहयोग और शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद युग में विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद जैसे मुद्दों को शामिल किया गया ।
सेनेगल की राजधानी डकार में जी-15 के तीसरे शिखर सम्मेलन (नवम्बर, 1992) में अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच की दूरी कम करने की अपील की गई । अर्जेण्टाइना में आयोजित जी-15 के शिखर सम्मेलन (नवम्बर, 1995) में संसाधनों के प्रवाह को नियमित करने और तकनीक के हस्तान्तरण को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया ।
सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला विश्व संस्थाओं में परिवर्तन के लिए विकासशील देशों के प्रयासों में तालमेल कायम करने का है । 11-13 मई, 1998 तक काहिरा में सम्पन्न जी-15 के आठवें शिखर सम्मेलन में दो प्रमुख लक्ष्यों-अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों का विकास तथा बहुपक्षीय व्यापार पद्धति का विकास और व्यापार एवं निवेश में अन्तर जी-15 सहयोग बढ़ाने पर प्रकाश डाला । मोण्टेगो सिटी (जमैका) में सम्पन्न (10-12 फरवरी 1999) नौवें जी-15 शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों के हित के मसलों पर व्यापक वार्ता की गई ।
इनमें पूंजी प्रवाहों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता सहित वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति पर चर्चाएं विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत एक पारदर्शी निष्पक्ष और न्यायसंगत नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के महत्व की पुन: पुष्टि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार दक्षिण-दक्षिण तथा अन्तर जी-15 सहयोग तथा इन मामलों में जी-15, जी-8 वार्ता कराने की सम्भावनाओं से सम्बद्ध मसले थे । जी-15 के कुल 19 सदस्य राष्ट्र हैं: मैक्सिको, जमैका, वेनेजुएला, पेरू, ब्राजील, अर्जेण्टाइना, अल्जीरिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, मिस्र, मलेशिया, इण्डोनेशिया, सेनेगल, भारत, श्रीलंका, कीनिया, कोलम्बिया, चिली और ईरान ।
एशिया सुरक्षा सम्मेलन:
3 जून, 2006 को सिंगापुर में एशिया सुरक्षा सम्मेलन लन्दन स्थित ‘इण्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट फार स्ट्रेटजिक स्टडीज’ के तत्वावधान में सम्पन्न हुआ । इसमें अमेरिका के रक्षामन्त्री डोनाल्ड रम्सफील्ड भी उपस्थित थे । अमेरिका और जापान की चिन्ता चीन को लेकर थी जो कब अपनी नीति बदल दे और संकट खड़ा कर दे ।
भारत के रक्षामन्त्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि चीन और भारत के बिना एशिया की सुरक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती । चीन, जापान और इण्डोनेशिया के साथ मिलकर भारत एशिया की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योग दे सकता है ।
अल्पविकसित देशों की समस्याओं पर चतुर्थ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन:
9-13 मई, 2011 को विश्व के 48 अल्पविकसित देशों की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का चतुर्थ सम्मेलन इस्तांबूल (तुर्की) में सम्पन्न हुआ । ऐसा सम्मेलन प्रति दस वर्ष बाद सम्पन्न होता है; इस प्रकार का पहला सम्मेलन 1980 से सम्पन्न हुआ था ।
इस्तांबूल सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि यह थी कि सम्मेलन के अन्त में लगभग आम सहमति से दो दस्तावेज जारी किए गए:
प्रथम:
इस्तांबूल कार्यवाही योजना जिसमें अगले दस वर्षों के लिए अल्पविकसित देशों के विकास की रणनीति का उल्लेख है ।
दूसरा:
दस्तावेज इस्तांबूल राजनीतिक घोषणा है जिसमें अल्पविकसित देशों के विकास के सम्बन्ध में सामान्य दृष्टिकोण का उल्लेख है ।
तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की मांगें:
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद तीसरी दुनिया के राष्ट्र एकजुट होकर निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत कर रहे हैं:
1. नव-उपनिवेशवाद का विरोध:
तीसरी दुनिया के राष्ट्र नव-उपनिवेशवाद तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के शोषण का विरोध करते हैं ।
2. नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग:
प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शोषण पर आधारित है अत: तीसरी दुनिया के राष्ट्र नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे हैं । वे चाहते हैं कि विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम किया जाये कच्चे माल तथा तैयार माल की कीमतों में ज्यादा अन्तर न हो तथा प्रतिकूल व्यापार शर्तों को हटाया जाये ।
3. उत्तर-दक्षिण संवाद:
तीसरी दुनिया के देश यह मांग कर रहे हैं कि उत्तर-दक्षिण संवाद जारी रखा जाये ताकि विकसित देश विकासशील देशों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकें ।
4. संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतन्त्रीकरण:
तींसरी दुनिया के देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन चाहते हैं ताकि एशिया-अफ्रीका के देशों को उसमें स्थायी सदस्यता प्राप्त हो सके । विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी पुनर्गठन चाहते हैं ।
तीसरे विश्व के विकासशील देश: ऋणग्रस्तता एक विकट समस्या:
विश्व विकास आन्दोलन (WDM) की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वित्तीय संस्थान प्रतिवर्ष विकासशील तीसरे विश्व के देशों को जितना ऋण देते हैं उससे कहीं अधिक वे ब्याज और भुगतान के रूप में वसूलते हैं ।
रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक ने वर्ष 1992 में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को कुल 3 अरब डॉलर का ऋण दिया, परन्तु ऋण के ब्याज और भुगतान के उपरान्त इन देशों को मात्र 88 करोड़ 5 लाख डॉलर ही प्राप्त हो सके ।
विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित वार्षिक विश्व विकास की रिपोर्ट में उनके उस बहुप्रचारित दावे का विश्लेषण किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत को सन् 1994 से 1999 के दौरान 2,636 मिलियन डॉलर की रकम प्रदान की गई है । जबकि वास्तविकता यह है कि विदेशी ऋणदाताओं को भारत द्वारा ब्याज और अन्य सेवा शुल्कों को मिलाकर 4,703 मिलियन डॉलर की रकम दी गई है । इन आंकड़ों को देखने से लगता है कि भारत से बाहर जाने वाली पूंजी 2,067 मिलियन डॉलर है ।
वर्ष 1992 में विश्व बैंक ने अफ्रीकी देशों को 2.6 अरब डॉलर ऋण दिया लेकिन इन देशों पर विश्व बैंक के पुराने ऋण और ब्याज के भुगतान के रूप में इसकी दो-तिहाई से भी अधिक राशि निकल गई । इतना ही नहीं नाइजीरिया ने 1992 में विश्व बैंक से जितना ऋण लिया उससे कहीं अधिक उसे ब्याज का भुगतान करना पड़ा ।
विश्व बैंक ने लैटिन अमरीकी देशों को 1992 में कुल 5.2 अरब डालर का ऋण दिया, जबकि वह अब तक इसके लिए कुल 75 अरब डॉलर वसूल चुका है । तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, ब्राजील, आदि कई देशों की स्थितियां भी लगभग इसी प्रकार की हैं ।
रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों पर विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय समुदाय द्वारा दिये गये ऋण का बोझ बढ़ता जायेगा क्योंकि ये संस्थान अब रियायती दरों पर ऋण प्रदान कर रहे हैं । लेकिन सच तो यह है कि रियायती दरों पर बहुत ही कम ऋण दिये जा रहे हैं । उदाहरणत: वर्ष 1992-93 के लिए विश्व बैंक ने अफ्रीकी देशों को 2.8 अरब डॉलर का ऋण देने का वायदा किया जिसमें से केवल 47 करोड़ डॉलर ही रियायती दरों पर था ।
इन संस्थानों द्वारा विकासशील देशों का ऋण माफ करने की कोई उम्मीद नहीं है । इन संस्थानों की मान्यता है कि यदि इन देशों के ऋण माफ किये गये तो अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में उनकी साख गिरेगी तथा धन उगाहने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।
तीसरे विश्व में हथियारों की होड़:
इस बात पर तो अब किसी को आश्चर्य नहीं होता कि हथियारों का विनिर्माण विश्व का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है । परन्तु यह निश्चित ही ताज्जुब की बात है कि विकसित देशों ने तीसरी दुनिया के देशों को अपने हथियारों को बेचने की सबसे बड़ी मण्डी बना दिया है ।
1972 से 1982 के दौरान सेनाओं पर खर्च के बारे में अमरीकी शस्त्र नियन्त्रण एवं निःशस्त्रीकरण संस्था की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में औद्योगिक राष्ट्रों का रक्षा खर्च 24 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जबकि तीसरी दुनिया के देशों का रक्षा व्यय इसी अवधि में 5 प्रतिशत की दर से बढ़ा । इस दस साल की अवधि में हथियारों का आयात विकसित देशों में 11 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि तीसरी दुनिया के देशों में हथियारों के आयात में 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि तीसरी दुनिया में हथियारों के सबसे बडे खरीदार 1973 के बाद से लेकर अब तक मध्य-पूर्व के देश रहे हैं । विश्व भर में कुल हथियार आयात में 1982 में मध्य-पूर्व का हिस्सा 42 प्रतिशत था ।
तीसरी दुनिया के जो दस देश अपने केन्द्रीय बजट का सर्वाधिक हिस्सा हथियारों की खरीद पर खर्च कर रहे हैं उनमें से आठ मध्य-पूर्व के हैं । ओमान जैसा छोटा-सा खाड़ी राष्ट्र केन्द्रीय बजट का आधा हिस्सा हथियारों पर खर्च कर रहा है ।
1950 व 1960 के दशकों में तीसरी दुनिया के देश अपनी हथियारों की जरूरतें पूरी तरह आयात के द्वारा पूरा करते थे । 1980 के दशक में इन मुल्कों में लगभग 1,250 करोड़ रुपए मूल्यों के हथियारों का वार्षिक विनिर्माण भी होने लगा । मगर यह अस्त्र-शस्त्र विनिर्माण विश्व स्तर पर हो रहे आयुध उत्पादन का एक प्रतिशत भी नहीं है ।
उधर तीसरी दुनिया के देश जितने हथियार अपने यहां बना रहे हैं उसके मुकाबले 10 गुना अधिक मूल्य के हथियारों का आयात कर रहे हैं । 1970 के पहले तीसरी दुनिया के सिर्फ भारत, अर्जेण्टीना ब्राजील व मिस्र ही ऐसे देश थे जहां हथियारों का निर्माण होता था । अब 26 विकासोमुख देशों में हथियारों के विनिर्माण का काम चल रहा है । हालांकि तीसरी दुनिया के कुल अस्त्र-शस्त्र उत्पादन का आधा हिस्सा सिर्फ इजरायल में हो रहा है ।
तीसरी दुनिया के जिन चार देशों में हथियारों का विनिर्माण तेजी से बढ़ा है वे हैं भारत, इजरायल, दक्षिणी अफ्रीका व चिली । इन देशों में विशिष्ट राजनीतिक जरूरतों के कारण हथियारों का निर्माण शुरू हुआ । उधर कुछ विकासोन्मुख देश ऐसे हैं जहां विदेशी कम्पनियों ने व्यावसायिक कारणों से हथियारों का उत्पादन शुरू किया है ।
तीसरी दुनिया में शुरू हो चुके हथियारों के इस सीमित पैमाने के उत्पादन को लेकर भी पश्चिमी देशों के हथियार निर्माताओं में फिक्र पैदा हो गयी । जब तक ये मुल्क अपने हथियारों की जरूरतों के लिए पश्चिमी देशों या रूस पर पूर्णत: आश्रित थे तब तक हथियारों की होड़ तीसरी दुनिया में मची रहने में शस्त्रास्त्र के इन सौदागरों को लाभ-ही-लाभ नजर आता था । अब हथियारों की बिक्री करने वाले इन देशों को तीसरी दुनिया की हथियार विनिर्माण की कोशिशें ‘हथियारों की होड़’ का खतरा बनकर दिखाई देने लगी हैं ।
हथियारों के परम्परागत निर्माता व विक्रेता देश अभी तक इस बात को लेकर मन-ही-मन खुश हैं कि हथियारों के निर्माण की तकनीक में इतनी तेजी से बदलाव आ रहा है कि उनका विनिर्माण तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों के लिए असम्भव बना रहेगा ।
चाहे स्वदेशीकरण की कितनी ही चेष्टाएं तीसरी दुनिया के देश क्यों न करें उन्हें विशिष्ट रक्षा उपकरणों की अपनी आवश्यकताओं के लिए औद्योगिक राष्ट्रों पर निर्भर रहना ही होगा । अमरीकी संसद के लिए तैयार की गई एक वार्षिक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार 1998-2005 के दौरान भारत हथियारों की खरीद के मामले में पहले स्थान पर रहा और उसने इस अवधि में 20.7 अरब डॉलर के हथियार खरीद समझौते किए ।
वर्ष 2005 में भारत ने 5.4 अरब डॉलर के सऊदी अरब ने 3.4 अरब डॉलर के तथा चीन ने 2.8 अरब डॉलर के हथियार खरीद समझौते कर क्रमश: प्रथम तीन स्थान पर रहे । रिपोर्ट में कहा गया है कि हथियार आपूर्तिकर्ता देशों के लिए विकासशील देश आकर्षक बाजार बने हुए हैं ।
2005 के दौरान विकासशील देशों को कुल 30.2 अरब डॉलर मूल्य के हथियारों की आपूर्ति की गई जो कि वर्ष 2004 की तुलना में बहुत अधिक थी । मार्च, 2014 में जारी सीपरी रिपोर्ट के अनुसार 2009-13 की पांच वर्षीय अवधि में भारत के हथियार आयात में 111 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा विश्व के कुल शस्त्र आयात में उसका अंश 7% से बढकर 14 प्रतिशत हो गया ।
तीसरे विश्व की एकता का प्रश्न:
पश्चिमी विद्वानों के मतानुसार तीसरी दुनिया के देशों की एकता का विचार सैद्धान्तिक रूप से उनके मध्य अधिकांश मामलों पर विचार साम्य होने से सम्भव प्रतीत होता है । किन्तु इन देशों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में विभिन्नताओं के कारण व्यवहार में हम उनमें पारस्परिक फूट पाते हैं ।
ऊपरी तौर पर भले ही वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विश्व महाशक्तियों की आलोचना कर लें एवं राजनीतिक दबाव के साथ ही नयी विदेशी मदद को अस्वीकृत करने की खुली घोषणा कर दें किन्तु असल में वे अपने देश की आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति के लिए अधिक-से-अधिक मदद चाहते हैं । तीसरी दुनिया में ऐसे बहुत कम राष्ट्र हैं जो बड़ी शक्तियों की मदद के बिना आसानी से अपना काम चला सकें ।
इसके अलावा स्वयं तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के साथ कच्चे माल के निर्यात वस्तुओं के निर्धारण एवं उनके बाजारों के हितों में परस्पर विरोधाभास पाया जाता है । तीसरी दुनिया के तेल उत्पादक राष्ट्रों (जिन्होंने तीसरी दुनिया में विशेष ‘धनवान’ की श्रेणी प्राप्त कर ली है) ने भी अपने साथी राष्ट्रों के हितों का अभी तक कोई ख्याल नहीं किया है एवं उल्टे वे इन राष्ट्रों को महंगे दामों पर तेल निर्यात करते हैं ।
कम्पूचिया से वियतनामी सेनाओं की वापसी का प्रश्न रहा हो या ईरान-इराक संघर्ष के शान्तिपूर्ण निपटारे की समस्या या फिलिस्तीनी शरणार्थियों का मसला या अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का मुद्दा हो; आपसी फूट के कारण तीसरे विश्व के देश कोई भी ठोस कदम नहीं उठा सके । इन सभी कारणों से तीसरी दुनिया की सौदा करने की स्थिति कमजोर रही है ।
संयुक्त राज्य अमरीका और तृतीय विश्व:
संयुक्त राज्य अमरीका की एशिया, लैटिन अमरीका और अफ्रीका में नीति का विश्लेषण करने से ‘तृतीय विश्व’ के देशों के प्रति उसके दृष्टिकोण एवं नीति का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है ।
इस नीति के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं:
1. साम्यवाद परिरोधन की नीति:
अमरीका ने तृतीय विश्व में साम्यवाद परिरोधन की नीति अपनाई । साम्यवाद परिरोधन की नीति साम्यवाद के प्रभाव एवं प्रसार को रोकना चाहती है तथा अवसर मिल जाए तो उसका पूर्ण उन्मूलन चाहती है । रीओ सन्धि, ‘अमरीकी राज्यों का संगठन’, ट्रूमैन सिद्धान्त, सीटो सन्धि, आइजनहॉवर सिद्धान्त के निर्माण का मूल ध्येय तृतीय विश्व के देशों को साम्यवादी चंगुल से बचाना था ।
2. आर्थिक सहायता की नीति:
तृतीय विश्व के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए अमरीका ने आर्थिक सहायता की नीति अपनाई । यूनान और तुर्की को ट्रूमैन सिद्धान्त के अन्तर्गत 40 करोड़ डॉलर की सहायता दी गयी । ईरान को द्वितीय विश्व-युद्ध काल में ही 2 करोड़ 60 लाख डॉलर की आर्थिक सहायता दी गई ।
रीगन प्रशासन के अन्तर्गत तीसरी दुनिया के वे देश ही आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके जिन्होंने सीधे-साधे अमरीकी हितों के लिए काम किया चाहे उनके देशों में सैनिक तन्त्र तानाशाही और अधिनायक तन्त्र ही विद्यमान था ।
3. सैनिक गठबन्धनों की नीति:
द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई-पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट । पूंजीवादी गुट का नेता अमरीका था । इन्हीं दिनों एशिया अफ्रीका और लैटिन अमरीका में नव-स्वतन्त्र देशों का उदय हुआ । अमरीका ने सैनिक गठबन्धनों की नीति का सूत्रपात कर तीसरी दुनिया के इन नव-स्वतन्त्र देशों को अपने गुट से सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया । सीटो सन्धि द्वारा दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को, सेण्टो सन्धि द्वारा पश्चिमी एशिया के देशों को, रीओ सन्धि द्वारा अटलाण्टिक और प्रशान्त महासागर के देशों को अमरीकी गुटबन्दी में शामिल करने का प्रयत्न किया ।
4. सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति:
अमरीका ने तीसरी दुनिया के देशों में सैनिक अड्डों, बन्दरगाहों तथा तेल टैंकों आदि की सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश की । हिन्द महासागर में अमरीका के न केवल स्थायी सैनिक अड्डे हैं बल्कि उसे अनेक तटवर्ती देशों की हवाई पट्टियों और बन्दरगाहों के प्रयोग की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं । डियागो गार्शिया उसका प्रमुख बन्दरगाह है ।
जिन देशों में अमरीका को हवाई पट्टियों या बन्दरगाहों की सुविधाएं उपलब्ध हैं उनमें प्रमुख हैं: मिस्र में एट्ज्योन का हवाई सैनिक अड्डा, शर्म-अल-शेख का नौ-सैनिक अड्डा तथा रस बानस का अड्डा; सोमालिया में बरबेरा; पाकिस्तान में कराची के पश्चिम में वादर का बन्दरगाह; कीनिया में मोम्बासा; ओमान में मसीरा हवाई अड्डा और मैराह आदि । इसके अतिरिक्त, बहरीन, जिबूती और सऊदी अरब में अमरीका के पास स्थायी अड्डे हैं ।
अमरीका के हिन्दमहासागरीय अड्डों में डियागो गार्शिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । डियागो गार्शिया पर अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करके अमरीका एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों पर अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है और रूस के नौ-सैनिक रास्तों पर नजर रख सकता है ।
5. हस्तक्षेप की नीति:
अमरीका ने तीसरी दुनिया में हस्तक्षेप अथवा तीसरी दुनिया के कमजोर देशों पर अपनी मर्जी लादने की नीति भी अपनायी । इस नीति का मूल उद्देश्य तीसरी दुनिया के उन देशों की सरकारों को अपदस्थ करना है या उनका तख्ता पलटना है जो अमरीका के लिए किसी दृष्टि से असहायक हैं । अमरीका को वे सरकारें गवारा नहीं चाहे वे लोगों द्वारा चुनी हुई क्यों न हों जो उसके इशारे पर नहीं चलतीं ।
जो सरकारें उसकी खिलाफत करती हैं उसे वे गवारा नहीं । वह तीसरी दुनिया के देशों की स्वतन्त्रता और सार्वभौमिकता को लील जाना चाहता है । लेबनान के गृह-युद्ध और जोर्डन में उसने आइजनहॉवर सिद्धान्त के अन्तर्गत अपनी सेनाएं भेजीं वियतनाम युद्ध में सक्रिय भाग लिया और लोन नोल को उकसाकर कम्बोडिया में राजकुमार सिंहनुक का तख्ता पलट करवा दिया ।
1983 में अमरीकी सैनिक हस्तक्षेप से ग्रेनाडा में कराई गई बगावत, 1983 में निकारागुआ के बन्दरगाहों में बिछाई गई बारूदी सुरंगें, सादीनिस्ता निकारागुआ की सरकार के विरोधी केंट्रोस को दी जा रही आर्थिक और सैनिक सहायता तथा लीबियाई नेता कर्नल गद्दाफी का सफाया करने के लिए अप्रैल 1986 को लीबिया पर किया गया हमला सीरिया के हाफिज असद को आतंकवादी ठहराना मई 1989 में पनामा में अमरीकी सेनाएं भेजना तथा बाद में 20 दिसम्बर 1989 को वहां सैनिक शासक जनरल मेनुअल एण्टोनियो नोरिएगा को अमरीकी सेनाओं द्वारा अपदस्थ करना, हैती में जनतन्त्र की बहाली के नाम पर एरिस्टाइड को पुन: सत्तासीन करना (1994), आदि सब एक ही कड़ी से जुड़े सवाल हैं ।
6. आर्थिक ओर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति:
तीसरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से अमरीका आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना में प्रयत्नशील है । अमरीका बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विकासशील देशों की लूट का एक माध्यम असमान व्यापार है ।
विकासशील देशों में सस्ते श्रम कच्चे माल तथा शोषण की तीव्रता के कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विकासशील देशों में विनियोजित पूंजी से प्राप्त मुनाफे की दर सर्वाधिक ऊंची है । अमरीकी व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1950 से 1965 के बीच अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने यूरोप में विनियोजित पूंजी पर 74 प्रतिशत और विकासशील देशों में विनियोजित पूंजी पर 264 प्रतिशत मुनाफा कमाया ।
इसी प्रकार अमरीका तीसरी दुनिया में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना का भी प्रयत्न करता रहा है । अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्र, अमरीकी पुस्तकालय, अमरीकी पत्र-पत्रिकाएं, स्कॉलरशिप योजनाएं, वाइस ऑफ अमेरिका के प्रसारण अमरीकी सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के प्रमुख उपकरण हैं ।
अमरीका के सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक विशेषता यह है कि विकासशील देशों को यहां से प्रति वर्ष कम कीमत की लाखों पुस्तकें भेजी जाती हैं । अमरीकी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों का प्रचार और तीसरी दुनिया के देशों के सांस्कृतिक मूल्यों को हीन बताना सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है ।
7. दबाव की नीति:
संयुक्त राज्य अमरीका तीसरी दुनिया के देशों पर दबाव डालकर उनकी नीतियों को अपने अनुकूल परिवर्तित करवाने का प्रयास करता रहा है ।
अमरीकी दबाव के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं:
(1) 1975 में अमरीकी बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक कम्पनी ने मैक्सिको की सरकार पर दबाव डाला कि वह अपने श्रम कानून को जो मजदूरों को थोड़ा संरक्षण देता है बदल डाले । जब मैक्सिको की सरकार ने ऐसा करने से इकार कर दिया तो कम्पनी ने अपना कारखाना बन्द कर उसे कोस्टारिका में स्थानान्तरित कर दिया । इसके परिणामस्वरूप 12,000 मजदूर बेरोजगार हो गए ।
(2) चिली में जब अलेन्दे की सरकार ने अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के कदम उठाए तो जबाव में अमरीकी कम्पनियों ने अलेन्दे की हत्या करवा दी तथा सरकार को उलटवा दिया ।
(3) भारत ने अणु अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया तो अमरीका ने रूस पर दबाव डाला कि वह भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरो से नाता तोड़ ले ।
8. शस्त्र निर्यात:
अमरीका तीसरी दुनिया के देशों को हथियारों का निर्यात करता रहा है । 1950 से 1972 तक अमरीका ने तीसरी दुनिया के देशों को 8,522 करोड़ डॉलर के हथियारों का निर्यात किया । अमरीका ने इजरायल, सऊदी अरब, जोर्डन, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, दक्षिण कोरिया, आदि देशों की कठपुतली तथा दलाल सरकारों को हथियारों से लैस कर विकासशील देशों को विकास कार्य छोड्कर प्रतिरक्षा व्यय बढ़ाने के लिए मजबूर किया ।
9. परमाणु अप्रसार सन्धि:
अमरीका ‘परमाणु क्लब’ को सीमित रखना चाहता है । वह नहीं चाहता कि तीसरी दुनिया के देश अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखें । वह चाहता है कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगायें । वह यह भी चाहता है कि उत्तरी कोरिया अपने परमाणु संयन्त्रों को अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की जांच के लिए खोल दे ।
ADVERTISEMENTS:
10. उच्च तकनीक के हस्तान्तरण को रोकना:
विकासशील देशों के स्वावलम्बी बनने के प्रयासों को रोकने के लिए अमरीका एम. टी. सी. आर. (MTCR) सन्धि का सहारा लेता है । भारत को क्रायोजेनिक इंजन और उसकी तकनीक को हस्तान्तरित करने से रोकने के लिए अमरीका ने इसी सन्धि के तहत रूस पर दबाव डाला था । इससे पूर्व अमरीका ने भारत को सुपर कम्प्यूटर और भारी पानी देने के अपने ही समझौतों को तोड़ते हुए इन्हें भारत को देने से इकार कर दिया था ।
तीसरी दुनिया के देशों में चाहे भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर का मुद्दा हो अथवा पश्चिमी एशिया में अरब-इजरायल संघर्ष अथवा दक्षिण-पूर्वी एशिया में वियतनाम का मसला; अमरीकी हथियार किसी-न-किसी रूप में अवश्य प्रयुक्त हुए हैं ।
निष्कर्ष:
सोवियत संघ के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के ध्वस्त होने के बाद स्थापित एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में तीसरी दुनिया के देशों पर अमरीकी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है । विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा ‘विश्व व्यापार संघ’ (WTO) जैसी संस्थाओं पर अमरीका का आधिपत्य है, अत: इन संस्थाओं के माध्यम से अमरीका तीसरी दुनिया के देशों पर आर्थिक नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है ।